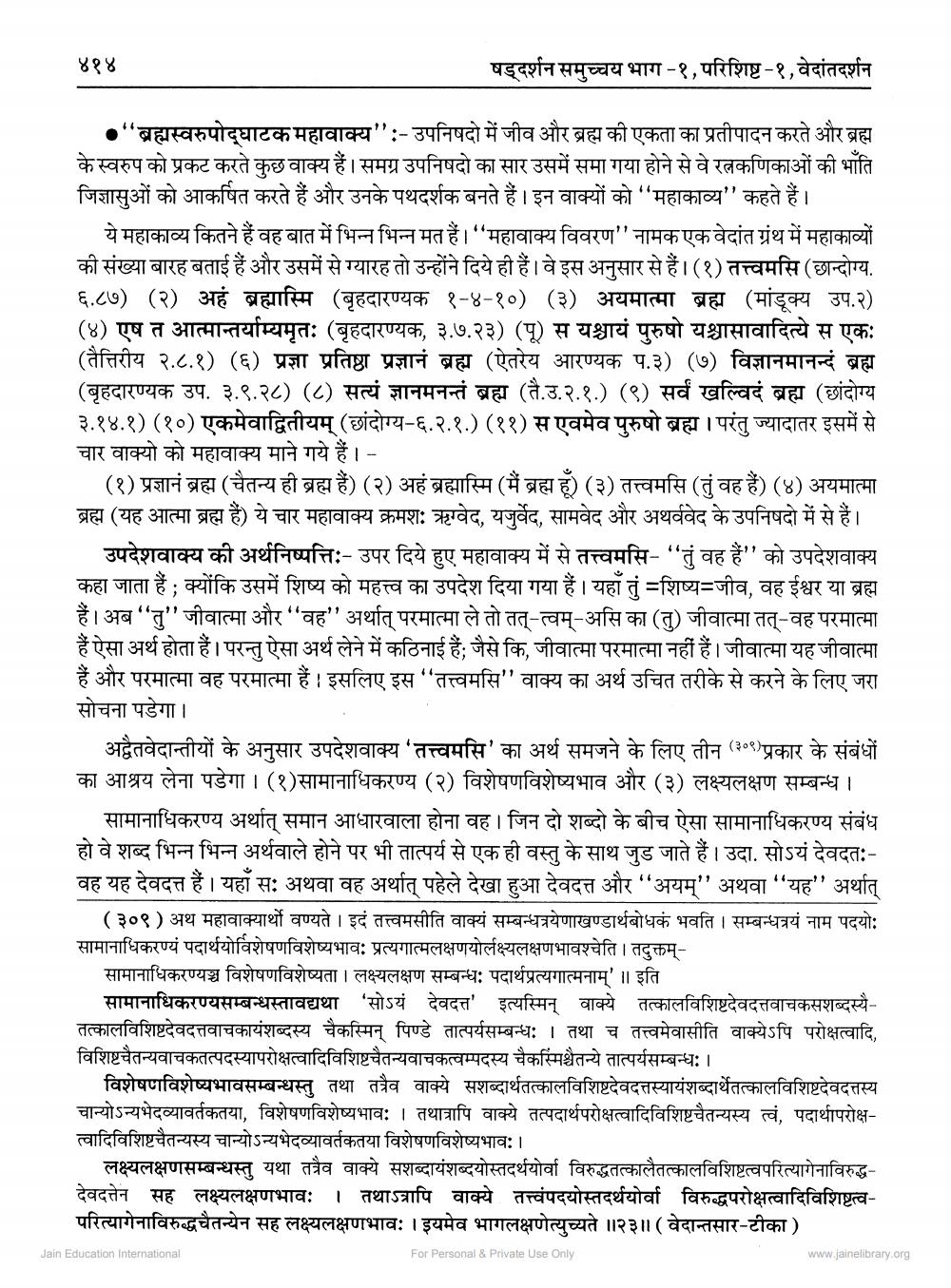________________
४१४
षड्दर्शन समुच्चय भाग-१, परिशिष्ट-१, वेदांतदर्शन
•"ब्रह्मस्वरुपोद्घाटक महावाक्य" :- उपनिषदो में जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतीपादन करते और ब्रह्म के स्वरुप को प्रकट करते कुछ वाक्य हैं। समग्र उपनिषदो का सार उसमें समा गया होने से वे रत्नकणिकाओं की भाँति जिज्ञासुओं को आकर्षित करते हैं और उनके पथदर्शक बनते हैं। इन वाक्यों को "महाकाव्य" कहते हैं।
ये महाकाव्य कितने हैं वह बात में भिन्न भिन्न मत हैं। "महावाक्य विवरण'' नामक एक वेदांत ग्रंथ में महाकाव्यों की संख्या बारह बताई हैं और उसमें से ग्यारह तो उन्होंने दिये ही हैं। वे इस अनुसार से हैं। (१) तत्त्वमसि (छान्दोग्य. ६.८७) (२) अहं ब्रह्मास्मि (बृहदारण्यक १-४-१०) (३) अयमात्मा ब्रह्म (मांडूक्य उप.२) (४) एष त आत्मान्तर्याम्यमतः (बहदारण्यक, ३.७.२३) (प) स यश्चायं पुरुषो यश्चासावादित्ये स एकः (तैत्तिरीय २.८.१) (६) प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म (ऐतरेय आरण्यक प.३) (७) विज्ञानमानन्दं ब्रह्म (बृहदारण्यक उप. ३.९.२८) (८) सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तै.उ.२.१.) (९) सर्वं खल्विदं ब्रह्म (छांदोग्य ३.१४.१) (१०) एकमेवाद्वितीयम् (छांदोग्य-६.२.१.) (११) स एवमेव पुरुषो ब्रह्म । परंतु ज्यादातर इसमें से चार वाक्यो को महावाक्य माने गये हैं। -
(१) प्रज्ञानं ब्रह्म (चैतन्य ही ब्रह्म हैं) (२) अहं ब्रह्मास्मि (मैं ब्रह्म हूँ) (३) तत्त्वमसि (तुं वह हैं) (४) अयमात्मा ब्रह्म (यह आत्मा ब्रह्म हैं) ये चार महावाक्य क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के उपनिषदो में से हैं।
उपदेशवाक्य की अर्थनिष्पत्तिः- उपर दिये हुए महावाक्य में से तत्त्वमसि- "तुं वह हैं' को उपदेशवाक्य कहा जाता हैं ; क्योंकि उसमें शिष्य को महत्त्व का उपदेश दिया गया हैं। यहा तुं =शिष्य-जीव, वह ईश्वर या ब्रह्म हैं। अब "तु" जीवात्मा और "वह" अर्थात् परमात्मा ले तो तत्-त्वम्-असि का (तु) जीवात्मा तत्-वह परमात्मा हैं ऐसा अर्थ होता है। परन्तु ऐसा अर्थ लेने में कठिनाई हैं; जैसे कि, जीवात्मा परमात्मा नहीं हैं। जीवात्मा यह जीवात्मा हैं और परमात्मा वह परमात्मा हैं। इसलिए इस "तत्त्वमसि' वाक्य का अर्थ उचित तरीके से करने के लिए जरा सोचना पडेगा।
अद्वैतवेदान्तीयों के अनुसार उपदेशवाक्य 'तत्त्वमसि' का अर्थ समजने के लिए तीन (३०९)प्रकार के संबंधों का आश्रय लेना पडेगा । (१)सामानाधिकरण्य (२) विशेषणविशेष्यभाव और (३) लक्ष्यलक्षण सम्बन्ध ।
सामानाधिकरण्य अर्थात् समान आधारवाला होना वह। जिन दो शब्दो के बीच ऐसा सामानाधिकरण्य संबंध हो वे शब्द भिन्न भिन्न अर्थवाले होने पर भी तात्पर्य से एक ही वस्तु के साथ जुड़ जाते हैं। उदा. सोऽयं देवदत:वह यह देवदत्त हैं । यहाँ सः अथवा वह अर्थात् पहेले देखा हुआ देवदत्त और "अयम्" अथवा "यह" अर्थात्
(३०९) अथ महावाक्यार्थो वण्यते । इदं तत्त्वमसीति वाक्यं सम्बन्धत्रयेणाखण्डार्थबोधकं भवति । सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः सामानाधिकरण्यं पदार्थयोविशेषणविशेष्यभावः प्रत्यगात्मलक्षणयोर्लक्ष्यलक्षणभावश्चेति । तदुक्तम्
सामानाधिकरण्यञ्च विशेषणविशेष्यता । लक्ष्यलक्षण सम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम्' ।। इति
सामानाधिकरण्यसम्बन्धस्तावद्यथा 'सोऽयं देवदत्त' इत्यस्मिन् वाक्ये तत्कालविशिष्टदेवदत्तवाचकसशब्दस्यैतत्कालविशिष्टदेवदत्तवाचकायंशब्दस्य चैकस्मिन् पिण्डे तात्पर्यसम्बन्धः । तथा च तत्त्वमेवासीति वाक्येऽपि परोक्षत्वादि, विशिष्टचैतन्यवाचकतत्पदस्यापरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यवाचकत्वम्पदस्य चैकस्मिश्चैतन्ये तात्पर्यसम्बन्धः ।
विशेषणविशेष्यभावसम्बन्धस्तु तथा तत्रैव वाक्ये सशब्दार्थतत्कालविशिष्टदेवदत्तस्यायंशब्दार्थेतत्कालविशिष्टदेवदत्तस्य चान्योऽन्यभेदव्यावर्तकतया, विशेषणविशेष्यभावः । तथात्रापि वाक्ये तत्पदार्थपरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यस्य त्वं, पदार्थापरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यस्य चान्योऽन्यभेदव्यावर्तकतया विशेषणविशेष्यभावः ।
लक्ष्यलक्षणसम्बन्धस्तु यथा तत्रैव वाक्ये सशब्दायंशब्दयोस्तदर्थयोर्वा विरुद्धतत्कालैतत्कालविशिष्टत्वपरित्यागेनाविरुद्धदेवदत्तेन सह लक्ष्यलक्षणभावः । तथाऽत्रापि वाक्ये तत्त्वंपदयोस्तदर्थयोर्वा विरुद्धपरोक्षत्वादिविशिष्टत्वपरित्यागेनाविरुद्धचैतन्येन सह लक्ष्यलक्षणभावः । इयमेव भागलक्षणेत्युच्यते ॥२३॥ ( वेदान्तसार-टीका)
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org