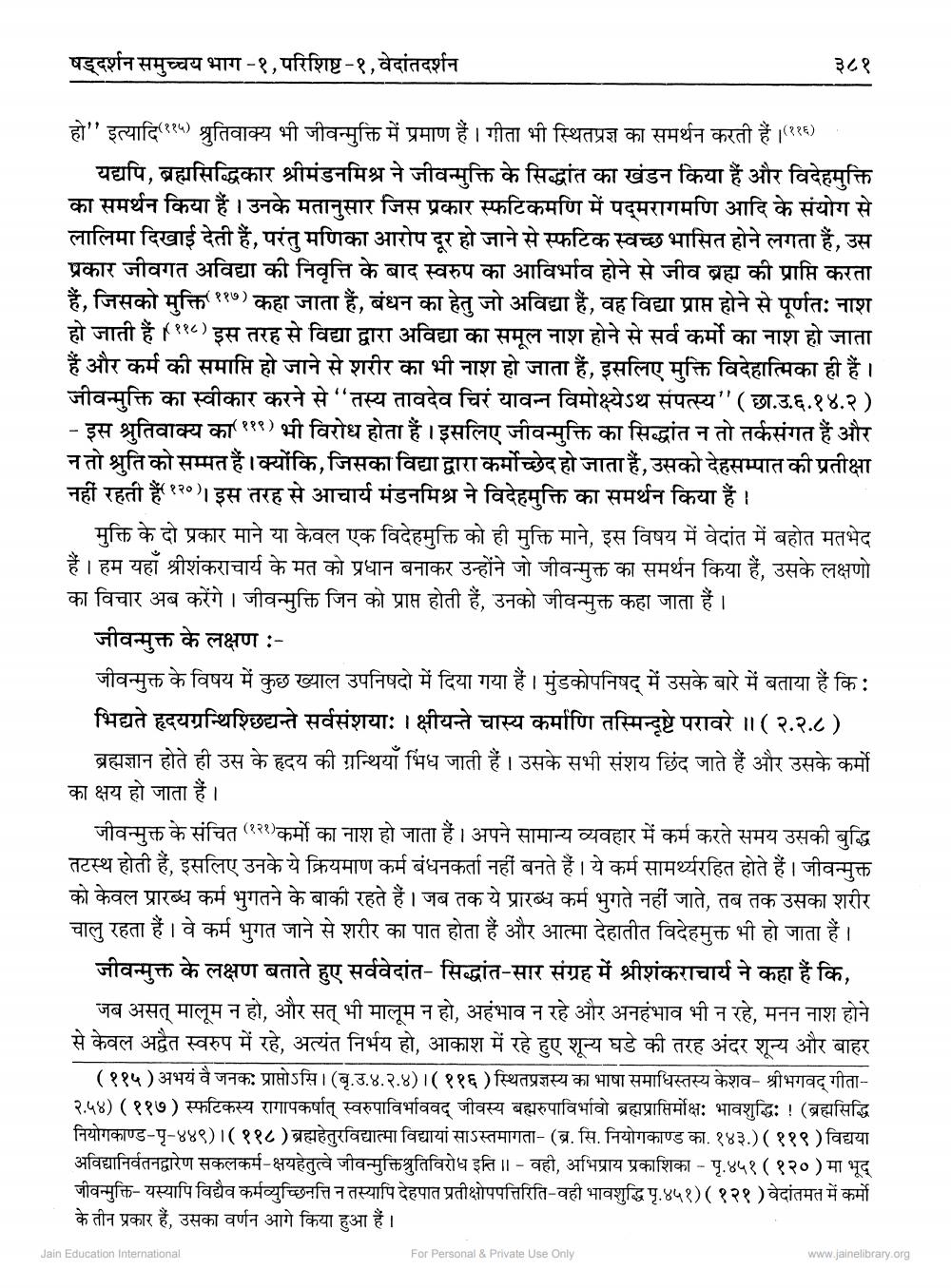________________
षड्दर्शन समुच्चय भाग -१, परिशिष्ट-१, वेदांतदर्शन
३८१
हो" इत्यादि(११५) श्रुतिवाक्य भी जीवन्मुक्ति में प्रमाण हैं । गीता भी स्थितप्रज्ञ का समर्थन करती हैं । ११६) ___ यद्यपि, ब्रह्मसिद्धिकार श्रीमंडनमिश्र ने जीवन्मुक्ति के सिद्धांत का खंडन किया हैं और विदेहमुक्ति का समर्थन किया हैं। उनके मतानुसार जिस प्रकार स्फटिकमणि में पद्मरागमणि आदि के संयोग से लालिमा दिखाई देती हैं, परंतु मणिका आरोप दूर हो जाने से स्फटिक स्वच्छ भासित होने लगता हैं, उस प्रकार जीवगत अविद्या की निवृत्ति के बाद स्वरुप का आविर्भाव होने से जीव ब्रह्म की प्राप्ति करता हैं, जिसको मुक्ति १९७) कहा जाता हैं, बंधन का हेतु जो अविद्या हैं, वह विद्या प्राप्त होने से पूर्णतः नाश हो जाती हैं । ११८) इस तरह से विद्या द्वारा अविद्या का समूल नाश होने से सर्व कर्मो का नाश हो जाता हैं और कर्म की समाप्ति हो जाने से शरीर का भी नाश हो जाता हैं, इसलिए मुक्ति विदेहात्मिका ही हैं। जीवन्मुक्ति का स्वीकार करने से "तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्य'' ( छा.उ.६.१४.२) - इस श्रुतिवाक्य का ११९) भी विरोध होता हैं । इसलिए जीवन्मुक्ति का सिद्धांत न तो तर्कसंगत हैं और न तो श्रुति को सम्मत हैं। क्योंकि, जिसका विद्या द्वारा कर्मोच्छेद हो जाता हैं, उसको देहसम्पात की प्रतीक्षा नहीं रहती हैं। १२० । इस तरह से आचार्य मंडनमिश्र ने विदेहमुक्ति का समर्थन किया हैं। ___ मुक्ति के दो प्रकार माने या केवल एक विदेहमुक्ति को ही मुक्ति माने, इस विषय में वेदांत में बहोत मतभेद हैं। हम यहाँ श्रीशंकराचार्य के मत को प्रधान बनाकर उन्होंने जो जीवन्मुक्त का समर्थन किया हैं, उसके लक्षणो का विचार अब करेंगे । जीवन्मुक्ति जिन को प्राप्त होती हैं, उनको जीवन्मुक्त कहा जाता हैं।
जीवन्मुक्त के लक्षण :जीवन्मुक्त के विषय में कुछ ख्याल उपनिषदो में दिया गया हैं। मुंडकोपनिषद् में उसके बारे में बताया हैं कि : भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ (२.२.८) ब्रह्मज्ञान होते ही उस के हृदय की ग्रन्थियाँ भिंध जाती हैं। उसके सभी संशय छिंद जाते हैं और उसके कर्मो का क्षय हो जाता हैं।
जीवन्मुक्त के संचित (१२१ कर्मो का नाश हो जाता हैं। अपने सामान्य व्यवहार में कर्म करते समय उसकी बुद्धि तटस्थ होती हैं, इसलिए उनके ये क्रियमाण कर्म बंधनकर्ता नहीं बनते हैं। ये कर्म सामर्थ्यरहित होते हैं। जीवन्मुक्त को केवल प्रारब्ध कर्म भुगतने के बाकी रहते हैं। जब तक ये प्रारब्ध कर्म भुगते नहीं जाते, तब तक उसका शरीर चालु रहता हैं । वे कर्म भुगत जाने से शरीर का पात होता हैं और आत्मा देहातीत विदेहमुक्त भी हो जाता हैं।
जीवन्मुक्त के लक्षण बताते हुए सर्ववेदांत-सिद्धांत-सार संग्रह में श्रीशंकराचार्य ने कहा हैं कि,
जब असत् मालूम न हो, और सत् भी मालूम न हो, अहंभाव न रहे और अनहंभाव भी न रहे, मनन नाश होने से केवल अद्वैत स्वरुप में रहे, अत्यंत निर्भय हो, आकाश में रहे हुए शून्य घडे की तरह अंदर शून्य और बाहर
(११५) अभयं वै जनकः प्राप्तोऽसि । (बृ.उ.४.२.४) । (११६) स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव- श्रीभगवद् गीता२.५४) (११७) स्फटिकस्य रागापकर्षात् स्वरुपाविर्भाववद् जीवस्य बह्मरुपाविर्भावो ब्रह्मप्राप्तिर्मोक्षः भावशुद्धिः ! (ब्रह्मसिद्धि नियोगकाण्ड-पृ-४४९) । (११८) ब्रह्महेतुरविद्यात्मा विद्यायां साऽस्तमागता- (ब्र. सि. नियोगकाण्ड का. १४३.) ( ११९) विद्यया अविद्यानिर्वतनद्वारेण सकलकर्म-क्षयहेतुत्वे जीवन्मुक्तिश्रुतिविरोध इति ।। - वही, अभिप्राय प्रकाशिका - पृ.४५१ (१२०) मा भूद् जीवन्मुक्ति- यस्यापि विद्यैव कर्मव्युच्छिनत्ति न तस्यापि देहपात प्रतीक्षोपपत्तिरिति-वही भावशुद्धि पृ.४५१)(१२१) वेदांतमत में कर्मो के तीन प्रकार हैं, उसका वर्णन आगे किया हुआ हैं।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org