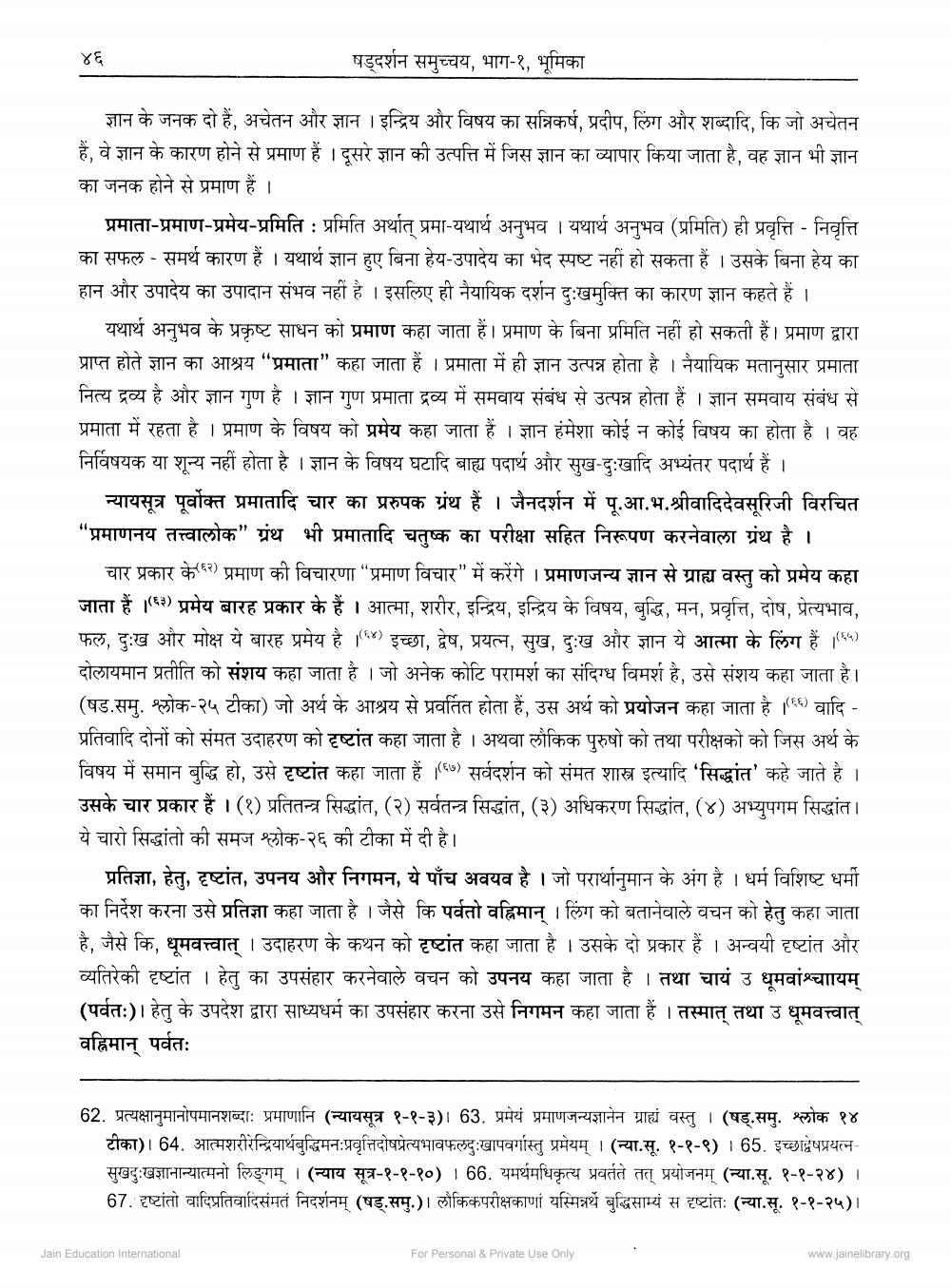________________
४६
षड्दर्शन समुच्चय, भाग-१, भूमिका
___ ज्ञान के जनक दो हैं, अचेतन और ज्ञान । इन्द्रिय और विषय का सन्निकर्ष, प्रदीप, लिंग और शब्दादि, कि जो अचेतन हैं, वे ज्ञान के कारण होने से प्रमाण हैं । दूसरे ज्ञान की उत्पत्ति में जिस ज्ञान का व्यापार किया जाता है, वह ज्ञान भी ज्ञान
का जनक होने से प्रमाण हैं । ___ प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय-प्रमिति : प्रमिति अर्थात् प्रमा-यथार्थ अनुभव । यथार्थ अनुभव (प्रमिति) ही प्रवृत्ति - निवृत्ति
का सफल - समर्थ कारण हैं । यथार्थ ज्ञान हुए बिना हेय-उपादेय का भेद स्पष्ट नहीं हो सकता हैं । उसके बिना हेय का हान और उपादेय का उपादान संभव नहीं है । इसलिए ही नैयायिक दर्शन दुःखमुक्ति का कारण ज्ञान कहते हैं । ___ यथार्थ अनुभव के प्रकृष्ट साधन को प्रमाण कहा जाता हैं। प्रमाण के बिना प्रमिति नहीं हो सकती हैं। प्रमाण द्वारा प्राप्त होते ज्ञान का आश्रय "प्रमाता" कहा जाता हैं । प्रमाता में ही ज्ञान उत्पन्न होता है । नैयायिक मतानुसार प्रमाता नित्य द्रव्य है और ज्ञान गुण है । ज्ञान गुण प्रमाता द्रव्य में समवाय संबंध से उत्पन्न होता हैं । ज्ञान समवाय संबंध से प्रमाता में रहता है । प्रमाण के विषय को प्रमेय कहा जाता हैं । ज्ञान हमेशा कोई न कोई विषय का होता है । वह निर्विषयक या शून्य नहीं होता है । ज्ञान के विषय घटादि बाह्य पदार्थ और सुख-दुःखादि अभ्यंतर पदार्थ हैं ।
न्यायसूत्र पूर्वोक्त प्रमातादि चार का प्ररुपक ग्रंथ हैं । जैनदर्शन में पू.आ.भ.श्रीवादिदेवसूरिजी विरचित "प्रमाणनय तत्त्वालोक" ग्रंथ भी प्रमातादि चतुष्क का परीक्षा सहित निरूपण करनेवाला ग्रंथ है ।
चार प्रकार के (६२) प्रमाण की विचारणा “प्रमाण विचार" में करेंगे । प्रमाणजन्य ज्ञान से ग्राह्य वस्तु को प्रमेय कहा जाता हैं ।(६३) प्रमेय बारह प्रकार के हैं । आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, इन्द्रिय के विषय, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख और मोक्ष ये बारह प्रमेय है ।(६४) इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान ये आत्मा के लिंग हैं ।(६५) दोलायमान प्रतीति को संशय कहा जाता है । जो अनेक कोटि परामर्श का संदिग्ध विमर्श है, उसे संशय कहा जाता है। (षड.समु. श्लोक-२५ टीका) जो अर्थ के आश्रय से प्रवर्तित होता हैं, उस अर्थ को प्रयोजन कहा जाता है ।६६) वादि - प्रतिवादि दोनों को संमत उदाहरण को दृष्टांत कहा जाता है । अथवा लौकिक पुरुषो को तथा परीक्षको को जिस अर्थ के विषय में समान बुद्धि हो, उसे दृष्टांत कहा जाता हैं ।६७) सर्वदर्शन को संमत शास्त्र इत्यादि 'सिद्धांत' कहे जाते है । उसके चार प्रकार हैं । (१) प्रतितन्त्र सिद्धांत, (२) सर्वतन्त्र सिद्धांत, (३) अधिकरण सिद्धांत, (४) अभ्युपगम सिद्धांत। ये चारो सिद्धांतो की समज श्लोक-२६ की टीका में दी है। __ प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन, ये पाँच अवयव है । जो परार्थानुमान के अंग है । धर्म विशिष्ट धर्मी का निर्देश करना उसे प्रतिज्ञा कहा जाता है । जैसे कि पर्वतो वह्निमान् । लिंग को बतानेवाले वचन को हेतु कहा जाता है, जैसे कि, धूमवत्त्वात् । उदाहरण के कथन को दृष्टांत कहा जाता है । उसके दो प्रकार हैं । अन्वयी दृष्टांत और व्यतिरेकी दृष्टांत । हेतु का उपसंहार करनेवाले वचन को उपनय कहा जाता है । तथा चायं उ धूमवांश्चाायम् (पर्वतः)। हेतु के उपदेश द्वारा साध्यधर्म का उपसंहार करना उसे निगमन कहा जाता हैं । तस्मात् तथा उ धूमवत्त्वात् वह्निमान् पर्वतः
62. प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि (न्यायसूत्र १-१-३)। 63. प्रमेयं प्रमाणजन्यज्ञानेन ग्राह्यं वस्तु । (षड्.समु. श्लोक १४
टीका)। 64. आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम् । (न्या.सू. १-१-९) । 65. इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम् । (न्याय सूत्र-१-१-१०) । 66. यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत् प्रयोजनम् (न्या.सू. १-१-२४) । 67. दृष्टांतो वादिप्रतिवादिसंमतं निदर्शनम् (षड्.समु.)। लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टांतः (न्या.सू. १-१-२५)।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org