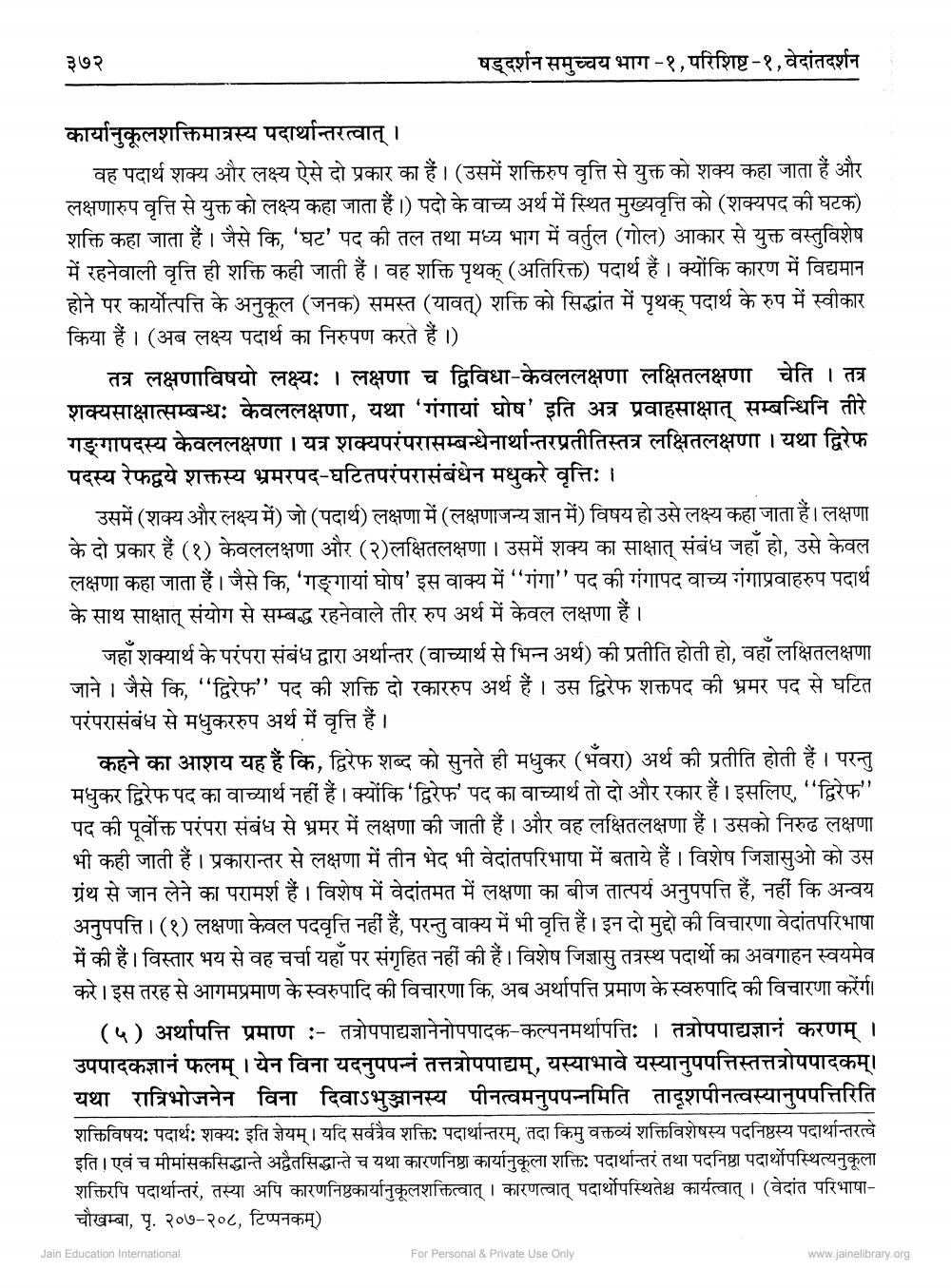________________
३७२
षड्दर्शन समुच्चय भाग-१, परिशिष्ट-१, वेदांतदर्शन
कार्यानुकूलशक्तिमात्रस्य पदार्थान्तरत्वात् ।
वह पदार्थ शक्य और लक्ष्य ऐसे दो प्रकार का हैं। (उसमें शक्तिरुप वृत्ति से युक्त को शक्य कहा जाता हैं और लक्षणारुप वृत्ति से युक्त को लक्ष्य कहा जाता हैं।) पदो के वाच्य अर्थ में स्थित मुख्यवृत्ति को (शक्यपद की घटक) शक्ति कहा जाता हैं । जैसे कि, 'घट' पद की तल तथा मध्य भाग में वर्तुल (गोल) आकार से युक्त वस्तुविशेष में रहनेवाली वृत्ति ही शक्ति कही जाती हैं । वह शक्ति पृथक् (अतिरिक्त) पदार्थ हैं। क्योंकि कारण में विद्यमान होने पर कार्योत्पत्ति के अनुकूल (जनक) समस्त (यावत्) शक्ति को सिद्धांत में पृथक् पदार्थ के रुप में स्वीकार किया हैं। (अब लक्ष्य पदार्थ का निरुपण करते हैं ।) ___ तत्र लक्षणाविषयो लक्ष्यः । लक्षणा च द्विविधा-केवललक्षणा लक्षितलक्षणा चेति । तत्र शक्यसाक्षात्सम्बन्धः केवललक्षणा, यथा 'गंगायां घोष' इति अत्र प्रवाहसाक्षात् सम्बन्धिनि तीरे गङ्गापदस्य केवललक्षणा । यत्र शक्यपरंपरासम्बन्धेनार्थान्तरप्रतीतिस्तत्र लक्षितलक्षणा । यथा द्विरेफ पदस्य रेफद्वये शक्तस्य भ्रमरपद-घटितपरंपरासंबंधेन मधुकरे वृत्तिः ।
उसमें (शक्य और लक्ष्य में) जो (पदार्थ) लक्षणा में (लक्षणाजन्य ज्ञान में) विषय हो उसे लक्ष्य कहा जाता हैं। लक्षणा के दो प्रकार हैं (१) केवललक्षणा और (२)लक्षितलक्षणा। उसमें शक्य का साक्षात् संबंध जहाँ हो, उसे केवल लक्षणा कहा जाता हैं। जैसे कि, 'गङ्गायां घोष' इस वाक्य में “गंगा'' पद की गंगापद वाच्य गंगाप्रवाहरुप पदार्थ के साथ साक्षात् संयोग से सम्बद्ध रहनेवाले तीर रुप अर्थ में केवल लक्षणा हैं।
जहाँ शक्यार्थ के परंपरा संबंध द्वारा अर्थान्तर (वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ) की प्रतीति होती हो, वहाँ लक्षितलक्षणा जाने । जैसे कि, "द्विरेफ" पद की शक्ति दो रकाररुप अर्थ हैं । उस द्विरेफ शक्तपद की भ्रमर पद से घटित परंपरासंबंध से मधुकररुप अर्थ में वृत्ति हैं।
कहने का आशय यह हैं कि, द्विरेफ शब्द को सुनते ही मधुकर (भंवरा) अर्थ की प्रतीति होती हैं । परन्तु मधुकर द्विरेफ पद का वाच्यार्थ नहीं हैं। क्योंकि 'द्विरेफ' पद का वाच्यार्थ तो दो और रकार हैं। इसलिए, "द्विरेफ" पद की पूर्वोक्त परंपरा संबंध से भ्रमर में लक्षणा की जाती हैं। और वह लक्षितलक्षणा हैं। उसको निरुढ लक्षणा भी कही जाती हैं। प्रकारान्तर से लक्षणा में तीन भेद भी वेदांतपरिभाषा में बताये हैं। विशेष जिज्ञासुओ को उस ग्रंथ से जान लेने का परामर्श हैं । विशेष में वेदांतमत में लक्षणा का बीज तात्पर्य अनुपपत्ति हैं, नहीं कि अन्वय अनुपपत्ति । (१) लक्षणा केवल पदवृत्ति नहीं हैं, परन्तु वाक्य में भी वृत्ति हैं। इन दो मुद्दो की विचारणा वेदांतपरिभाषा में की हैं। विस्तार भय से वह चर्चा यहाँ पर संगृहित नहीं की हैं। विशेष जिज्ञासु तत्रस्थ पदार्थो का अवगाहन स्वयमेव करे। इस तरह से आगमप्रमाण के स्वरुपादि की विचारणा कि, अब अर्थापत्ति प्रमाण के स्वरुपादि की विचारणा करेंगी
(५) अर्थापत्ति प्रमाण :- तत्रोपपाद्यज्ञानेनोपपादक-कल्पनमर्थापत्तिः । तत्रोपपाद्यज्ञानं करणम् । उपपादकज्ञानं फलम् । येन विना यदनुपपन्नं तत्तत्रोपपाद्यम्, यस्याभावे यस्यानुपपत्तिस्तत्तत्रोपपादकम्। यथा रात्रिभोजनेन विना दिवाऽभुञ्जानस्य पीनत्वमनुपपन्नमिति तादृशपीनत्वस्यानुपपत्तिरिति शक्तिविषयः पदार्थः शक्यः इति ज्ञेयम । यदि सर्वत्रैव शक्तिः पदार्थान्तरम, तदा किम वक्तव्यं शक्तिविशेषस्य पदनिष्ठस्य पदार्थान्तरत्वे इति । एवं च मीमांसकसिद्धान्ते अद्वैतसिद्धान्ते च यथा कारणनिष्ठा कार्यानुकूला शक्तिः पदार्थान्तरं तथा पदनिष्ठा पदार्थोपस्थित्यनुकूला शक्तिरपि पदार्थान्तरं, तस्या अपि कारणनिष्ठकार्यानुकूलशक्तित्वात् । कारणत्वात् पदार्थोपस्थितेश्च कार्यत्वात् । (वेदांत परिभाषाचौखम्बा, पृ. २०७-२०८, टिप्पनकम्)
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org