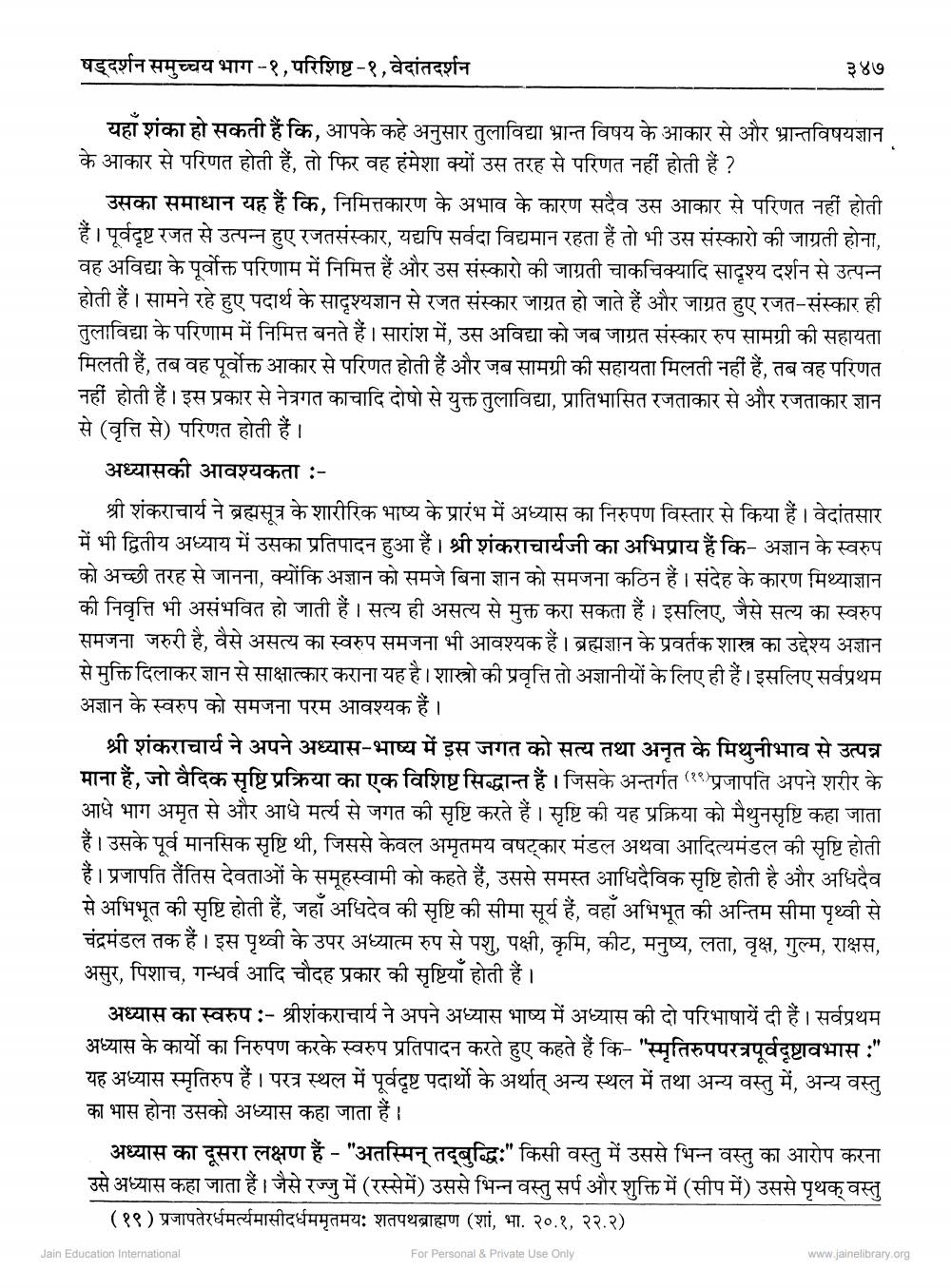________________
षड्दर्शन समुच्चय भाग-१, परिशिष्ट-१, वेदांतदर्शन
३४७
यहाँ शंका हो सकती हैं कि, आपके कहे अनुसार तुलाविद्या भ्रान्त विषय के आकार से और भ्रान्तविषयज्ञान के आकार से परिणत होती हैं, तो फिर वह हमेशा क्यों उस तरह से परिणत नहीं होती हैं ?
उसका समाधान यह हैं कि, निमित्तकारण के अभाव के कारण सदैव उस आकार से परिणत नहीं होती हैं। पूर्वदृष्ट रजत से उत्पन्न हुए रजतसंस्कार, यद्यपि सर्वदा विद्यमान रहता हैं तो भी उस संस्कारो की जाग्रती होना, वह अविद्या के पूर्वोक्त परिणाम में निमित्त हैं और उस संस्कारो की जाग्रती चाकचिक्यादि सादृश्य दर्शन से उत्पन्न होती हैं। सामने रहे हुए पदार्थ के सादृश्यज्ञान से रजत संस्कार जाग्रत हो जाते हैं और जाग्रत हुए रजत-संस्कार ही तुलाविद्या के परिणाम में निमित्त बनते हैं। सारांश में, उस अविद्या को जब जाग्रत संस्कार रुप सामग्री की सहायता मिलती हैं, तब वह पूर्वोक्त आकार से परिणत होती हैं और जब सामग्री की सहायता मिलती नहीं हैं, तब वह परिणत नहीं होती हैं। इस प्रकार से नेत्रगत काचादि दोषो से युक्त तुलाविद्या, प्रातिभासित रजताकार से और रजताकार ज्ञान से (वृत्ति से) परिणत होती हैं।
अध्यासकी आवश्यकता :
श्री शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के शारीरिक भाष्य के प्रारंभ में अध्यास का निरुपण विस्तार से किया हैं । वेदांतसार में भी द्वितीय अध्याय में उसका प्रतिपादन हुआ हैं। श्री शंकराचार्यजी का अभिप्राय हैं कि- अज्ञान के स्वरुप को अच्छी तरह से जानना, क्योंकि अज्ञान को समजे बिना ज्ञान को समजना कठिन हैं। संदेह के कारण मिथ्याज्ञान की निवृत्ति भी असंभवित हो जाती हैं । सत्य ही असत्य से मुक्त करा सकता हैं। इसलिए, जैसे सत्य का स्वरुप समजना जरुरी है, वैसे असत्य का स्वरुप समजना भी आवश्यक हैं। ब्रह्मज्ञान के प्रवर्तक शास्त्र का उद्देश्य अज्ञान से मुक्ति दिलाकर ज्ञान से साक्षात्कार कराना यह है। शास्त्रो की प्रवृत्ति तो अज्ञानीयों के लिए ही हैं। इसलिए सर्वप्रथम अज्ञान के स्वरुप को समजना परम आवश्यक हैं।
श्री शंकराचार्य ने अपने अध्यास-भाष्य में इस जगत को सत्य तथा अनृत के मिथुनीभाव से उत्पन्न माना हैं, जो वैदिक सृष्टि प्रक्रिया का एक विशिष्ट सिद्धान्त हैं। जिसके अन्तर्गत (१९ प्रजापति अपने शरीर के आधे भाग अमृत से और आधे मर्त्य से जगत की सृष्टि करते हैं । सृष्टि की यह प्रक्रिया को मैथुनसृष्टि कहा जाता हैं। उसके पूर्व मानसिक सृष्टि थी, जिससे केवल अमृतमय वषट्कार मंडल अथवा आदित्यमंडल की सृष्टि होती हैं। प्रजापति तैंतिस देवताओं के समूहस्वामी को कहते हैं, उससे समस्त आधिदैविक सृष्टि होती है और अधिदैव से अभिभूत की सृष्टि होती हैं, जहाँ अधिदेव की सृष्टि की सीमा सूर्य हैं, वहाँ अभिभूत की अन्तिम सीमा पृथ्वी से चंद्रमंडल तक हैं । इस पृथ्वी के उपर अध्यात्म रुप से पशु, पक्षी, कृमि, कीट, मनुष्य, लता, वृक्ष, गुल्म, राक्षस, असुर, पिशाच, गन्धर्व आदि चौदह प्रकार की सृष्टियाँ होती हैं।
अध्यास का स्वरुप :- श्रीशंकराचार्य ने अपने अध्यास भाष्य में अध्यास की दो परिभाषायें दी हैं। सर्वप्रथम अध्यास के कार्यो का निरुपण करके स्वरुप प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि- "स्मृतिरुपपरत्रपूर्वदृष्टावभास :" यह अध्यास स्मृतिरुप हैं । परत्र स्थल में पूर्वदृष्ट पदार्थो के अर्थात् अन्य स्थल में तथा अन्य वस्तु में, अन्य वस्तु का भास होना उसको अध्यास कहा जाता हैं। __ अध्यास का दूसरा लक्षण हैं - "अतस्मिन् तबुद्धिः" किसी वस्तु में उससे भिन्न वस्तु का आरोप करना उसे अध्यास कहा जाता हैं। जैसे रज्जु में (रस्सेमें) उससे भिन्न वस्तु सर्प और शुक्ति में (सीप में) उससे पृथक् वस्तु (१९) प्रजापतेरर्धमर्त्यमासीदर्धममृतमयः शतपथब्राह्मण (शां, भा. २०.१, २२.२)
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org