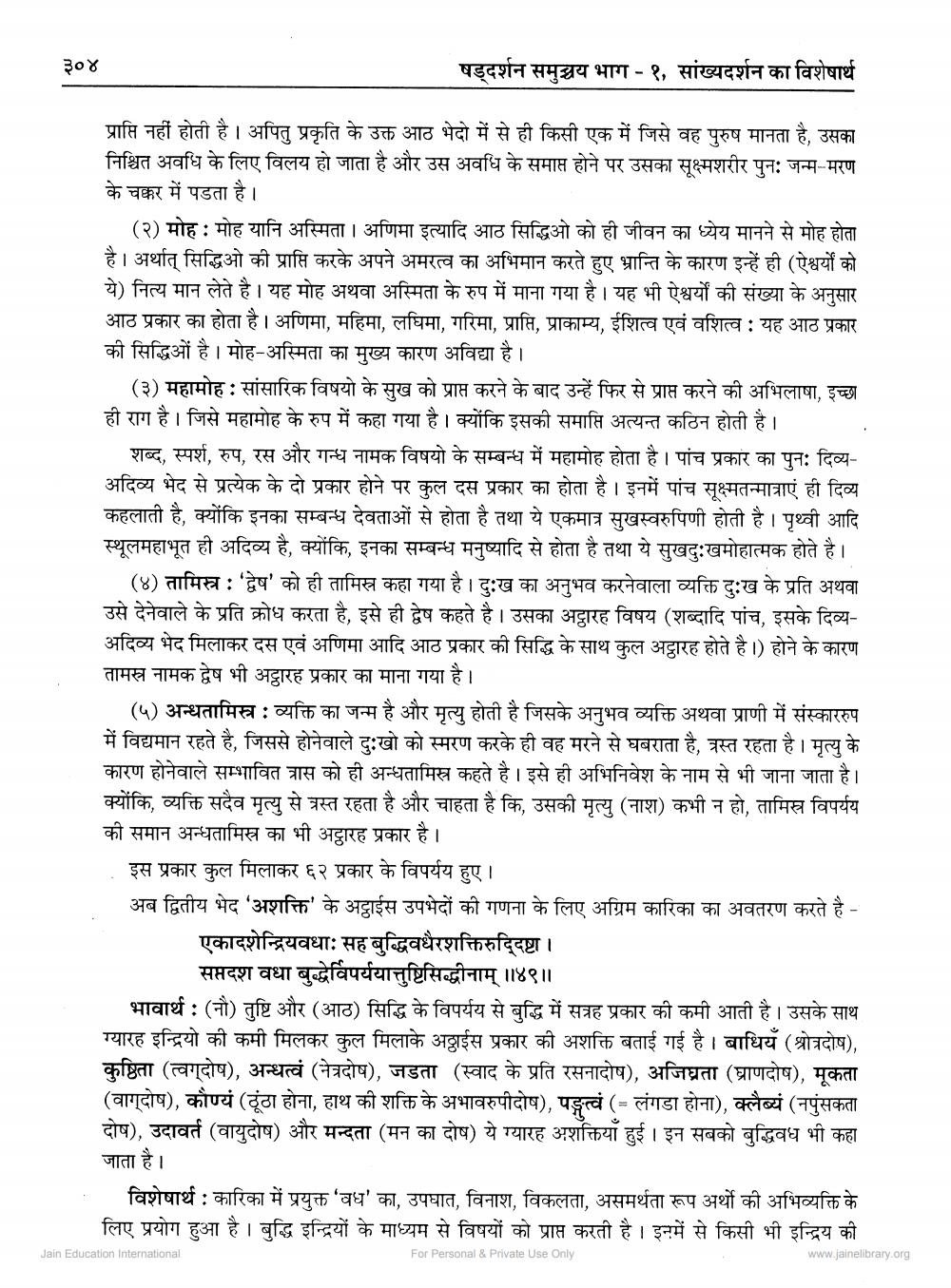________________
३०४
षड्दर्शन समुचय भाग - १, सांख्यदर्शन का विशेषार्थ
प्राप्ति नहीं होती है। अपितु प्रकृति के उक्त आठ भेदो में से ही किसी एक में जिसे वह पुरुष मानता है, उसका निश्चित अवधि के लिए विलय हो जाता है और उस अवधि के समाप्त होने पर उसका सूक्ष्मशरीर पुन: जन्म-मरण के चक्कर में पडता है
I
(२) मोह : मोह यानि अस्मिता । अणिमा इत्यादि आठ सिद्धिओ को ही जीवन का ध्येय मानने से मोह होता है । अर्थात् सिद्धिओ की प्राप्ति करके अपने अमरत्व का अभिमान करते हुए भ्रान्ति के कारण इन्हें ही (ऐश्वर्यों को ये) नित्य मान लेते है । यह मोह अथवा अस्मिता के रुप में माना गया है। यह भी ऐश्वर्यों की संख्या के अनुसार आठ प्रकार का होता है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व एवं वशित्व : यह आठ प्रकार की सिद्धिओं है । मोह-अस्मिता का मुख्य कारण अविद्या है।
(३) महामोह : सांसारिक विषयो के सुख को प्राप्त करने के बाद उन्हें फिर से प्राप्त करने की अभिलाषा, इच्छा ही राग है । जिसे महामोह के रुप में कहा गया है। क्योंकि इसकी समाप्ति अत्यन्त कठिन होती है।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध नामक विषयो के सम्बन्ध में महामोह होता है। पांच प्रकार का पुनः दिव्यअदिव्य भेद से प्रत्येक के दो प्रकार होने पर कुल दस प्रकार का होता है। इनमें पांच सूक्ष्मतन्मात्राएं ही दिव्य कहलाती है, क्योंकि इनका सम्बन्ध देवताओं से होता है तथा ये एकमात्र सुखस्वरुपिणी होती है । पृथ्वी आदि स्थूलमहाभूत ही अदिव्य है, क्योंकि, इनका सम्बन्ध मनुष्यादि से होता है तथा ये सुखदुःखमोहात्मक होते है।
(४) तामिस्र : 'द्वेष' को ही तामिस्र कहा गया है। दुःख का अनुभव करनेवाला व्यक्ति दुःख के प्रति अथवा उसे देनेवाले के प्रति क्रोध करता है, इसे ही द्वेष कहते है । उसका अट्ठारह विषय (शब्दादि पांच, इसके दिव्यअदिव्य भेद मिलाकर दस एवं अणिमा आदि आठ प्रकार की सिद्धि के साथ कुल अट्ठारह होते है ।) होने के कारण तामस्र नामक द्वेष भी अट्ठारह प्रकार का माना गया है।
(५) अन्धतामिस्र : व्यक्ति का जन्म है और मृत्यु होती है जिसके अनुभव व्यक्ति अथवा प्राणी में संस्काररुप में विद्यमान रहते है, जिससे होनेवाले दुःखो को स्मरण करके ही वह मरने से घबराता है, त्रस्त रहता है । मृत्यु ं कारण होनेवाले सम्भावित त्रास को ही अन्धतामिस्र कहते है । इसे ही अभिनिवेश के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि, व्यक्ति सदैव मृत्यु से त्रस्त रहता है और चाहता है कि, उसकी मृत्यु (नाश) कभी न हो, तामिस्र विपर्यय की समान अन्धतामिस्र का भी अट्ठारह प्रकार है ।
इस प्रकार कुल मिलाकर ६२ प्रकार के विपर्यय हुए।
-
अब द्वितीय भेद 'अशक्ति' के अट्ठाईस उपभेदों की गणना के लिए अग्रिम कारिका का अवतरण करते है एकादशेन्द्रियवधाः सह बुद्धिवधैरशक्तिरुद्दिष्टा । सप्तदश वधा बुद्धेर्विपर्ययात्तुष्टिसिद्धीनाम् ॥४९॥
भावार्थ : (नौ) तुष्टि और (आठ) सिद्धि के विपर्यय से बुद्धि में सत्रह प्रकार की कमी आती है। उसके साथ ग्यारह इन्द्रियो की कमी मिलकर कुल मिलाके अठ्ठाईस प्रकार की अशक्ति बताई गई है । बाधिय (श्रोत्रदोष), कुष्ठिता (त्वग्दोष), अन्धत्वं (नेत्रदोष), जडता (स्वाद के प्रति रसनादोष), अजिघ्रता (घ्राणदोष), मूकता (वाग्दोष), कौण्यं (ठूंठा होना, हाथ की शक्ति के अभावरुपीदोष), पङ्गुत्वं (= लंगडा होना), क्लैब्यं (नपुंसकता दोष), उदावर्त (वायुदोष) और मन्दता ( मन का दोष) ये ग्यारह अशक्तियाँ हुई। इन सबको बुद्धिवध भी कहा
जाता है।
1
विशेषार्थ : कारिका में प्रयुक्त 'वध' का, उपघात, विनाश, विकलता, असमर्थता रूप अर्थो की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है । बुद्धि इन्द्रियों के माध्यम से विषयों को प्राप्त करती है । इनमें से किसी भी इन्द्रिय की
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org