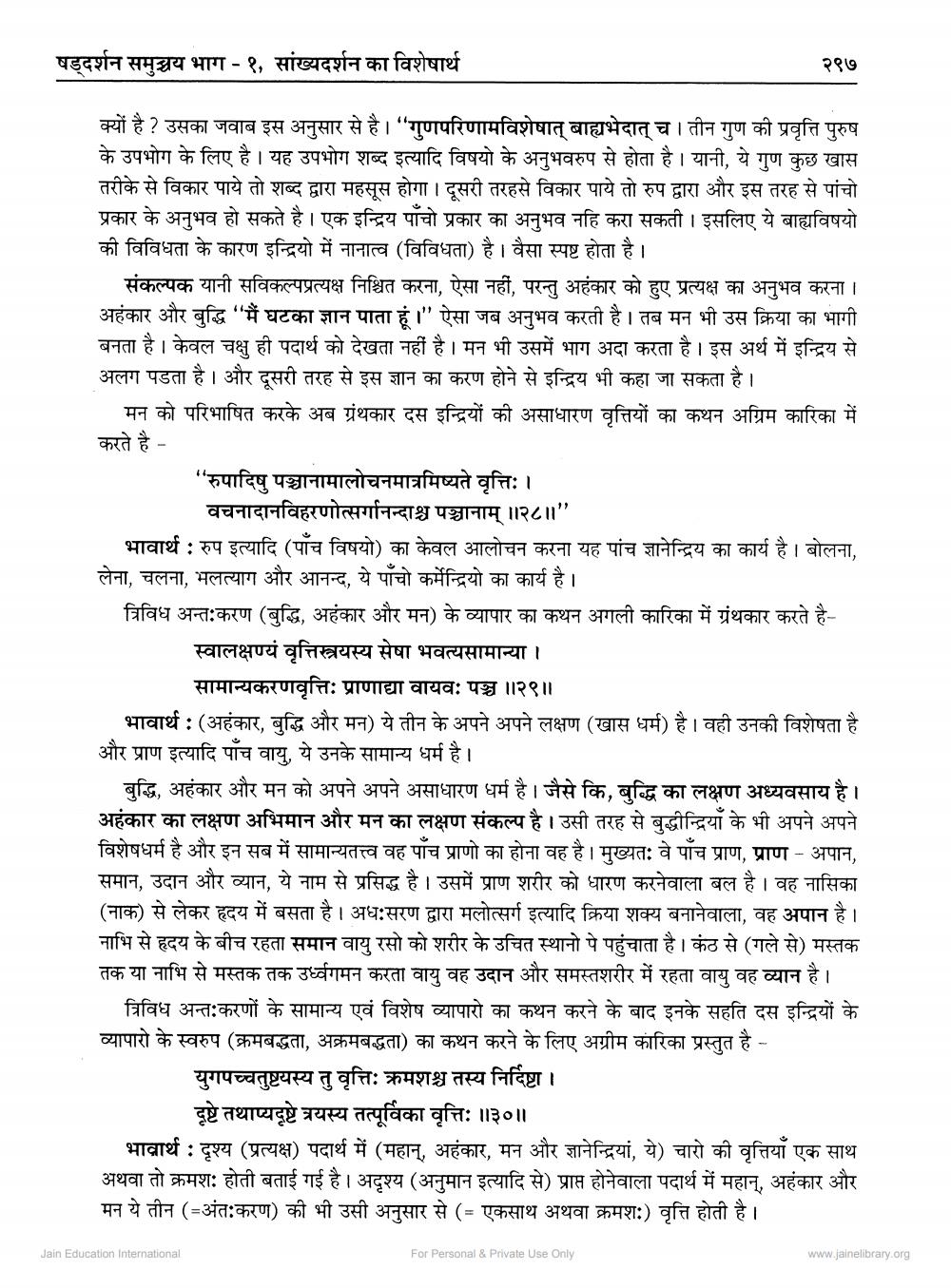________________
षड्दर्शन समुच्चय भाग -
१, सांख्यदर्शन का विशेषार्थ
क्यों है ? उसका जवाब इस अनुसार से है। " गुणपरिणामविशेषात् बाह्यभेदात् च । तीन गुण की प्रवृत्ति पुरुष के उपभोग के लिए है। यह उपभोग शब्द इत्यादि विषयो के अनुभवरूप से होता है। यानी, ये गुण कुछ खास तरीके से विकार पाये तो शब्द द्वारा महसूस होगा। दूसरी तरहसे विकार पाये तो रुप द्वारा और इस तरह से पांचो प्रकार के अनुभव हो सकते है । एक इन्द्रिय पाँचो प्रकार का अनुभव नहि करा सकती। इसलिए ये बाह्यविषयो की विविधता के कारण इन्द्रियो में नानात्व (विविधता) है। वैसा स्पष्ट होता है ।
संकल्पक यानी सविकल्पप्रत्यक्ष निश्चित करना, ऐसा नहीं, परन्तु अहंकार को हुए प्रत्यक्ष का अनुभव करना । अहंकार और बुद्धि "मैं घटका ज्ञान पाता हूं।" ऐसा जब अनुभव करती है। तब मन भी उस क्रिया का भागी बनता है । केवल चक्षु ही पदार्थ को देखता नहीं है। मन भी उसमें भाग अदा करता है । इस अर्थ में इन्द्रिय से अलग पड़ता है । और दूसरी तरह से इस ज्ञान का करण होने से इन्द्रिय भी कहा जा सकता है ।
I
२९७
मन को परिभाषित करके अब ग्रंथकार दस इन्द्रियों की असाधारण वृत्तियों का कथन अग्रिम कारिका में करते है -
"रुपादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः । वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम् ॥२८॥"
भावार्थ : रुप इत्यादि (पाँच विषयो) का केवल आलोचन करना यह पांच ज्ञानेन्द्रिय का कार्य है। बोलना, लेना, चलना, भलत्याग और आनन्द, ये पाँचो कर्मेन्द्रियो का कार्य है।
त्रिविध अन्त:करण (बुद्धि, अहंकार और मन ) के व्यापार का कथन अगली कारिका में ग्रंथकार करते हैस्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य सेषा भवत्यसामान्या ।
सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ २९॥
Jain Education International
भावार्थ : (अहंकार, बुद्धि और मन ) ये तीन के अपने अपने लक्षण (खास धर्म) है। वही उनकी विशेषता है और प्राण इत्यादि पाँच वायु, ये उनके सामान्य धर्म है ।
बुद्धि, अहंकार और मन को अपने अपने असाधारण धर्म है। जैसे कि, बुद्धि का लक्षण अध्यवसाय है । अहंकार का लक्षण अभिमान और मन का लक्षण संकल्प है । उसी तरह से बुद्धीन्द्रियाँ के भी अपने अपने विशेषधर्म है और इन सब में सामान्यतत्त्व वह पाँच प्राणो का होना वह है। मुख्यतः वे पाँच प्राण, प्राण अपान, समान, उदान और व्यान, ये नाम से प्रसिद्ध है । उसमें प्राण शरीर को धारण करनेवाला बल है । वह नासिका (नाक) से लेकर हृदय में बसता है । अधःसरण द्वारा मलोत्सर्ग इत्यादि क्रिया शक्य बनानेवाला, वह अपान है 1 नाभि से हृदय के बीच रहता समान वायु रसो को शरीर के उचित स्थानो पे पहुंचाता है। कंठ से (गले से) मस्तक तक या नाभि से मस्तक तक उर्ध्वगमन करता वायु वह उदान और समस्तशरीर में रहता वायु वह व्यान है । त्रिविध अन्तःकरणों के सामान्य एवं विशेष व्यापारो का कथन करने के बाद इनके सहति दस इन्द्रियों के व्यापारो के स्वरुप (क्रमबद्धता, अक्रमबद्धता) का कथन करने के लिए अग्रीम कारिका प्रस्तुत है - युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा ।
दृष्टे तथाप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः ॥३०॥
भावार्थ : दृश्य (प्रत्यक्ष) पदार्थ में (महान्, अहंकार, मन और ज्ञानेन्द्रियां, ये) चारो की वृत्तियाँ एक साथ अथवा तो क्रमश: होती बताई गई है। अदृश्य (अनुमान इत्यादि से) प्राप्त होनेवाला पदार्थ में महान्, अहंकार और मन ये तीन (=अंत:करण) की भी उसी अनुसार से ( एकसाथ अथवा क्रमश: ) वृत्ति होती है ।
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org