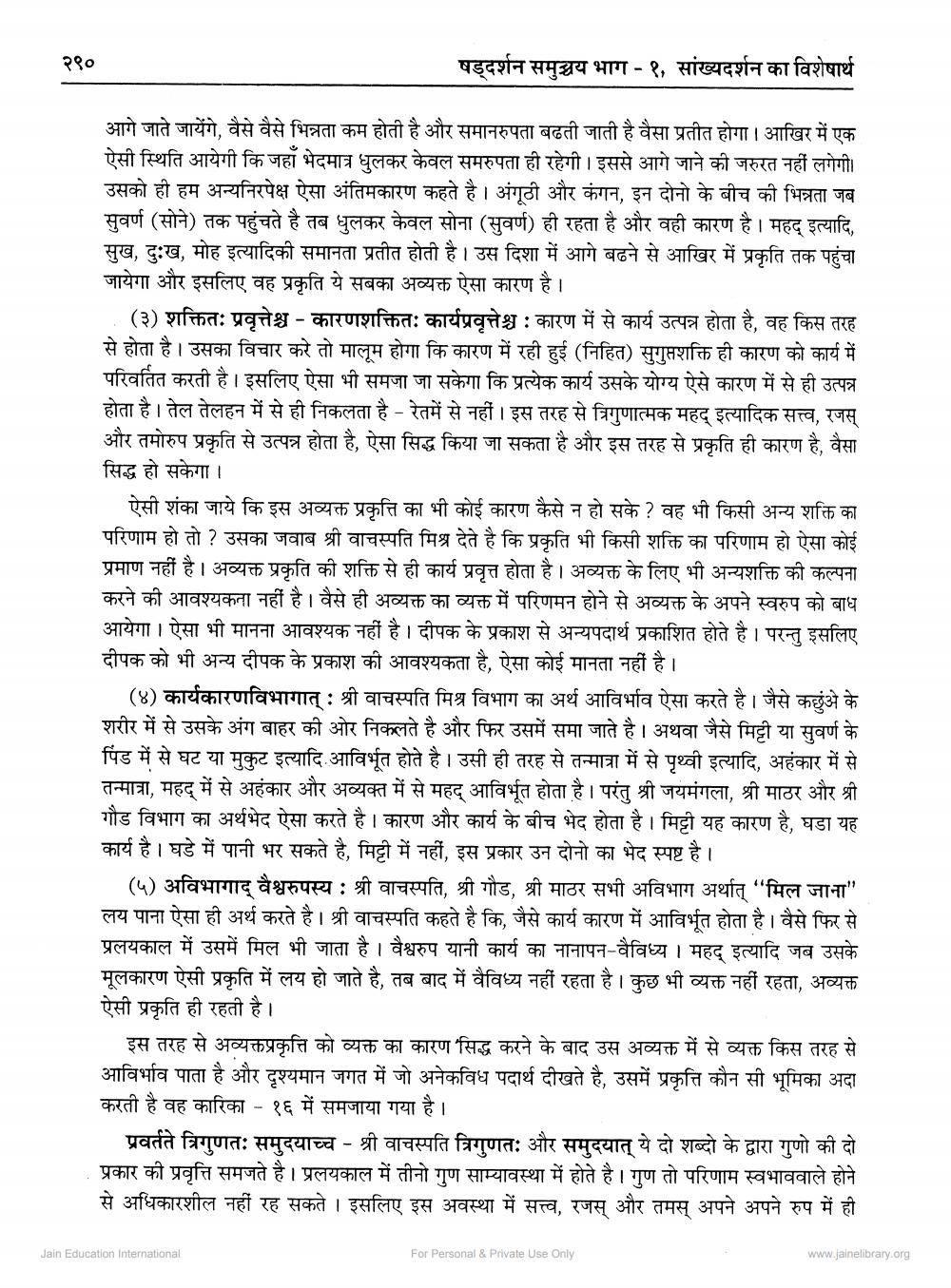________________
२९०
षड्दर्शन समुञ्चय भाग - १, सांख्यदर्शन का विशेषार्थ
आगे जाते जायेंगे, वैसे वैसे भिन्नता कम होती है और समानरुपता बढती जाती है वैसा प्रतीत होगा। आखिर में एक ऐसी स्थिति आयेगी कि जहाँ भेदमात्र धुलकर केवल समरुपता ही रहेगी। इससे आगे जाने की जरुरत नहीं लगेगी। उसको ही हम अन्यनिरपेक्ष ऐसा अंतिमकारण कहते है। अंगूठी और कंगन, इन दोनो के बीच की भिन्नता जब सुवर्ण (सोने) तक पहुंचते है तब धुलकर केवल सोना (सुवर्ण) ही रहता है और वही कारण है। महद् इत्यादि, सुख, दुःख, मोह इत्यादिकी समानता प्रतीत होती है। उस दिशा में आगे बढ़ने से आखिर में प्रकृति तक पहुंचा जायेगा और इसलिए वह प्रकृति ये सबका अव्यक्त ऐसा कारण है। . (३) शक्तितः प्रवृत्तेश्च - कारणशक्तितः कार्यप्रवृत्तेश्च : कारण में से कार्य उत्पन्न होता है, वह किस तरह से होता है। उसका विचार करे तो मालूम होगा कि कारण में रही हुई (निहित) सुगुप्तशक्ति ही कारण को कार्य में परिवर्तित करती है। इसलिए ऐसा भी समजा जा सकेगा कि प्रत्येक कार्य उसके योग्य ऐसे कारण में से ही उत्पन्न होता है। तेल तेलहन में से ही निकलता है - रेतमें से नहीं। इस तरह से त्रिगुणात्मक महद् इत्यादिक सत्त्व, रजस्
और तमोरुप प्रकृति से उत्पन्न होता है, ऐसा सिद्ध किया जा सकता है और इस तरह से प्रकृति ही कारण है, वैसा सिद्ध हो सकेगा।
ऐसी शंका जाये कि इस अव्यक्त प्रकृत्ति का भी कोई कारण कैसे न हो सके? वह भी किसी अन्य शक्ति का परिणाम हो तो? उसका जवाब श्री वाचस्पति मिश्र देते है कि प्रकृति भी किसी शक्ति का परिणाम हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। अव्यक्त प्रकृति की शक्ति से ही कार्य प्रवृत्त होता है। अव्यक्त के लिए भी अन्यशक्ति की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही अव्यक्त का व्यक्त में परिणमन होने से अव्यक्त के अपने स्वरुप को बाध आयेगा । ऐसा भी मानना आवश्यक नहीं है। दीपक के प्रकाश से अन्यपदार्थ प्रकाशित होते है। परन्तु इसलिए दीपक को भी अन्य दीपक के प्रकाश की आवश्यकता है, ऐसा कोई मानता नहीं है।
(४) कार्यकारणविभागात् : श्री वाचस्पति मिश्र विभाग का अर्थ आविर्भाव ऐसा करते है। जैसे कछुओ के शरीर में से उसके अंग बाहर की ओर निकलते है और फिर उसमें समा जाते है । अथवा जैसे मिट्टी या सुवर्ण के पिंड में से घट या मुकुट इत्यादि आविर्भूत होते है। उसी ही तरह से तन्मात्रा में से पृथ्वी इत्यादि, अहंकार में से तन्मात्रा, महद् में से अहंकार और अव्यक्त में से महद् आविर्भूत होता है। परंतु श्री जयमंगला, श्री माठर और श्री गौड विभाग का अर्थभेद ऐसा करते है। कारण और कार्य के बीच भेद होता है। मिट्टी यह कारण है, घडा यह कार्य है। घडे में पानी भर सकते है, मिट्टी में नहीं, इस प्रकार उन दोनो का भेद स्पष्ट है।
(५) अविभागाद् वैश्वरुपस्य : श्री वाचस्पति, श्री गौड, श्री माठर सभी अविभाग अर्थात् “मिल जाना" लय पाना ऐसा ही अर्थ करते है। श्री वाचस्पति कहते है कि, जैसे कार्य कारण में आविर्भूत होता है। वैसे फिर से प्रलयकाल में उसमें मिल भी जाता है। वैश्वरुप यानी कार्य का नानापन-वैविध्य । महद इत्यादि जब उसके मूलकारण ऐसी प्रकृति में लय हो जाते है, तब बाद में वैविध्य नहीं रहता है। कुछ भी व्यक्त नहीं रहता, अव्यक्त ऐसी प्रकृति ही रहती है।
इस तरह से अव्यक्तप्रकृत्ति को व्यक्त का कारण सिद्ध करने के बाद उस अव्यक्त में से व्यक्त किस तरह से आविर्भाव पाता है और दृश्यमान जगत में जो अनेकविध पदार्थ दीखते है, उसमें प्रकृत्ति कौन सी भूमिका अदा करती है वह कारिका - १६ में समजाया गया है।
प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च - श्री वाचस्पति त्रिगुणतः और समुदयात् ये दो शब्दो के द्वारा गुणो की दो प्रकार की प्रवृत्ति समजते है। प्रलयकाल में तीनो गुण साम्यावस्था में होते है । गुण तो परिणाम स्वभाववाले होने से अधिकारशील नहीं रह सकते । इसलिए इस अवस्था में सत्त्व, रजस् और तमस् अपने अपने रुप में ही
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org