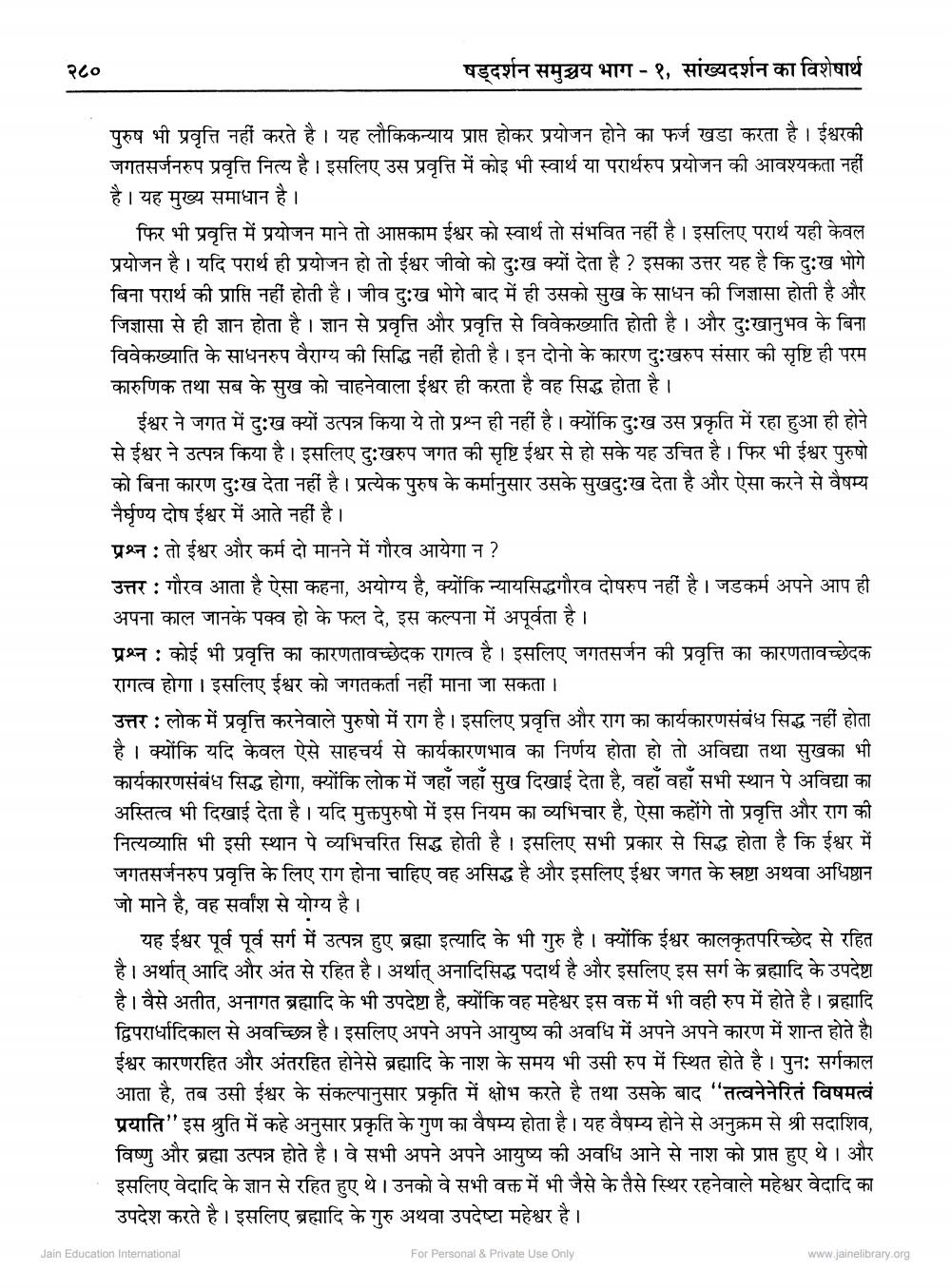________________
२८०
षड्दर्शन समुच्चय भाग - १, सांख्यदर्शन का विशेषार्थ
पुरुष भी प्रवृत्ति नहीं करते है । यह लौकिकन्याय प्राप्त होकर प्रयोजन होने का फर्ज खडा करता है । ईश्वरकी जगतसर्जनरुप प्रवृत्ति नित्य है । इसलिए उस प्रवृत्ति में कोइ भी स्वार्थ या परार्थरुप प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है । यह मुख्य समाधान है।
फिर भी प्रवृत्ति में प्रयोजन माने तो आप्तकाम ईश्वर को स्वार्थ तो संभवित नहीं है । इसलिए परार्थ यही केवल प्रयोजन है। यदि परार्थ ही प्रयोजन हो तो ईश्वर जीवो को दुःख क्यों देता है ? इसका उत्तर यह है कि दुःख भोगे बिना परार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। जीव दुःख भोगे बाद में ही उसको सुख के साधन की जिज्ञासा होती है और जिज्ञासा से ही ज्ञान होता है। ज्ञान से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से विवेकख्याति होती है । और दुःखानुभव के बिना विवेकख्याति के साधनरुप वैराग्य की सिद्धि नहीं होती है। इन दोनो के कारण दुःखरुप संसार की सृष्टि ही परम कारुणिक तथा सब के सुख को चाहनेवाला ईश्वर ही करता है वह सिद्ध होता है ।
ईश्वर ने जगत में दुःख क्यों उत्पन्न किया ये तो प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि दुःख उस प्रकृति में रहा हुआ ही होने ईश्वर ने उत्पन्न किया है। इसलिए दुःखरुप जगत की सृष्टि ईश्वर से हो सके यह उचित है। फिर भी ईश्वर पुरुषो को बिना कारण दुःख देता नहीं है। प्रत्येक पुरुष के कर्मानुसार उसके सुखदुःख देता है और ऐसा करने से वैषम्य नैर्घृण्य दोष ईश्वर में आते नहीं है ।
प्रश्न : तो ईश्वर और कर्म दो मानने में गौरव आयेगा न ?
उत्तर : गौरव आता है ऐसा कहना, अयोग्य है, क्योंकि न्यायसिद्धगौरव दोषरूप नहीं है । जडकर्म अपने आप ही अपना काल जानके पक्व हो के फल दे, इस कल्पना में अपूर्वता है ।
प्रश्न: कोई भी प्रवृत्ति का कारणतावच्छेदक रागत्व है। इसलिए जगतसर्जन की प्रवृत्ति का कारणतावच्छेदक रागत्व होगा । इसलिए ईश्वर को जगतकर्ता नहीं माना जा सकता ।
1
उत्तर : लोक में प्रवृत्ति करनेवाले पुरुषो में राग है। इसलिए प्रवृत्ति और राग का कार्यकारणसंबंध सिद्ध नहीं होता है । क्योंकि यदि केवल ऐसे साहचर्य से कार्यकारणभाव का निर्णय होता हो तो अविद्या तथा सुखका भी कार्यकारणसंबंध सिद्ध होगा, क्योंकि लोक में जहाँ जहाँ सुख दिखाई देता है, वहाँ वहाँ सभी स्थान पे अविद्या का अस्तित्व भी दिखाई देता है। यदि मुक्तपुरुषो में इस नियम का व्यभिचार है, ऐसा कहोंगे तो प्रवृत्ति और राग की नित्यव्याप्ति भी इसी स्थान पे व्यभिचरित सिद्ध होती है । इसलिए सभी प्रकार से सिद्ध होता है कि ईश्वर में जगतसर्जनरुप प्रवृत्ति के लिए राग होना चाहिए वह असिद्ध है और इसलिए ईश्वर जगत के स्रष्टा अथवा अधिष्ठान जो माने है, वह सर्वांश से योग्य है।
यह ईश्वर पूर्व पूर्व सर्ग में उत्पन्न हुए ब्रह्मा इत्यादि के भी गुरु है । क्योंकि ईश्वर कालकृतपरिच्छेद से रहित है। अर्थात् आदि और अंत से रहित है। अर्थात् अनादिसिद्ध पदार्थ है और इसलिए इस सर्ग के ब्रह्मादि के उपदेष्टा है। वैसे अतीत, अनागत ब्रह्मादि के भी उपदेष्टा है, क्योंकि वह महेश्वर इस वक्त में भी वही रुप में होते है । ब्रह्मादि द्विपरार्धादिकाल से अवच्छिन्न है । इसलिए अपने अपने आयुष्य की अवधि में अपने अपने कारण में शान्त होते है। ईश्वर कारणरहित और अंतरहित होनेसे ब्रह्मादि के नाश के समय भी उसी रुप में स्थित होते है । पुनः सर्गकाल आता है, तब उसी ईश्वर के संकल्पानुसार प्रकृति में क्षोभ करते है तथा उसके बाद "तत्वनेनेरितं विषमत्वं प्रयाति" इस श्रुति में कहे अनुसार प्रकृति के गुण का वैषम्य होता है। यह वैषम्य होने से अनुक्रम से श्री सदाशिव, विष्णु और ब्रह्मा उत्पन्न होते है । वे सभी अपने अपने आयुष्य की अवधि आने से नाश को प्राप्त हुए थे। और इसलिए वेदादि के ज्ञान से रहित हुए थे । उनको वे सभी वक्त में भी जैसे के तैसे स्थिर रहनेवाले महेश्वर वेदादि का उपदेश करते है। इसलिए ब्रह्मादि के गुरु अथवा उपदेष्टा महेश्वर है ।
1
For Personal & Private Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org