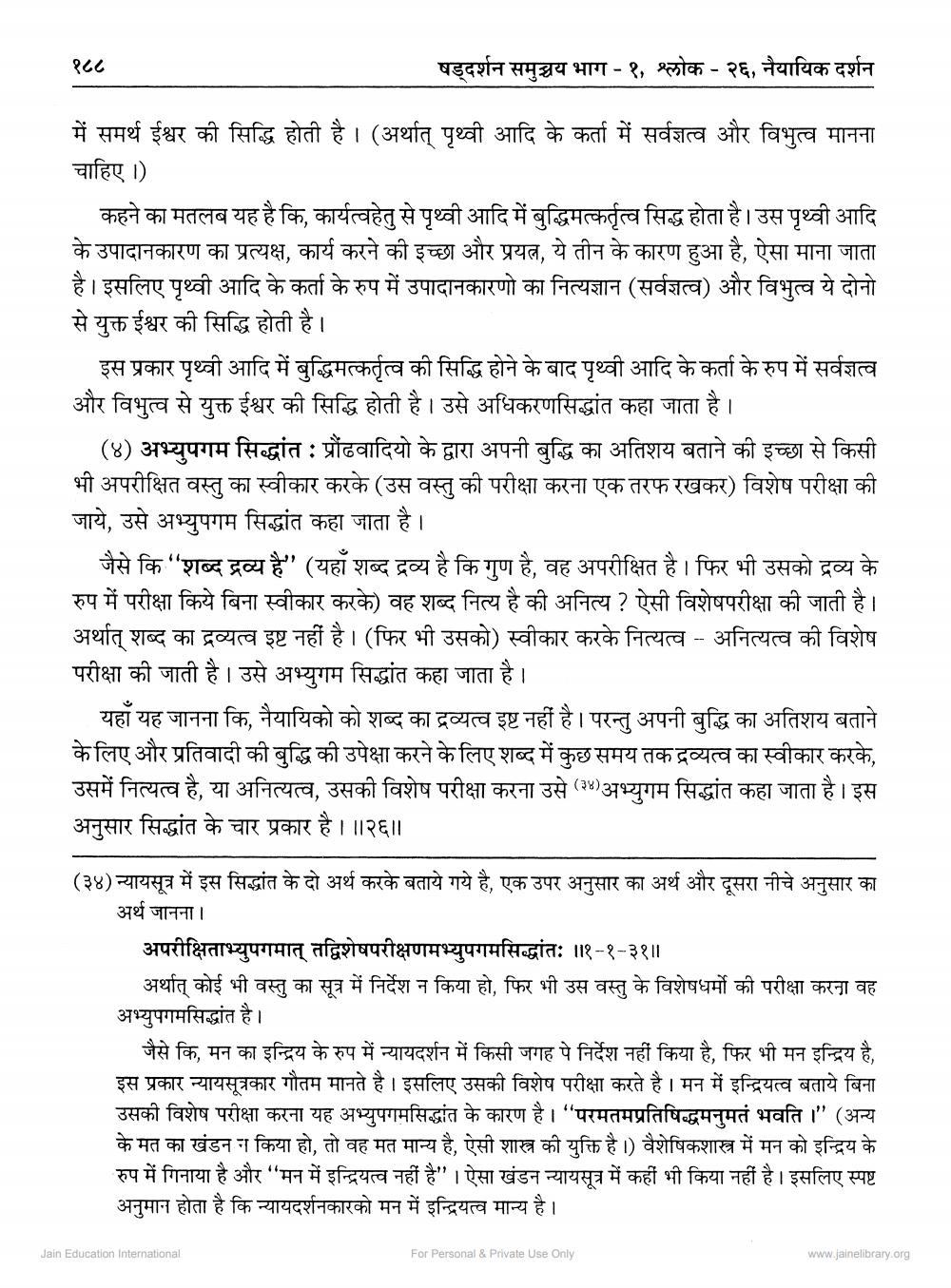________________
षड्दर्शन समुच्चय भाग - १, श्लोक - २६, नैयायिक दर्शन
में समर्थ ईश्वर की सिद्धि होती है । (अर्थात् पृथ्वी आदि के कर्ता में सर्वज्ञत्व और विभुत्व मानना चाहिए ।)
१८८
कहने का मतलब यह है कि, कार्यत्वहेतु से पृथ्वी आदि में बुद्धिमत्कर्तृत्व सिद्ध होता है। उस पृथ्वी आदि के उपादानकारण का प्रत्यक्ष, कार्य करने की इच्छा और प्रयत्न, ये तीन के कारण हुआ है, ऐसा माना जाता है। इसलिए पृथ्वी आदि के कर्ता के रुप में उपादानकारणो का नित्यज्ञान (सर्वज्ञत्व) और विभुत्व ये दोनो से युक्त ईश्वर की सिद्धि होती है।
इस प्रकार पृथ्वी आदि में बुद्धिमत्कर्तृत्व की सिद्धि होने के बाद पृथ्वी आदि के कर्ता के रुप में सर्वज्ञत्व और विभुत्व से युक्त ईश्वर की सिद्धि होती है। उसे अधिकरणसिद्धांत कहा जाता है ।
(४) अभ्युपगम सिद्धांत : प्रौढवादियो के द्वारा अपनी बुद्धि का अतिशय बताने की इच्छा से किसी भी अपरीक्षित वस्तु का स्वीकार करके (उस वस्तु की परीक्षा करना एक तरफ रखकर) विशेष परीक्षा की जाये, उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहा जाता है ।
जैसे कि “शब्द द्रव्य है” (यहाँ शब्द द्रव्य है कि गुण है, वह अपरीक्षित है। फिर भी उसको द्रव्य के रुप में परीक्षा किये बिना स्वीकार करके) वह शब्द नित्य है की अनित्य ? ऐसी विशेषपरीक्षा की जाती है । अर्थात् शब्द का द्रव्यत्व इष्ट नहीं है। (फिर भी उसको) स्वीकार करके नित्यत्व अनित्यत्व की विशेष परीक्षा की जाती है। उसे अभ्युगम सिद्धांत कहा जाता है
1
यहाँ यह जानना कि, नैयायिको को शब्द का द्रव्यत्व इष्ट नहीं है । परन्तु अपनी बुद्धि का अतिशय बताने के लिए और प्रतिवादी की बुद्धि की उपेक्षा करने के लिए शब्द में कुछ समय तक द्रव्यत्व का स्वीकार करके, उसमें नित्यत्व है, या अनित्यत्व, उसकी विशेष परीक्षा करना उसे (२४) अभ्युगम सिद्धांत कहा जाता है। इस अनुसार सिद्धांत के चार प्रकार है | ||२६||
(३४) न्यायसूत्र में इस सिद्धांत के दो अर्थ करके बताये गये है, एक उपर अनुसार का अर्थ और दूसरा नीचे अनुसार का अर्थ जानना ।
अपरीक्षिताभ्युपगमात् तद्विशेषपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धांतः ॥१-१-३१॥
अर्थात् कोई भी वस्तु का सूत्र में निर्देश न किया हो, फिर भी उस वस्तु के विशेषधर्मो की परीक्षा करना वह अभ्युपगमसिद्धांत है।
जैसे कि, मन का इन्द्रिय के रुप में न्यायदर्शन में किसी जगह पे निर्देश नहीं किया है, फिर भी मन इन्द्रिय है, इस प्रकार न्यायसूत्रकार गौतम मानते है। इसलिए उसकी विशेष परीक्षा करते है । मन में इन्द्रियत्व बताये बिना उसकी विशेष परीक्षा करना यह अभ्युपगमसिद्धांत के कारण है । "परमतमप्रतिषिद्धमनुमतं भवति ।" (अन्य के मत का खंडन न किया हो, तो वह मत मान्य है, ऐसी शास्त्र की युक्ति है।) वैशेषिकशास्त्र में मन को इन्द्रिय के रुप में गिनाया है और "मन में इन्द्रियत्व नहीं है"। ऐसा खंडन न्यायसूत्र में कहीं भी किया नहीं है। इसलिए स्पष्ट अनुमान होता है कि न्यायदर्शनकारको मन में इन्द्रियत्व मान्य 1
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org