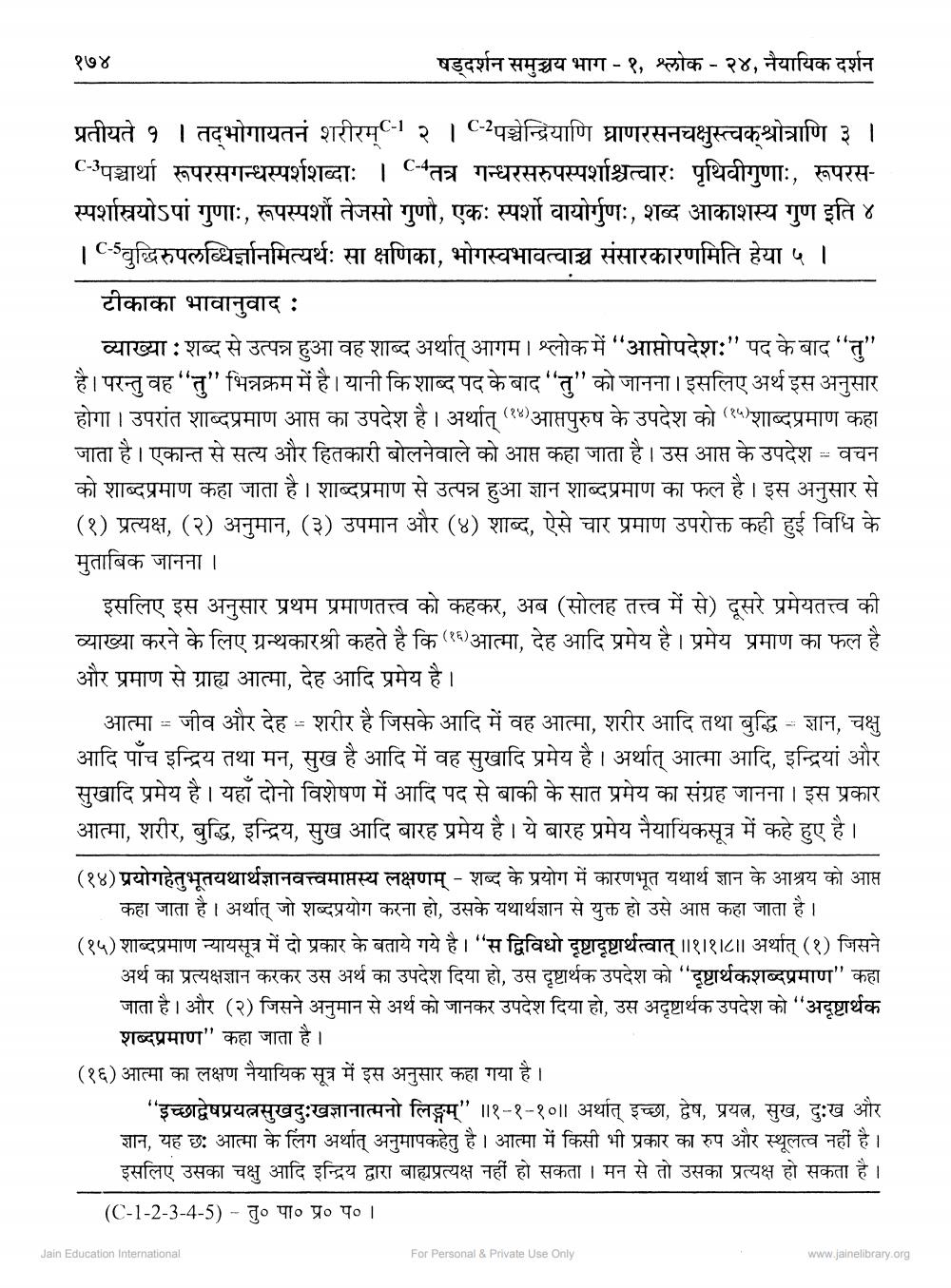________________
१७४
षड्दर्शन समुञ्चय भाग - १, श्लोक - २४, नैयायिक दर्शन
प्रतीयते १ । तद्भोगायतनं शरीरम्-1 २ । C--पञ्चेन्द्रियाणि घ्राणरसनचक्षुस्त्वक्श्रोत्राणि ३ । C-पञ्चार्था रूपरसगन्धस्पर्शशब्दाः । तत्र गन्धरसरुपस्पर्शाश्चत्वारः पृथिवीगुणाः, रूपरसस्पर्शास्रयोऽपां गुणाः, रूपस्पर्शी तेजसो गुणो, एकः स्पर्शो वायोर्गुणः, शब्द आकाशस्य गुण इति ४ । C-5बुद्धिरुपलब्धिर्ज्ञानमित्यर्थः सा क्षणिका, भोगस्वभावत्वाञ्च संसारकारणमिति हेया ५ ।।
टीकाका भावानुवाद :
व्याख्या : शब्द से उत्पन्न हुआ वह शाब्द अर्थात् आगम। श्लोक में "आप्तोपदेशः" पद के बाद "तु" है। परन्तु वह "तु" भिन्नक्रम में है। यानी कि शाब्द पद के बाद "तु" को जानना। इसलिए अर्थ इस अनुसार होगा। उपरांत शाब्दप्रमाण आप्त का उपदेश है। अर्थात् (१४)आप्तपुरुष के उपदेश को (१५)शाब्दप्रमाण कहा जाता है। एकान्त से सत्य और हितकारी बोलनेवाले को आप्त कहा जाता है। उस आप्त के उपदेश = वचन को शाब्दप्रमाण कहा जाता है। शाब्दप्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान शाब्दप्रमाण का फल है। इस अनुसार से (१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) उपमान और (४) शाब्द, ऐसे चार प्रमाण उपरोक्त कही हुई विधि के मुताबिक जानना ।
इसलिए इस अनुसार प्रथम प्रमाणतत्त्व को कहकर, अब (सोलह तत्त्व में से) दूसरे प्रमेयतत्त्व की व्याख्या करने के लिए ग्रन्थकारश्री कहते है कि (१६)आत्मा, देह आदि प्रमेय है। प्रमेय प्रमाण का फल है और प्रमाण से ग्राह्य आत्मा, देह आदि प्रमेय है।
आत्मा - जीव और देह = शरीर है जिसके आदि में वह आत्मा, शरीर आदि तथा बुद्धि - ज्ञान, चक्षु आदि पाँच इन्द्रिय तथा मन, सुख है आदि में वह सुखादि प्रमेय है। अर्थात् आत्मा आदि, इन्द्रियां और सुखादि प्रमेय है। यहाँ दोनो विशेषण में आदि पद से बाकी के सात प्रमेय का संग्रह जानना । इस प्रकार आत्मा, शरीर, बुद्धि, इन्द्रिय, सुख आदि बारह प्रमेय है। ये बारह प्रमेय नैयायिकसूत्र में कहे हुए है। (१४) प्रयोगहेतुभूतयथार्थज्ञानवत्त्वमाप्तस्य लक्षणम् - शब्द के प्रयोग में कारणभूत यथार्थ ज्ञान के आश्रय को आप्त
कहा जाता है। अर्थात् जो शब्दप्रयोग करना हो, उसके यथार्थज्ञान से युक्त हो उसे आप्त कहा जाता है। (१५) शाब्दप्रमाण न्यायसूत्र में दो प्रकार के बताये गये है। "स द्विविधो दृष्टादृष्टार्थत्वात् ॥१।१।८।। अर्थात् (१) जिसने
अर्थ का प्रत्यक्षज्ञान करकर उस अर्थ का उपदेश दिया हो, उस दृष्टार्थक उपदेश को "दृष्टार्थकशब्दप्रमाण" कहा जाता है। और (२) जिसने अनुमान से अर्थ को जानकर उपदेश दिया हो, उस अदृष्टार्थक उपदेश को "अदृष्टार्थक
शब्दप्रमाण" कहा जाता है। (१६) आत्मा का लक्षण नैयायिक सूत्र में इस अनुसार कहा गया है।
"इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानात्मनो लिङ्गम्" ॥१-१-१०॥ अर्थात् इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान, यह छ: आत्मा के लिंग अर्थात् अनुमापकहेतु है। आत्मा में किसी भी प्रकार का रुप और स्थूलत्व नहीं है। इसलिए उसका चक्षु आदि इन्द्रिय द्वारा बाह्यप्रत्यक्ष नहीं हो सकता । मन से तो उसका प्रत्यक्ष हो सकता है।
(C-1-2-3-4-5) - तु० पा० प्र० प० ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org