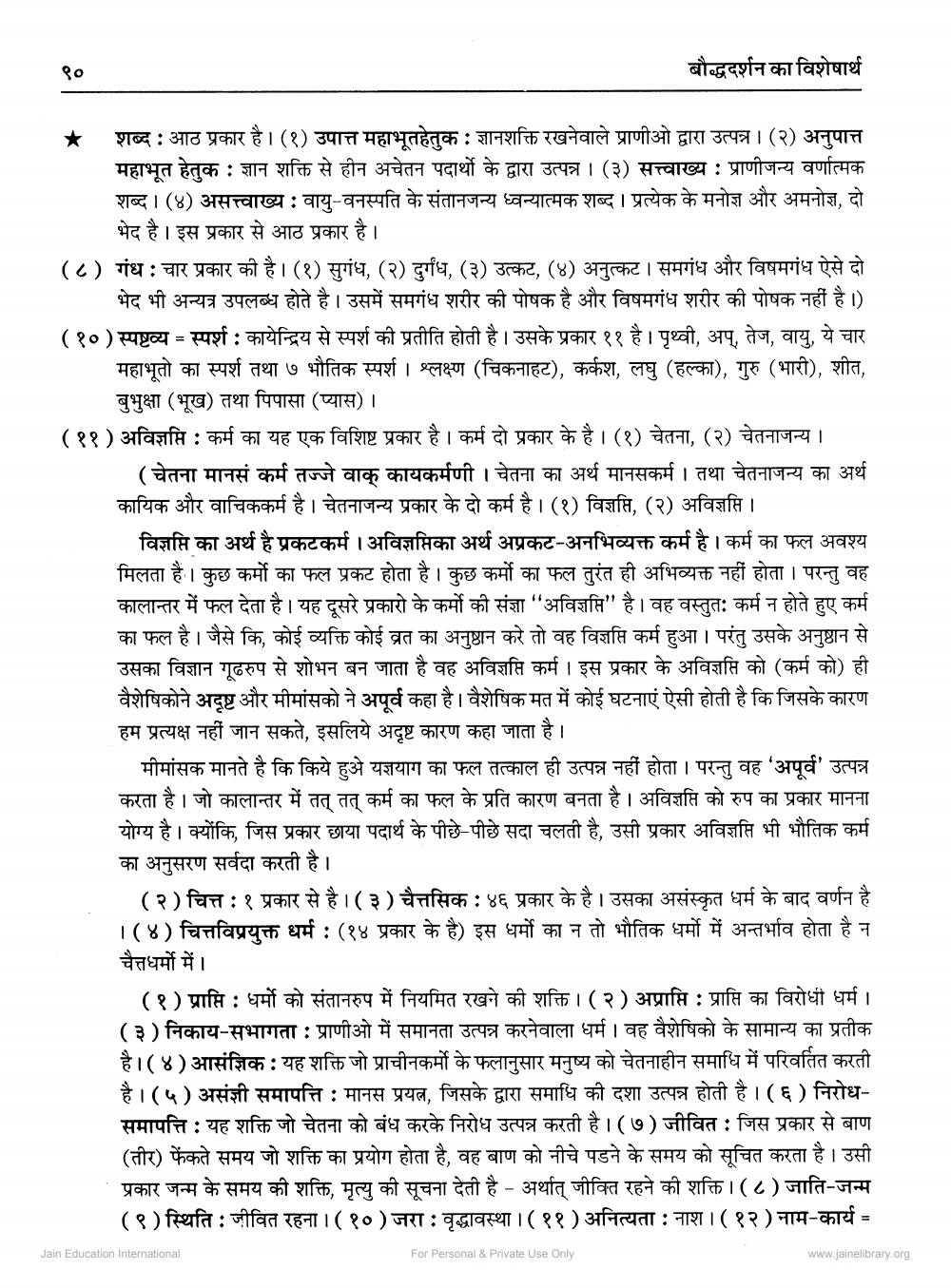________________
९०
★
बौद्धदर्शन का विशेषार्थ
शब्द : आठ प्रकार है । (१) उपात्त महाभूतहेतुक : ज्ञानशक्ति रखनेवाले प्राणीओ द्वारा उत्पन्न । (२) अनुपात्त महाभूत हेतुक : ज्ञान शक्ति से हीन अचेतन पदार्थो के द्वारा उत्पन्न । (३) सत्त्वाख्य: प्राणीजन्य वर्णात्मक शब्द । (४) असत्त्वाख्य : वायु-वनस्पति के संतानजन्य ध्वन्यात्मक शब्द । प्रत्येक के मनोज्ञ और अमनोज्ञ, दो भेद है। इस प्रकार से आठ प्रकार है ।
(८) गंध : चार प्रकार की है। (१) सुगंध, (२) दुर्गंध, (३) उत्कट, (४) अनुत्कट । समगंध और विषमगंध ऐसे दो भेद भी अन्यत्र उपलब्ध होते है। उसमें समगंध शरीर की पोषक है और विषमगंध शरीर की पोषक नहीं है ।)
( १० ) स्पष्टव्य = स्पर्श : कायेन्द्रिय से स्पर्श की प्रतीति होती है। उसके प्रकार ११ है । पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, ये चार महाभूतो का स्पर्श तथा ७ भौतिक स्पर्श । श्लक्ष्ण (चिकनाहट), कर्कश, लघु (हल्का), गुरु (भारी), शीत, बुभुक्षा (भूख) तथा पिपासा (प्यास) ।
(११) अविज्ञप्ति : कर्म का यह एक विशिष्ट प्रकार है। कर्म दो प्रकार के है। (१) चेतना, (२) चेतनाजन्य ।
( चेतना मानसं कर्म तज्जे वाक् कायकर्मणी । चेतना का अर्थ मानसकर्म । तथा चेतनाजन्य का अर्थ कायिक और वाचिककर्म है। चेतनाजन्य प्रकार के दो कर्म है । (१) विज्ञप्ति, (२) अविज्ञप्ति ।
विज्ञप्ति का अर्थ है प्रकटकर्म । अविज्ञप्तिका अर्थ अप्रकट-अनभिव्यक्त कर्म है । कर्म का फल अवश्य मिलता हैं । कुछ कर्मो का फल प्रकट होता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत ही अभिव्यक्त नहीं होता । परन्तु वह कालान्तर में फल देता है। यह दूसरे प्रकारो के कर्मो की संज्ञा "अविज्ञप्ति " है। वह वस्तुत: कर्म न होते हुए कर्म का फल है। जैसे कि, कोई व्यक्ति कोई व्रत का अनुष्ठान करे तो वह विज्ञप्ति कर्म हुआ । परंतु उसके अनुष्ठान से उसका विज्ञान गूढरुप से शोभन बन जाता है वह अविज्ञप्ति कर्म । इस प्रकार के अविज्ञप्ति को (कर्म को) ही वैशेषिकोने अदृष्ट और मीमांसको ने अपूर्व कहा है। वैशेषिक मत में कोई घटनाएं ऐसी होती है कि जिसके कारण हम प्रत्यक्ष नहीं जान सकते, इसलिये अदृष्ट कारण कहा जाता है ।
मीमांसक मानते है कि किये हुये यज्ञयाग का फल तत्काल ही उत्पन्न नहीं होता । परन्तु वह 'अपूर्व' उत्पन्न करता है। जो कालान्तर में तत् तत् कर्म का फल के प्रति कारण बनता है । अविज्ञप्ति को रुप का प्रकार मानना योग्य है। क्योंकि, जिस प्रकार छाया पदार्थ के पीछे-पीछे सदा चलती है, उसी प्रकार अविज्ञप्ति भी भौतिक कर्म का अनुसरण सर्वदा करती है।
(२) चित्त : १ प्रकार से है । ( ३ ) चैत्तसिक : ४६ प्रकार के है । उसका असंस्कृत धर्म के बाद वर्णन है। । ( ४ ) चित्तविप्रयुक्त धर्म : (१४ प्रकार के है) इस धर्मो का न तो भौतिक धर्मो में अन्तर्भाव होता है न चैत्तधर्मो में ।
(१) प्राप्ति : धर्मो को संतानरुप में नियमित रखने की शक्ति । (२) अप्राप्ति: प्राप्ति का विरोधी धर्म । (३) निकाय सभागता : प्राणीओ में समानता उत्पन्न करनेवाला धर्म। वह वैशेषिको के सामान्य का प्रतीक है । ( ४ ) आसंज्ञिक : यह शक्ति जो प्राचीनकर्मों के फलानुसार मनुष्य को चेतनाहीन समाधि में परिवर्तित करती है । (५) असंज्ञी समापत्ति : मानस प्रयत्न, जिसके द्वारा समाधि की दशा उत्पन्न होती है। ( ६ ) निरोधसमापत्ति : यह शक्ति जो चेतना को बंध करके निरोध उत्पन्न करती है । (७) जीवित : जिस प्रकार से बा (तीर) फेंकते समय जो शक्ति का प्रयोग होता है, वह बाण को नीचे पडने के समय को सूचित करता है । उसी प्रकार जन्म के समय की शक्ति, मृत्यु की सूचना देती है - अर्थात् जीवित रहने की शक्ति । ( ८ ) जाति - जन्म (९) स्थिति : जीवित रहना । (१०) जरा : वृद्धावस्था । ( ११ ) अनित्यता : नाश। ( १२ ) नाम-कार्य
For Personal & Private Use Only
Jain Education International
=
www.jainelibrary.org