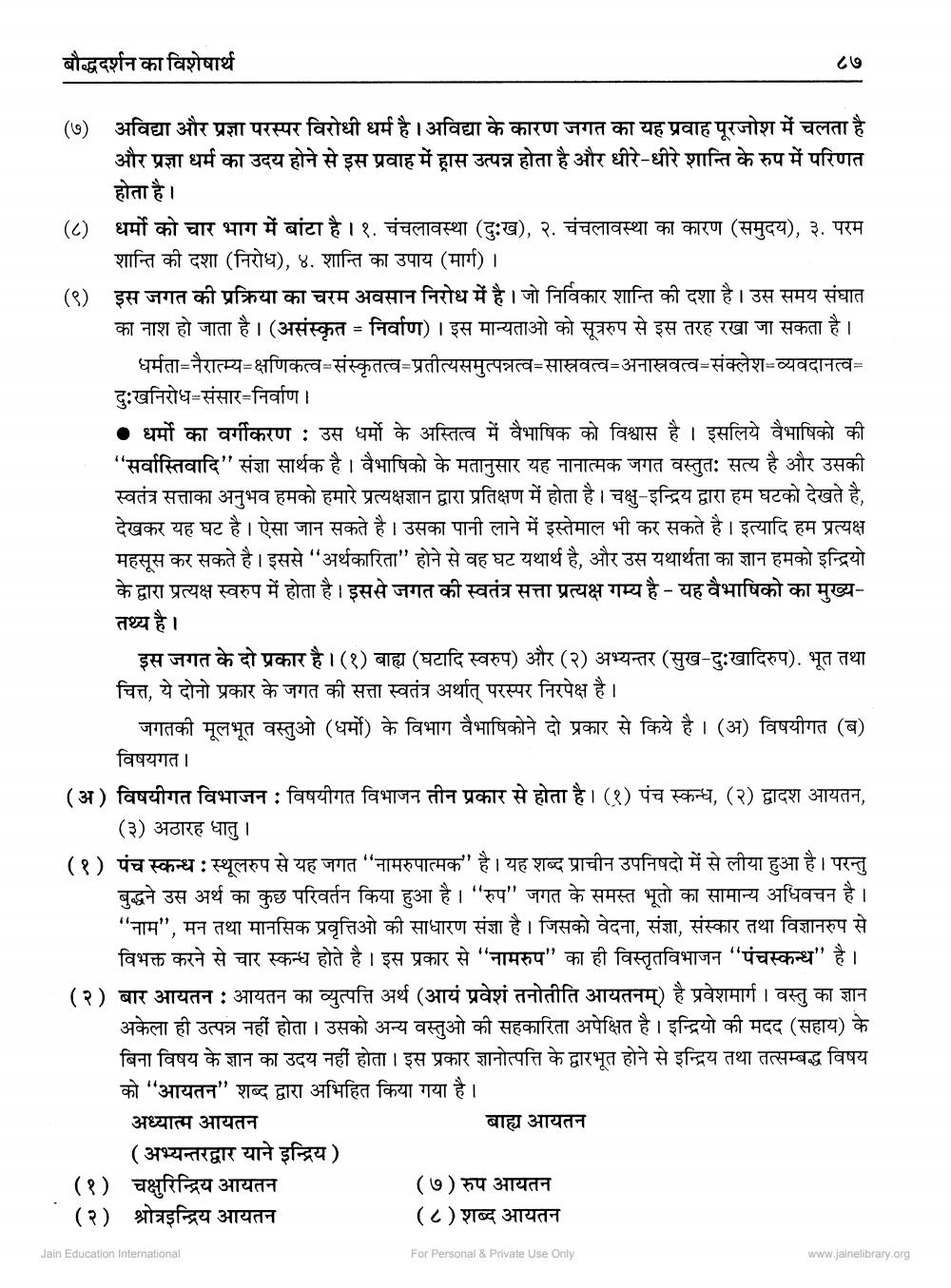________________
बौद्धदर्शन का विशेषार्थ
(७) अविद्या और प्रज्ञा परस्पर विरोधी धर्म है। अविद्या के कारण जगत का यह प्रवाह पूरजोश में चलता है
और प्रज्ञा धर्म का उदय होने से इस प्रवाह में हास उत्पन्न होता है और धीरे-धीरे शान्ति के रुप में परिणत
होता है। (८) धर्मों को चार भाग में बांटा है। १. चंचलावस्था (दःख), २. चंचलावस्था का कारण (समदय), ३. परम
शान्ति की दशा (निरोध), ४. शान्ति का उपाय (मार्ग)। (९) इस जगत की प्रक्रिया का चरम अवसान निरोध में है। जो निर्विकार शान्ति की दशा है। उस समय संघात
का नाश हो जाता है। (असंस्कृत = निर्वाण)। इस मान्यताओ को सूत्ररुप से इस तरह रखा जा सकता है।
धर्मता नैरात्म्य क्षणिकत्व संस्कृतत्व-प्रतीत्यसमुत्पन्नत्व-सास्रवत्व-अनास्रवत्व-संक्लेश-व्यवदानत्व दःखनिरोध संसार निर्वाण। • धर्मों का वर्गीकरण : उस धर्मो के अस्तित्व में वैभाषिक को विश्वास है । इसलिये वैभाषिको की "सर्वास्तिवादि" संज्ञा सार्थक है। वैभाषिको के मतानुसार यह नानात्मक जगत वस्तुतः सत्य है और उसकी स्वतंत्र सत्ताका अनुभव हमको हमारे प्रत्यक्षज्ञान द्वारा प्रतिक्षण में होता है। चक्षु-इन्द्रिय द्वारा हम घटको देखते है, देखकर यह घट है। ऐसा जान सकते है। उसका पानी लाने में इस्तेमाल भी कर सकते है । इत्यादि हम प्रत्यक्ष महसूस कर सकते है। इससे "अर्थकारिता" होने से वह घट यथार्थ है, और उस यथार्थता का ज्ञान हमको इन्द्रियो के द्वारा प्रत्यक्ष स्वरुप में होता है। इससे जगत की स्वतंत्र सत्ता प्रत्यक्ष गम्य है - यह वैभाषिको का मुख्यतथ्य है।
इस जगत के दो प्रकार है। (१) बाह्य (घटादि स्वरुप) और (२) अभ्यन्तर (सुख-दुःखादिरुप). भूत तथा चित्त, ये दोनो प्रकार के जगत की सत्ता स्वतंत्र अर्थात् परस्पर निरपेक्ष है।
जगतकी मूलभूत वस्तुओ (धर्मो) के विभाग वैभाषिकोने दो प्रकार से किये है । (अ) विषयीगत (ब)
विषयगत। (अ) विषयीगत विभाजन : विषयीगत विभाजन तीन प्रकार से होता है। (१) पंच स्कन्ध, (२) द्वादश आयतन,
(३) अठारह धातु । (१) पंच स्कन्ध : स्थूलरुप से यह जगत "नामरुपात्मक" है। यह शब्द प्राचीन उपनिषदो में से लीया हुआ है। परन्तु
बुद्धने उस अर्थ का कुछ परिवर्तन किया हुआ है । "रुप" जगत के समस्त भूतो का सामान्य अधिवचन है । "नाम", मन तथा मानसिक प्रवृत्तिओ की साधारण संज्ञा है। जिसको वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञानरुप से विभक्त करने से चार स्कन्ध होते है । इस प्रकार से "नामरुप" का ही विस्तृतविभाजन "पंचस्कन्ध" है। बार आयतन : आयतन का व्युत्पत्ति अर्थ (आयं प्रवेशं तनोतीति आयतनम्) है प्रवेशमार्ग । वस्तु का ज्ञान अकेला ही उत्पन्न नहीं होता । उसको अन्य वस्तुओ की सहकारिता अपेक्षित है। इन्द्रियो की मदद (सहाय) के बिना विषय के ज्ञान का उदय नहीं होता। इस प्रकार ज्ञानोत्पत्ति के द्वारभूत होने से इन्द्रिय तथा तत्सम्बद्ध विषय को "आयतन" शब्द द्वारा अभिहित किया गया है। अध्यात्म आयतन
बाह्य आयतन (अभ्यन्तरद्वार याने इन्द्रिय) (१) चक्षुरिन्द्रिय आयतन
(७)रुप आयतन - (२) श्रोत्रइन्द्रिय आयतन
(८)शब्द आयतन
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org