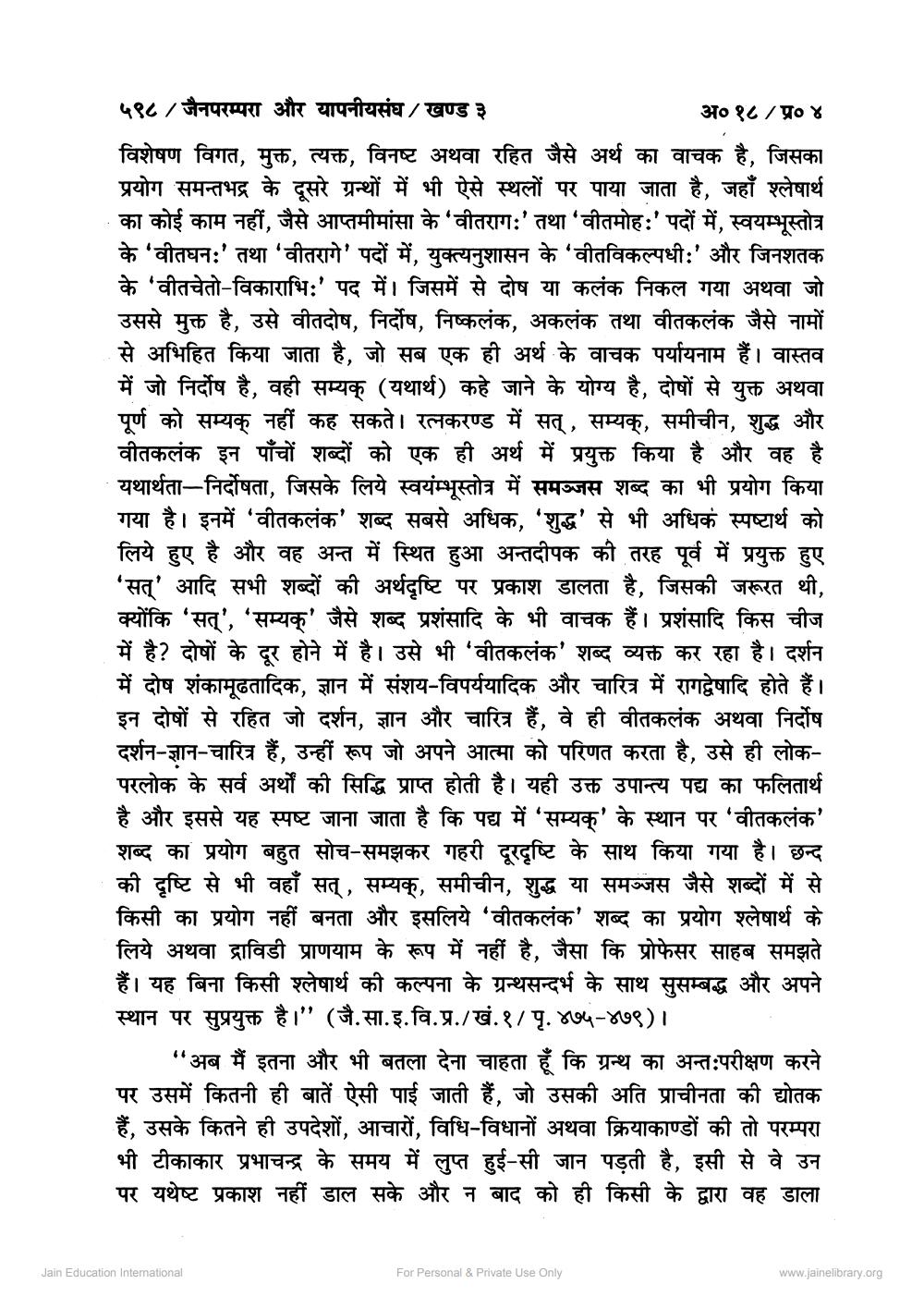________________
५९८ / जैनपरम्परा और यापनीयसंघ / खण्ड ३
अ०१८ / प्र० ४
विशेषण विगत, मुक्त, त्यक्त, विनष्ट अथवा रहित जैसे अर्थ का वाचक है, जिसका प्रयोग समन्तभद्र के दूसरे ग्रन्थों में भी ऐसे स्थलों पर पाया जाता है, जहाँ श्लेषार्थ का कोई काम नहीं, जैसे आप्तमीमांसा के 'वीतरागः ' तथा 'वीतमोह: ' पदों में, स्वयम्भूस्तोत्र के 'वीतघनः' तथा 'वीतरागे' पदों में, युक्त्यनुशासन के 'वीतविकल्पधी : ' और जिनशतक के 'वीतचेतो - विकाराभिः ' पद में। जिसमें से दोष या कलंक निकल गया अथवा जो उससे मुक्त है, उसे वीतदोष, निर्दोष, निष्कलंक, अकलंक तथा वीतकलंक जैसे नामों से अभिहित किया जाता है, जो सब एक ही अर्थ के वाचक पर्यायनाम हैं। वास्तव में जो निर्दोष है, वही सम्यक् ( यथार्थ ) कहे जाने के योग्य है, दोषों से युक्त अथवा पूर्ण को सम्यक् नहीं कह सकते। रत्नकरण्ड में सत्, सम्यक् समीचीन, शुद्ध और वीतकलंक इन पाँचों शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है और वह है यथार्थता - निर्दोषता, जिसके लिये स्वयंम्भूस्तोत्र में समञ्जस शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इनमें 'वीतकलंक' शब्द सबसे अधिक, 'शुद्ध' से भी अधिक स्पष्टार्थ को लिये हुए है और वह अन्त में स्थित हुआ अन्तदीपक की तरह पूर्व में प्रयुक्त हुए 'सत्' आदि सभी शब्दों की अर्थदृष्टि पर प्रकाश डालता है, जिसकी जरूरत थी, क्योंकि 'सत्', 'सम्यक्' जैसे शब्द प्रशंसादि के भी वाचक हैं। प्रशंसादि किस चीज में है? दोषों के दूर होने में है । उसे भी 'वीतकलंक' शब्द व्यक्त कर रहा है। दर्शन में दोष शंकामूढतादिक, ज्ञान में संशय-विपर्ययादिक और चारित्र में रागद्वेषादि होते हैं । इन दोषों से रहित जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं, वे ही वीतकलंक अथवा निर्दोष दर्शन - ज्ञान - चारित्र हैं, उन्हीं रूप जो अपने आत्मा को परिणत करता है, उसे ही लोकपरलोक के सर्व अर्थों की सिद्धि प्राप्त होती है । यही उक्त उपान्त्य पद्य का फलितार्थ है और इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि पद्य में 'सम्यक्' के स्थान पर 'वीतकलंक' शब्द का प्रयोग बहुत सोच-समझकर गहरी दूरदृष्टि के साथ किया गया है । छन्द की दृष्टि से भी वहाँ सत्, सम्यक्, समीचीन, शुद्ध या समञ्जस जैसे शब्दों में से किसी का प्रयोग नहीं बनता और इसलिये 'वीतकलंक' शब्द का प्रयोग श्लेषार्थ के लिये अथवा द्राविडी प्राणयाम के रूप में नहीं है, जैसा कि प्रोफेसर साहब समझते हैं। यह बिना किसी श्लेषार्थ की कल्पना के ग्रन्थसन्दर्भ के साथ सुसम्बद्ध और अपने स्थान पर सुप्रयुक्त है।" (जै. सा. इ.वि.प्र. / खं.१/ पृ. ४७५-४७९)।
44
'अब मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि ग्रन्थ का अन्तःपरीक्षण करने पर उसमें कितनी ही बातें ऐसी पाई जाती हैं, जो उसकी अति प्राचीनता की द्योतक हैं, उसके कितने ही उपदेशों, आचारों, विधि-विधानों अथवा क्रियाकाण्डों की तो परम्परा भी टीकाकार प्रभाचन्द्र के समय में लुप्त हुई-सी जान पड़ती है, इसी से वे उन पर यथेष्ट प्रकाश नहीं डाल सके और न बाद को ही किसी के द्वारा वह डाला
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org