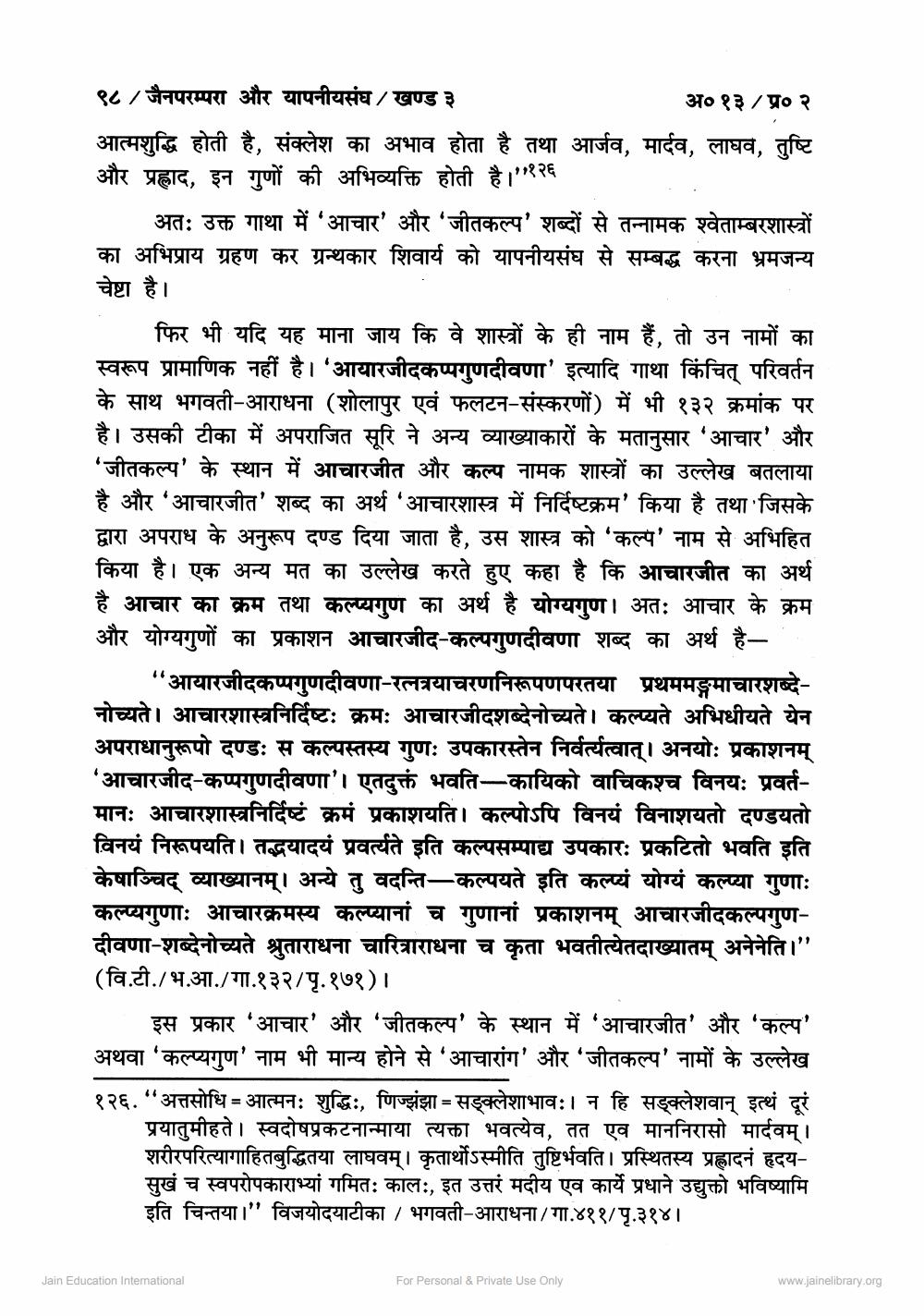________________
९८ / जैनपरम्परा और यापनीयसंघ / खण्ड ३
अ०१३ / प्र०२ आत्मशुद्धि होती है, संक्लेश का अभाव होता है तथा आर्जव, मार्दव, लाघव, तुष्टि और प्रह्लाद, इन गुणों की अभिव्यक्ति होती है।"१२६
अतः उक्त गाथा में 'आचार' और 'जीतकल्प' शब्दों से तन्नामक श्वेताम्बरशास्त्रों का अभिप्राय ग्रहण कर ग्रन्थकार शिवार्य को यापनीयसंघ से सम्बद्ध करना भ्रमजन्य चेष्टा है।
फिर भी यदि यह माना जाय कि वे शास्त्रों के ही नाम हैं, तो उन नामों का स्वरूप प्रामाणिक नहीं है। 'आयारजीदकप्पगुणदीवणा' इत्यादि गाथा किंचित् परिवर्तन के साथ भगवती-आराधना (शोलापुर एवं फलटन-संस्करणों) में भी १३२ क्रमांक पर है। उसकी टीका में अपराजित सूरि ने अन्य व्याख्याकारों के मतानुसार 'आचार' और 'जीतकल्प' के स्थान में आचारजीत और कल्प नामक शास्त्रों का उल्लेख बतलाया है और 'आचारजीत' शब्द का अर्थ 'आचारशास्त्र में निर्दिष्टक्रम' किया है तथा जिसके द्वारा अपराध के अनुरूप दण्ड दिया जाता है, उस शास्त्र को 'कल्प' नाम से अभिहित किया है। एक अन्य मत का उल्लेख करते हुए कहा है कि आचारजीत का अर्थ है आचार का क्रम तथा कल्प्यगुण का अर्थ है योग्यगुण। अतः आचार के क्रम और योग्यगुणों का प्रकाशन आचारजीद-कल्पगुणदीवणा शब्द का अर्थ है
___ "आयारजीदकप्पगुणदीवणा-रत्नत्रयाचरणनिरूपणपरतया प्रथममङ्गमाचारशब्देनोच्यते। आचारशास्त्रनिर्दिष्टः क्रमः आचारजीदशब्देनोच्यते। कल्प्यते अभिधीयते येन अपराधानुरूपो दण्डः स कल्पस्तस्य गुणः उपकारस्तेन निर्वर्त्यत्वात्। अनयोः प्रकाशनम् 'आचारजीद-कप्पगुणदीवणा'। एतदुक्तं भवति-कायिको वाचिकश्च विनयः प्रवर्तमानः आचारशास्त्रनिर्दिष्टं क्रमं प्रकाशयति। कल्पोऽपि विनयं विनाशयतो दण्डयतो विनयं निरूपयति। तद्भयादयं प्रवर्त्यते इति कल्पसम्पाद्य उपकारः प्रकटितो भवति इति केषाञ्चिद् व्याख्यानम्। अन्ये तु वदन्ति-कल्पयते इति कल्प्यं योग्यं कल्प्या गुणाः कल्प्यगुणाः आचारक्रमस्य कल्प्यानां च गुणानां प्रकाशनम् आचारजीदकल्पगुणदीवणा-शब्देनोच्यते श्रुताराधना चारित्राराधना च कृता भवतीत्येतदाख्यातम् अनेनेति।" (वि.टी./भ.आ./गा.१३२/पृ.१७१)।
इस प्रकार 'आचार' और 'जीतकल्प' के स्थान में 'आचारजीत' और 'कल्प' अथवा 'कल्प्यगुण' नाम भी मान्य होने से 'आचारांग' और 'जीतकल्प' नामों के उल्लेख १२६. "अत्तसोधि = आत्मनः शुद्धिः, णिज्झंझा = सङ्क्लेशाभावः। न हि सङ्क्लेशवान् इत्थं दूर
प्रयातुमीहते। स्वदोषप्रकटनान्माया त्यक्ता भवत्येव, तत एव माननिरासो मार्दवम्। शरीरपरित्यागाहितबुद्धितया लाघवम्। कृतार्थोऽस्मीति तुष्टिर्भवति। प्रस्थितस्य प्रह्लादनं हृदयसुखं च स्वपरोपकाराभ्यां गमितः कालः, इत उत्तरं मदीय एव कार्ये प्रधाने उद्युक्तो भविष्यामि इति चिन्तया।" विजयोदयाटीका / भगवती-आराधना / गा.४११/पृ.३१४ ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org