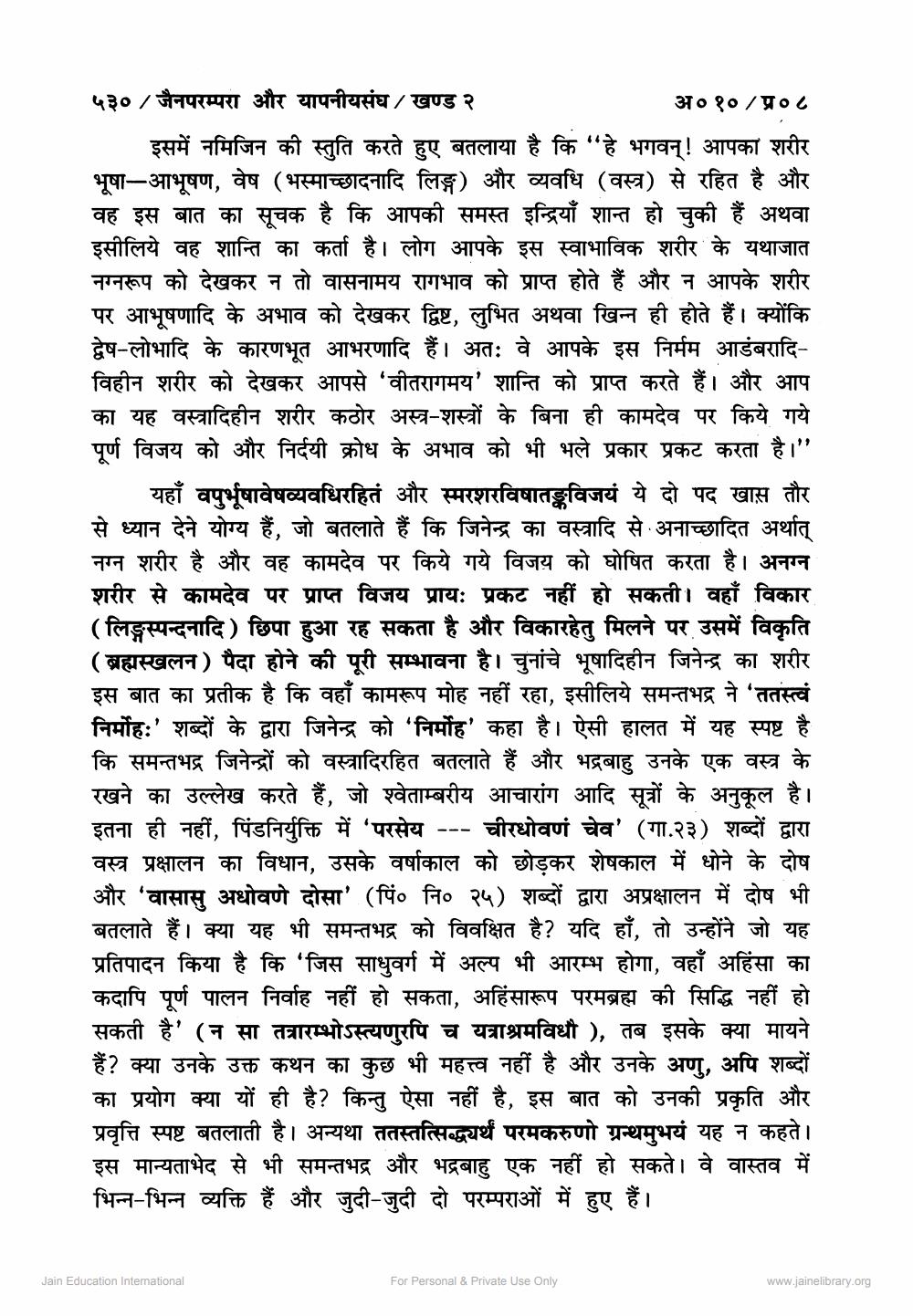________________
५३० / जैनपरम्परा और यापनीयसंघ / खण्ड २
अ०१०/प्र०८ इसमें नमिजिन की स्तुति करते हुए बतलाया है कि "हे भगवन्! आपका शरीर भूषा-आभूषण, वेष (भस्माच्छादनादि लिङ्ग) और व्यवधि (वस्त्र) से रहित है और वह इस बात का सूचक है कि आपकी समस्त इन्द्रियाँ शान्त हो चुकी हैं अथवा इसीलिये वह शान्ति का कर्ता है। लोग आपके इस स्वाभाविक शरीर के यथाजात नग्नरूप को देखकर न तो वासनामय रागभाव को प्राप्त होते हैं और न आपके शरीर पर आभूषणादि के अभाव को देखकर द्विष्ट, लुभित अथवा खिन्न ही होते हैं। क्योंकि द्वेष-लोभादि के कारणभूत आभरणादि हैं। अतः वे आपके इस निर्मम आडंबरादिविहीन शरीर को देखकर आपसे 'वीतरागमय' शान्ति को प्राप्त करते हैं। और आप का यह वस्त्रादिहीन शरीर कठोर अस्त्र-शस्त्रों के बिना ही कामदेव पर किये गये पूर्ण विजय को और निर्दयी क्रोध के अभाव को भी भले प्रकार प्रकट करता है।"
यहाँ वपुर्भूषावेषव्यवधिरहितं और स्मरशरविषातङ्कविजयं ये दो पद खास तौर से ध्यान देने योग्य हैं, जो बतलाते हैं कि जिनेन्द्र का वस्त्रादि से अनाच्छादित अर्थात् नग्न शरीर है और वह कामदेव पर किये गये विजय को घोषित करता है। अनग्न शरीर से कामदेव पर प्राप्त विजय प्रायः प्रकट नहीं हो सकती। वहाँ विकार (लिङ्गस्पन्दनादि) छिपा हुआ रह सकता है और विकारहेतु मिलने पर उसमें विकृति (ब्रह्मस्खलन) पैदा होने की पूरी सम्भावना है। चुनांचे भूषादिहीन जिनेन्द्र का शरीर इस बात का प्रतीक है कि वहाँ कामरूप मोह नहीं रहा, इसीलिये समन्तभद्र ने 'ततस्त्वं निर्मोहः' शब्दों के द्वारा जिनेन्द्र को 'निर्मोह' कहा है। ऐसी हालत में यह स्पष्ट है कि समन्तभद्र जिनेन्द्रों को वस्त्रादिरहित बतलाते हैं और भद्रबाहु उनके एक वस्त्र के रखने का उल्लेख करते हैं, जो श्वेताम्बरीय आचारांग आदि सूत्रों के अनुकूल है। इतना ही नहीं, पिंडनियुक्ति में 'परसेय --- चीरधोवणं चेव' (गा.२३) शब्दों द्वारा वस्त्र प्रक्षालन का विधान, उसके वर्षाकाल को छोड़कर शेषकाल में धोने के दोष
और 'वासास अधोवणे दोसा' (पिं० नि० २५) शब्दों द्वारा अप्रक्षालन में दोष भी बतलाते हैं। क्या यह भी समन्तभद्र को विवक्षित है? यदि हाँ, तो उन्होंने जो यह प्रतिपादन किया है कि 'जिस साधुवर्ग में अल्प भी आरम्भ होगा, वहाँ अहिंसा का कदापि पूर्ण पालन निर्वाह नहीं हो सकता, अहिंसारूप परमब्रह्म की सिद्धि नहीं हो सकती है' (न सा तत्रारम्भोऽस्त्यणुरपि च यत्राश्रमविधी ), तब इसके क्या मायने हैं? क्या उनके उक्त कथन का कुछ भी महत्त्व नहीं है और उनके अणु, अपि शब्दों का प्रयोग क्या यों ही है? किन्तु ऐसा नहीं है, इस बात को उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति स्पष्ट बतलाती है। अन्यथा ततस्तत्सिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयं यह न कहते। इस मान्यताभेद से भी समन्तभद्र और भद्रबाहु एक नहीं हो सकते। वे वास्तव में भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं और जुदी-जुदी दो परम्पराओं में हुए हैं।
Jain Education Intemational
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org