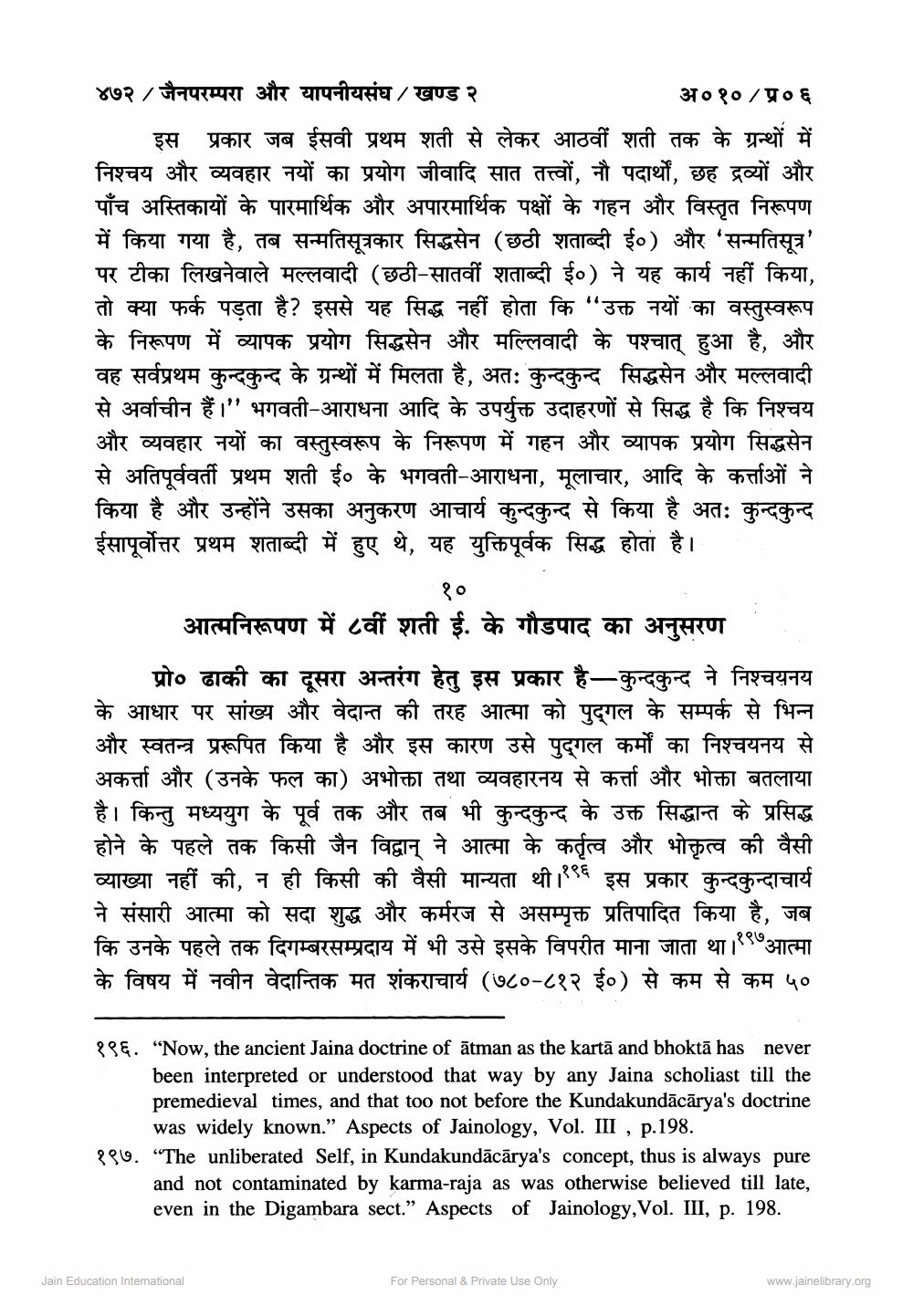________________
४७२ / जैनपरम्परा और यापनीयसंघ / खण्ड २
अ०१०/प्र०६ इस प्रकार जब ईसवी प्रथम शती से लेकर आठवीं शती तक के ग्रन्थों में निश्चय और व्यवहार नयों का प्रयोग जीवादि सात तत्त्वों, नौ पदार्थों, छह द्रव्यों और पाँच अस्तिकायों के पारमार्थिक और अपारमार्थिक पक्षों के गहन और विस्तृत निरूपण में किया गया है, तब सन्मतिसूत्रकार सिद्धसेन (छठी शताब्दी ई०) और 'सन्मतिसूत्र' पर टीका लिखनेवाले मल्लवादी (छठी-सातवीं शताब्दी ई०) ने यह कार्य नहीं किया, तो क्या फर्क पड़ता है? इससे यह सिद्ध नहीं होता कि "उक्त नयों का वस्तुस्वरूप के निरूपण में व्यापक प्रयोग सिद्धसेन और मल्लिवादी के पश्चात् हुआ है, और वह सर्वप्रथम कुन्दकुन्द के ग्रन्थों में मिलता है, अतः कुन्दकुन्द सिद्धसेन और मल्लवादी से अर्वाचीन हैं।" भगवती-आराधना आदि के उपर्युक्त उदाहरणों से सिद्ध है कि निश्चय और व्यवहार नयों का वस्तुस्वरूप के निरूपण में गहन और व्यापक प्रयोग सिद्धसेन से अतिपूर्ववर्ती प्रथम शती ई० के भगवती-आराधना, मूलाचार, आदि के कर्ताओं ने किया है और उन्होंने उसका अनुकरण आचार्य कुन्दकुन्द से किया है अतः कुन्दकुन्द ईसापूर्वोत्तर प्रथम शताब्दी में हुए थे, यह युक्तिपूर्वक सिद्ध होता है।
आत्मनिरूपण में ८वीं शती ई. के गौडपाद का अनुसरण प्रो० ढाकी का दूसरा अन्तरंग हेतु इस प्रकार है-कुन्दकुन्द ने निश्चयनय के आधार पर सांख्य और वेदान्त की तरह आत्मा को पुद्गल के सम्पर्क से भिन्न और स्वतन्त्र प्ररूपित किया है और इस कारण उसे पुद्गल कर्मों का निश्चयनय से अकर्ता और (उनके फल का) अभोक्ता तथा व्यवहारनय से कर्ता और भोक्ता बतलाया है। किन्तु मध्ययुग के पूर्व तक और तब भी कुन्दकुन्द के उक्त सिद्धान्त के प्रसिद्ध होने के पहले तक किसी जैन विद्वान् ने आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तृत्व की वैसी व्याख्या नहीं की, न ही किसी की वैसी मान्यता थी।९६ इस प्रकार कुन्दकुन्दाचार्य ने संसारी आत्मा को सदा शुद्ध और कर्मरज से असम्पृक्त प्रतिपादित किया है, जब कि उनके पहले तक दिगम्बरसम्प्रदाय में भी उसे इसके विपरीत माना जाता था। आत्मा के विषय में नवीन वेदान्तिक मत शंकराचार्य (७८०-८१२ ई०) से कम से कम ५०
१९६. "Now, the ancient Jaina doctrine of atman as the karta and bhoktā has never
been interpreted or understood that way by any Jaina scholiast till the premedieval times, and that too not before the Kundakundācārya's doctrine
was widely known." Aspects of Jainology, Vol. III , p.198. 880. "The unliberated Self, in Kundakundācārya's concept, thus is always pure
and not contaminated by karma-raja as was otherwise believed till late, even in the Digambara sect." Aspects of Jainology, Vol. III, p. 198.
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org