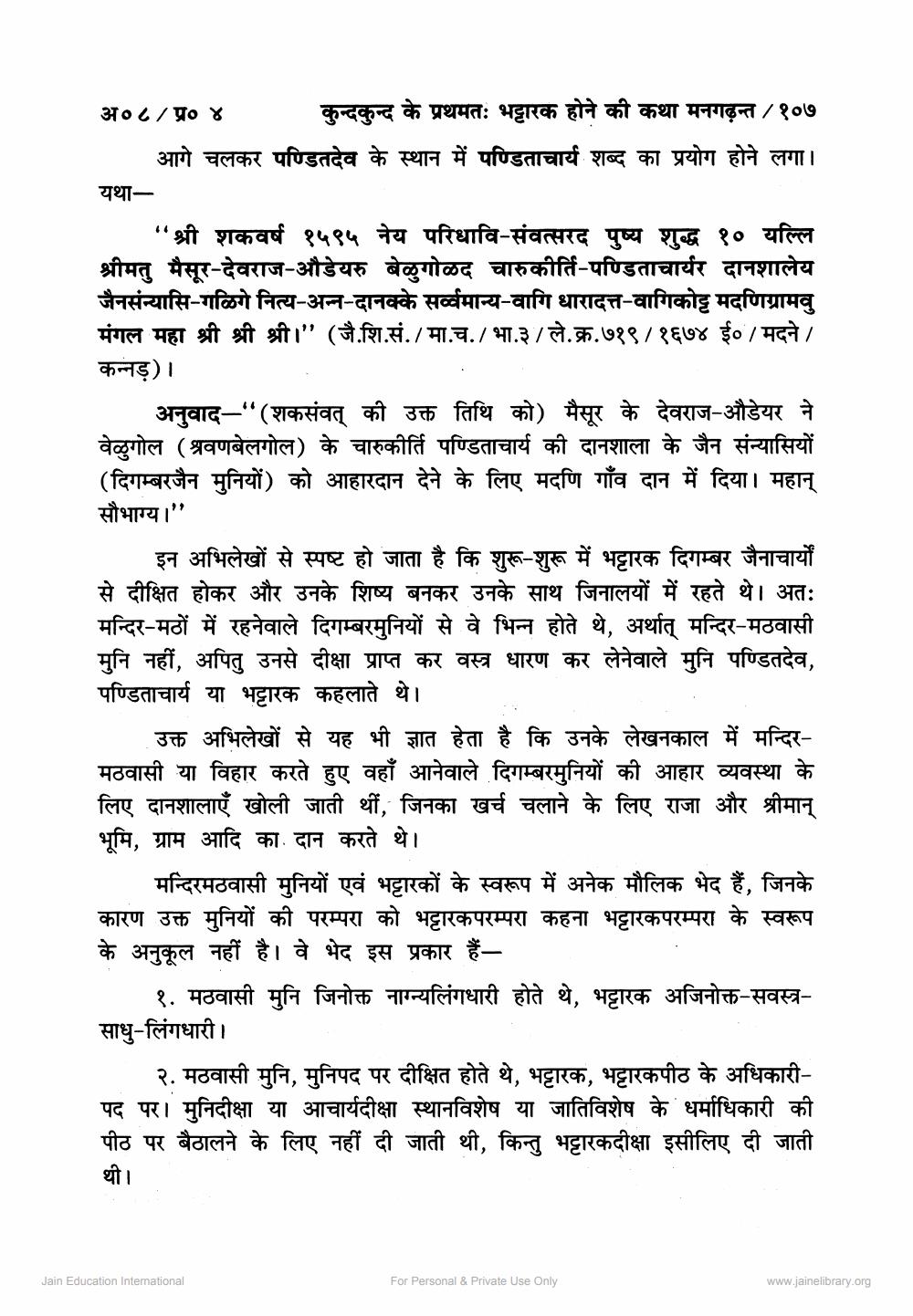________________
अ०८ / प्र० ४
कुन्दकुन्द के प्रथमतः भट्टारक होने की कथा मनगढ़न्त / १०७
आगे चलकर पण्डितदेव के स्थान में पण्डिताचार्य शब्द का प्रयोग होने लगा ।
यथा
44
'श्री शकवर्ष १५९५ नेय परिधावि-संवत्सरद पुष्य शुद्ध १० यल्लि श्रीमतु मैसूर - देवराज - औडेयरु बेळुगोळद चारुकीर्ति पण्डिताचार्यर दानशालेय जैनसंन्यासि - गळिगे नित्य- अन्न-दानक्के सर्व्वमान्य - वागि धारादत्त - वागिकोट्ट मदणिग्रामवु मंगल महा श्री श्री श्री ।" (जै.शि.सं. / मा.च./ भा.३/ले.क्र.७१९ / १६७४ ई० / मदने / कन्नड़)।
अनुवाद - " ( शकसंवत् की उक्त तिथि को ) मैसूर के देवराज - औडेयर ने वेळुगोल (श्रवणबेलगोल) के चारुकीर्ति पण्डिताचार्य की दानशाला के जैन संन्यासियों (दिगम्बरजैन मुनियों) को आहारदान देने के लिए मदणि गाँव दान में दिया । महान् सौभाग्य।”
इन अभिलेखों से स्पष्ट हो जाता है कि शुरू-शुरू में भट्टारक दिगम्बर जैनाचार्यों से दीक्षित होकर और उनके शिष्य बनकर उनके साथ जिनालयों में रहते थे । अतः मन्दिर - मठों में रहनेवाले दिगम्बरमुनियों से वे भिन्न होते थे, अर्थात् मन्दिर - मठवासी मुनि नहीं, अपितु उनसे दीक्षा प्राप्त कर वस्त्र धारण कर लेनेवाले मुनि पण्डितदेव, पण्डिताचार्य या भट्टारक कहलाते थे ।
उक्त अभिलेखों से यह भी ज्ञात हेता है कि उनके लेखनकाल में मन्दिरमठवासी या विहार करते हुए वहाँ आनेवाले दिगम्बरमुनियों की आहार व्यवस्था के लिए दानशालाएँ खोली जाती थीं, जिनका खर्च चलाने के लिए राजा और श्रीमान् भूमि, ग्राम आदि का दान करते थे ।
मन्दिरमठवासी मुनियों एवं भट्टारकों के स्वरूप में अनेक मौलिक भेद हैं, जिनके कारण उक्त मुनियों की परम्परा को भट्टारकपरम्परा कहना भट्टारकपरम्परा के स्वरूप के अनुकूल नहीं है। वे भेद इस प्रकार हैं
१. मठवासी मुनि जिनोक्त नाग्न्यलिंगधारी होते थे, भट्टारक अजिनोक्त-सवस्त्रसाधु-लिंगधारी ।
२. मठवासी मुनि, मुनिपद पर दीक्षित होते थे, भट्टारक, भट्टारकपीठ के अधिकारीपद पर । मुनिदीक्षा या आचार्यदीक्षा स्थानविशेष या जातिविशेष के धर्माधिकारी की पीठ पर बैठालने के लिए नहीं दी जाती थी, किन्तु भट्टारकदीक्षा इसीलिए दी जाती थी ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org