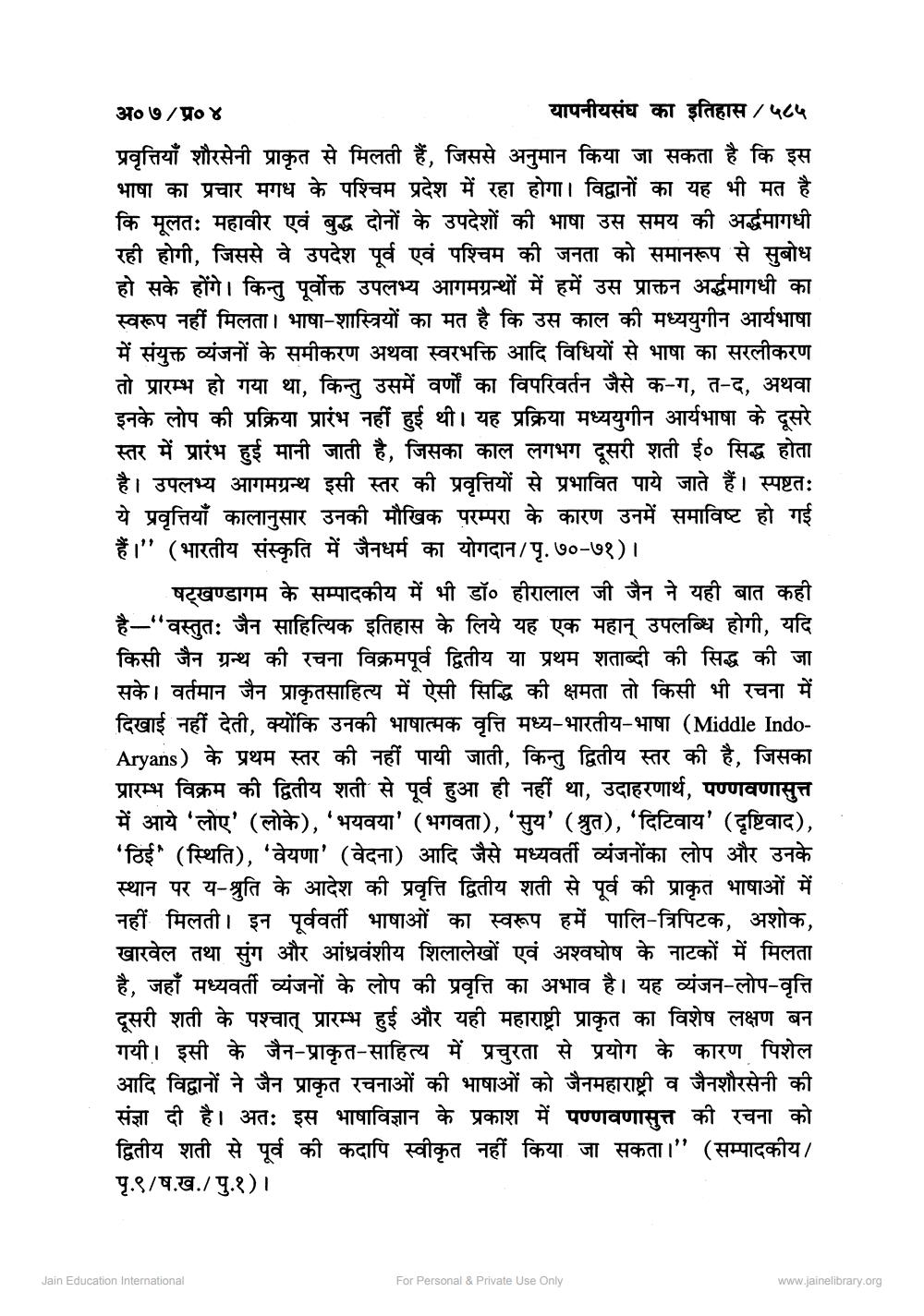________________
अ०७/प्र०४
यापनीयसंघ का इतिहास / ५८५ प्रवृत्तियाँ शौरसेनी प्राकृत से मिलती हैं, जिससे अनुमान किया जा सकता है कि इस भाषा का प्रचार मगध के पश्चिम प्रदेश में रहा होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि मूलतः महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेशों की भाषा उस समय की अर्द्धमागधी रही होगी, जिससे वे उपदेश पूर्व एवं पश्चिम की जनता को समानरूप से सुबोध हो सके होंगे। किन्तु पूर्वोक्त उपलभ्य आगमग्रन्थों में हमें उस प्राक्तन अर्द्धमागधी का स्वरूप नहीं मिलता। भाषा-शास्त्रियों का मत है कि उस काल की मध्ययुगीन आर्यभाषा में संयुक्त व्यंजनों के समीकरण अथवा स्वरभक्ति आदि विधियों से भाषा का सरलीकरण तो प्रारम्भ हो गया था, किन्तु उसमें वर्गों का विपरिवर्तन जैसे क-ग, त-द, अथवा इनके लोप की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी। यह प्रक्रिया मध्ययुगीन आर्यभाषा के दूसरे स्तर में प्रारंभ हुई मानी जाती है, जिसका काल लगभग दूसरी शती ई० सिद्ध होता है। उपलभ्य आगमग्रन्थ इसी स्तर की प्रवृत्तियों से प्रभावित पाये जाते हैं। स्पष्टतः ये प्रवृत्तियाँ कालानुसार उनकी मौखिक परम्परा के कारण उनमें समाविष्ट हो गई हैं।" (भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान / पृ. ७०-७१)।
षट्खण्डागम के सम्पादकीय में भी डॉ० हीरालाल जी जैन ने यही बात कही है-"वस्तुतः जैन साहित्यिक इतिहास के लिये यह एक महान् उपलब्धि होगी, यदि किसी जैन ग्रन्थ की रचना विक्रमपूर्व द्वितीय या प्रथम शताब्दी की सिद्ध की जा सके। वर्तमान जैन प्राकृतसाहित्य में ऐसी सिद्धि की क्षमता तो किसी भी रचना में दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनकी भाषात्मक वृत्ति मध्य-भारतीय-भाषा (Middle IndoAryans) के प्रथम स्तर की नहीं पायी जाती, किन्तु द्वितीय स्तर की है, जिसका प्रारम्भ विक्रम की द्वितीय शती से पूर्व हुआ ही नहीं था, उदाहरणार्थ, पण्णवणासुत्त में आये 'लोए' (लोके), 'भयवया' (भगवता), 'सुय' (श्रुत), 'दिटिवाय' (दृष्टिवाद), "ठिई (स्थिति), 'वेयणा' (वेदना) आदि जैसे मध्यवर्ती व्यंजनोंका लोप और उनके स्थान पर य-श्रुति के आदेश की प्रवृत्ति द्वितीय शती से पूर्व की प्राकृत भाषाओं में नहीं मिलती। इन पूर्ववर्ती भाषाओं का स्वरूप हमें पालि-त्रिपिटक, अशोक, खारवेल तथा सुंग और आंध्रवंशीय शिलालेखों एवं अश्वघोष के नाटकों में मिलता है, जहाँ मध्यवर्ती व्यंजनों के लोप की प्रवृत्ति का अभाव है। यह व्यंजन-लोप-वृत्ति दूसरी शती के पश्चात् प्रारम्भ हुई और यही महाराष्ट्री प्राकृत का विशेष लक्षण बन गयी। इसी के जैन-प्राकृत-साहित्य में प्रचुरता से प्रयोग के कारण पिशेल आदि विद्वानों ने जैन प्राकृत रचनाओं की भाषाओं को जैनमहाराष्ट्री व जैनशौरसेनी की संज्ञा दी है। अतः इस भाषाविज्ञान के प्रकाश में पण्णवणासुत्त की रचना को द्वितीय शती से पूर्व की कदापि स्वीकृत नहीं किया जा सकता।" (सम्पादकीय। पृ.९/ष.ख./ पु.१)।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org