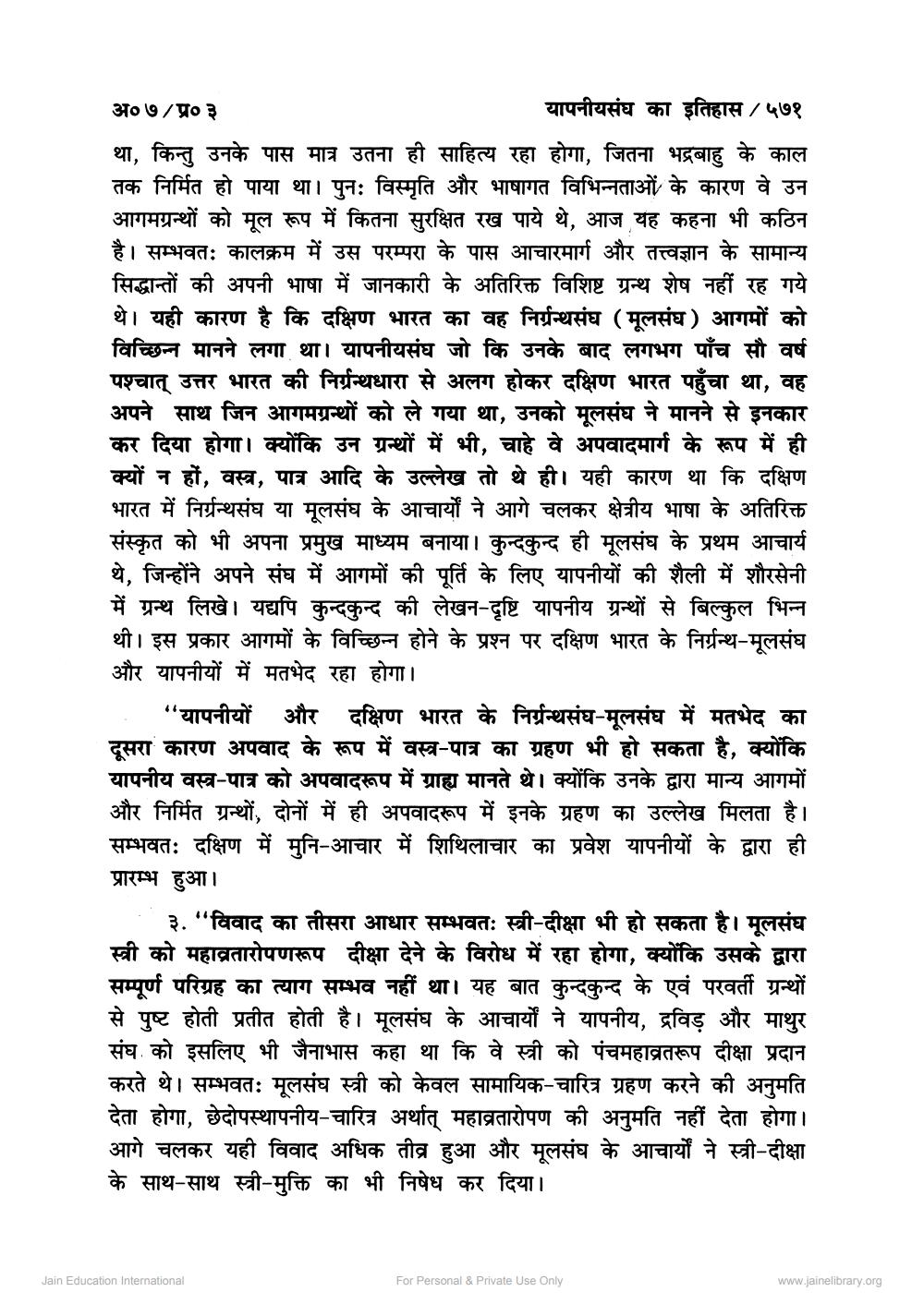________________
अ०७/प्र०३
यापनीयसंघ का इतिहास / ५७१ था, किन्तु उनके पास मात्र उतना ही साहित्य रहा होगा, जितना भद्रबाहु के काल तक निर्मित हो पाया था। पुनः विस्मृति और भाषागत विभिन्नताओं के कारण वे उन आगमग्रन्थों को मूल रूप में कितना सुरक्षित रख पाये थे, आज यह कहना भी कठिन है। सम्भवतः कालक्रम में उस परम्परा के पास आचारमार्ग और तत्त्वज्ञान के सामान्य सिद्धान्तों की अपनी भाषा में जानकारी के अतिरिक्त विशिष्ट ग्रन्थ शेष नहीं रह गये थे। यही कारण है कि दक्षिण भारत का वह निर्ग्रन्थसंघ (मूलसंघ) आगमों को विच्छिन्न मानने लगा था। यापनीयसंघ जो कि उनके बाद लगभग पाँच सौ वर्ष पश्चात् उत्तर भारत की निर्ग्रन्थधारा से अलग होकर दक्षिण भारत पहुँचा था, वह अपने साथ जिन आगमग्रन्थों को ले गया था, उनको मूलसंघ ने मानने से इनकार कर दिया होगा। क्योंकि उन ग्रन्थों में भी, चाहे वे अपवादमार्ग के रूप में ही क्यों न हों, वस्त्र, पात्र आदि के उल्लेख तो थे ही। यही कारण था कि दक्षिण भारत में निर्ग्रन्थसंघ या मूलसंघ के आचार्यों ने आगे चलकर क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त संस्कृत को भी अपना प्रमुख माध्यम बनाया। कुन्दकुन्द ही मूलसंघ के प्रथम आचार्य थे, जिन्होंने अपने संघ में आगमों की पूर्ति के लिए यापनीयों की शैली में शौरसेनी में ग्रन्थ लिखे। यद्यपि कुन्दकुन्द की लेखन-दृष्टि यापनीय ग्रन्थों से बिल्कुल भिन्न थी। इस प्रकार आगमों के विच्छिन्न होने के प्रश्न पर दक्षिण भारत के निर्ग्रन्थ-मूलसंघ और यापनीयों में मतभेद रहा होगा।
"यापनीयों और दक्षिण भारत के निर्ग्रन्थसंघ-मूलसंघ में मतभेद का दूसरा कारण अपवाद के रूप में वस्त्र-पात्र का ग्रहण भी हो सकता है, क्योंकि यापनीय वस्त्र-पात्र को अपवादरूप में ग्राह्य मानते थे। क्योंकि उनके द्वारा मान्य आगमों
और निर्मित ग्रन्थों, दोनों में ही अपवादरूप में इनके ग्रहण का उल्लेख मिलता है। सम्भवतः दक्षिण में मुनि-आचार में शिथिलाचार का प्रवेश यापनीयों के द्वारा ही प्रारम्भ हुआ।
- ३. "विवाद का तीसरा आधार सम्भवतः स्त्री-दीक्षा भी हो सकता है। मूलसंघ स्त्री को महाव्रतारोपणरूप दीक्षा देने के विरोध में रहा होगा, क्योंकि उसके द्वारा सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग सम्भव नहीं था। यह बात कुन्दकुन्द के एवं परवर्ती ग्रन्थों से पुष्ट होती प्रतीत होती है। मूलसंघ के आचार्यों ने यापनीय, द्रविड़ और माथुर संघ को इसलिए भी जैनाभास कहा था कि वे स्त्री को पंचमहाव्रतरूप दीक्षा प्रदान करते थे। सम्भवतः मूलसंघ स्त्री को केवल सामायिक-चारित्र ग्रहण करने की अनुमति देता होगा, छेदोपस्थापनीय-चारित्र अर्थात् महाव्रतारोपण की अनुमति नहीं देता होगा। आगे चलकर यही विवाद अधिक तीव्र हुआ और मूलसंघ के आचार्यों ने स्त्री-दीक्षा के साथ-साथ स्त्री-मुक्ति का भी निषेध कर दिया।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org