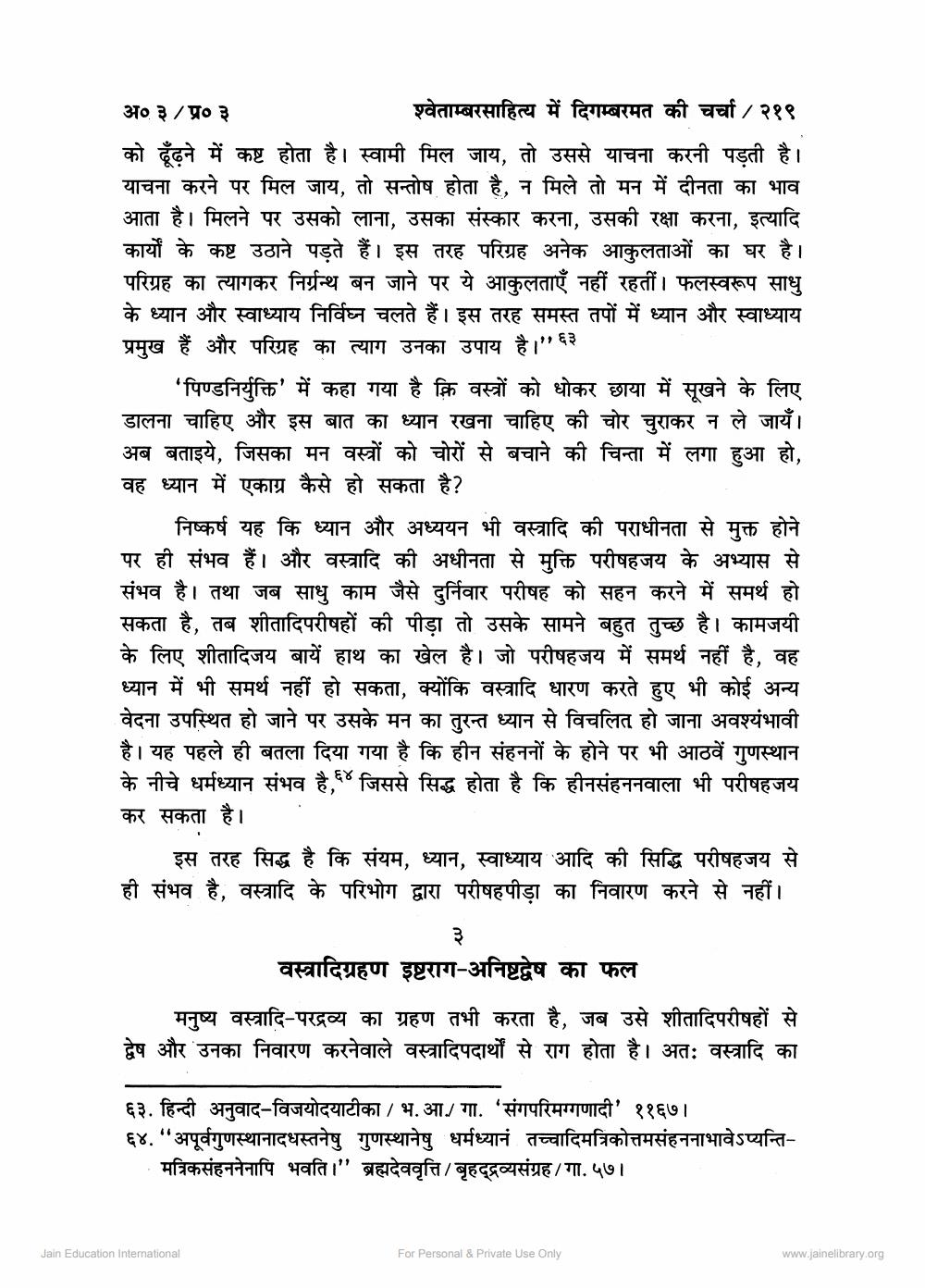________________
अ० ३ / प्र० ३
श्वेताम्बर साहित्य में दिगम्बरमत की चर्चा / २१९
को ढूँढ़ने में कष्ट होता है । स्वामी मिल जाय, तो उससे याचना करनी पड़ती है । याचना करने पर मिल जाय, तो सन्तोष होता है, न मिले तो मन में दीनता का भाव आता है। मिलने पर उसको लाना, उसका संस्कार करना, उसकी रक्षा करना, इत्यादि कार्यों के कष्ट उठाने पड़ते हैं । इस तरह परिग्रह अनेक आकुलताओं का घर है । परिग्रह का त्यागकर निर्ग्रन्थ बन जाने पर ये आकुलताएँ नहीं रहतीं। फलस्वरूप साधु के ध्यान और स्वाध्याय निर्विघ्न चलते हैं। इस तरह समस्त तपों में ध्यान और स्वाध्याय प्रमुख हैं और परिग्रह का त्याग उनका उपाय है।" ६३
'पिण्डनिर्युक्ति' में कहा गया है क़ि वस्त्रों को धोकर छाया में सूखने के लिए डालना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए की चोर चुराकर न ले जायँ । अब बताइये, जिसका मन वस्त्रों को चोरों से बचाने की चिन्ता में लगा हुआ हो, वह ध्यान में एकाग्र कैसे हो सकता है?
निष्कर्ष यह कि ध्यान और अध्ययन भी वस्त्रादि की पराधीनता से मुक्त होने पर ही संभव हैं। और वस्त्रादि की अधीनता से मुक्ति परीषहजय के अभ्यास से संभव है। तथा जब साधु काम जैसे दुर्निवार परीषह को सहन करने में समर्थ हो सकता है, तब शीतादिपरीषहों की पीड़ा तो उसके सामने बहुत तुच्छ है । कामजी के लिए शीतादिजय बायें हाथ का खेल है। जो परीषहजय में समर्थ नहीं है, वह ध्यान में भी समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वस्त्रादि धारण करते हुए भी कोई अन्य वेदना उपस्थित हो जाने पर उसके मन का तुरन्त ध्यान से विचलित हो जाना अवश्यंभावी है। यह पहले ही बतला दिया गया है कि हीन संहननों के होने पर भी आठवें गुणस्थान के नीचे धर्मध्यान संभव है, जिससे सिद्ध होता है कि हीनसंहननवाला भी परीषहजय कर सकता है।
इस तरह सिद्ध है कि संयम, ध्यान, स्वाध्याय आदि की सिद्धि परीषहजय से ही संभव है, वस्त्रादि के परिभोग द्वारा परीषहपीड़ा का निवारण करने से नहीं ।
३
वस्त्रादिग्रहण इष्टराग- अनिष्टद्वेष का फल
मनुष्य वस्त्रादि-परद्रव्य का ग्रहण तभी करता है, जब उसे शीतादिपरीषहों से द्वेष और उनका निवारण करनेवाले वस्त्रादिपदार्थों से राग होता है । अतः वस्त्रादि का
६३. हिन्दी अनुवाद - विजयोदयाटीका / भ.आ./ गा. 'संगपरिमग्गणादी' ११६७ । ६४. “ अपूर्वगुणस्थानादधस्तनेषु गुणस्थानेषु धर्मध्यानं तच्चादिमत्रिकोत्तमसंहननाभावेऽप्यन्तिमत्रिकसंहननेनापि भवति ।" ब्रह्मदेववृत्ति / बृहद्द्रव्यसंग्रह / गा. ५७ ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org