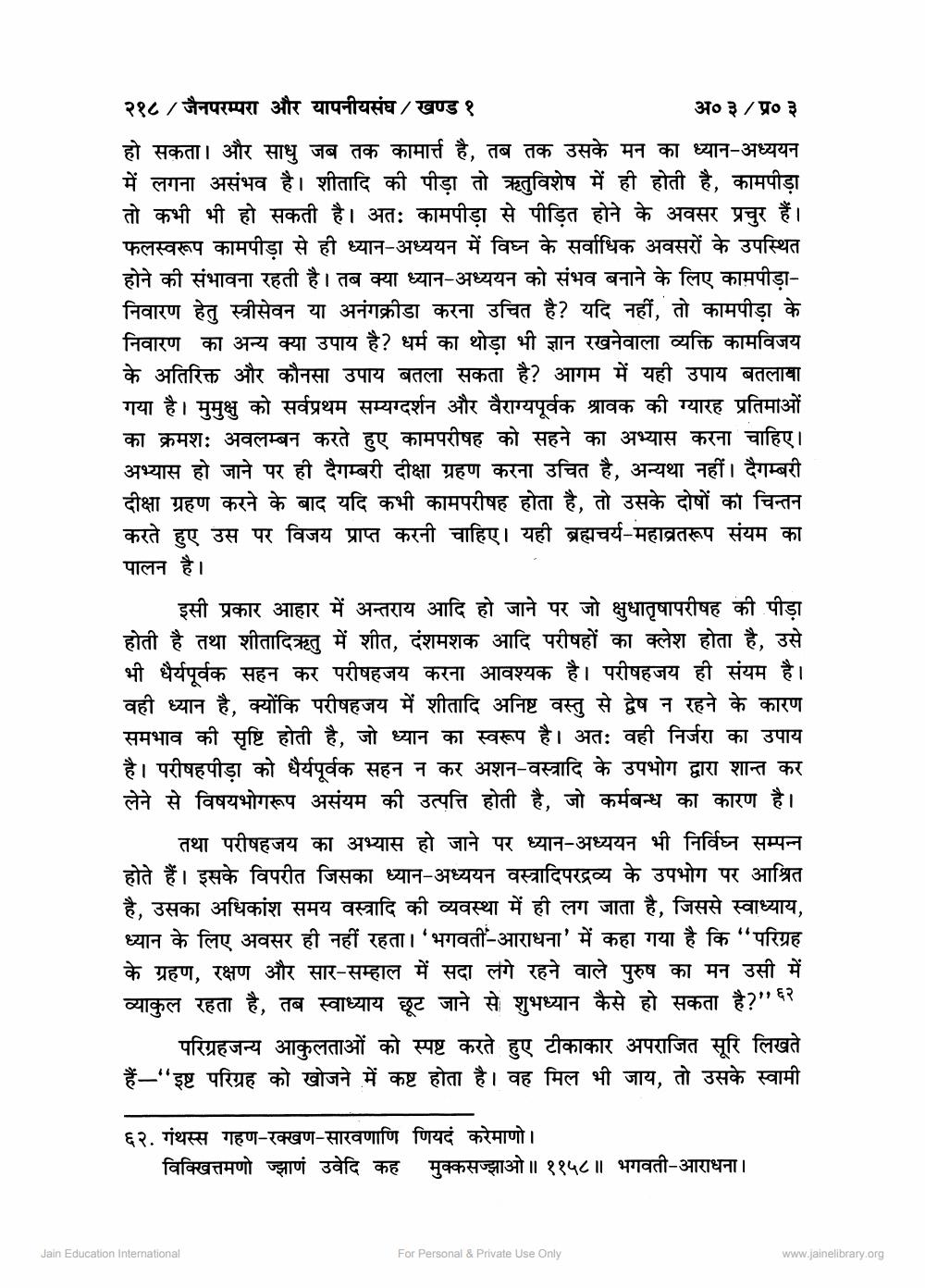________________
२१८ / जैनपरम्परा और यापनीयसंघ / खण्ड १
अ०३/प्र०३ हो सकता। और साधु जब तक कामात है, तब तक उसके मन का ध्यान-अध्ययन में लगना असंभव है। शीतादि की पीड़ा तो ऋतुविशेष में ही होती है, कामपीड़ा तो कभी भी हो सकती है। अतः कामपीड़ा से पीड़ित होने के अवसर प्रचुर हैं। फलस्वरूप कामपीड़ा से ही ध्यान-अध्ययन में विघ्न के सर्वाधिक अवसरों के उपस्थित होने की संभावना रहती है। तब क्या ध्यान-अध्ययन को संभव बनाने के लिए कामपीड़ानिवारण हेतु स्त्रीसेवन या अनंगक्रीडा करना उचित है? यदि नहीं, तो कामपीड़ा के निवारण का अन्य क्या उपाय है? धर्म का थोड़ा भी ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति कामविजय के अतिरिक्त और कौनसा उपाय बतला सकता है? आगम में यही उपाय बतलाया गया है। मुमुक्षु को सर्वप्रथम सम्यग्दर्शन और वैराग्यपूर्वक श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं का क्रमशः अवलम्बन करते हुए कामपरीषह को सहने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास हो जाने पर ही दैगम्बरी दीक्षा ग्रहण करना उचित है, अन्यथा नहीं। दैगम्बरी दीक्षा ग्रहण करने के बाद यदि कभी कामपरीषह होता है, तो उसके दोषों का चिन्तन करते हुए उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यही ब्रह्मचर्य-महाव्रतरूप संयम का पालन है।
इसी प्रकार आहार में अन्तराय आदि हो जाने पर जो क्षुधातृषापरीषह की पीड़ा होती है तथा शीतादिऋतु में शीत, दंशमशक आदि परीषहों का क्लेश होता है, उसे भी धैर्यपूर्वक सहन कर परीषहजय करना आवश्यक है। परीषहजय ही संयम है। वही ध्यान है, क्योंकि परीषहजय में शीतादि अनिष्ट वस्तु से द्वेष न रहने के कारण समभाव की सृष्टि होती है, जो ध्यान का स्वरूप है। अतः वही निर्जरा का उपाय है। परीषहपीड़ा को धैर्यपूर्वक सहन न कर अशन-वस्त्रादि के उपभोग द्वारा शान्त कर लेने से विषयभोगरूप असंयम की उत्पत्ति होती है, जो कर्मबन्ध का कारण है।
तथा परीषहजय का अभ्यास हो जाने पर ध्यान-अध्ययन भी निर्विघ्न सम्पन्न होते हैं। इसके विपरीत जिसका ध्यान-अध्ययन वस्त्रादिपरद्रव्य के उपभोग पर आश्रित है, उसका अधिकांश समय वस्त्रादि की व्यवस्था में ही लग जाता है, जिससे स्वाध्याय, ध्यान के लिए अवसर ही नहीं रहता। भगवती-आराधना' में कहा गया है कि "परिग्रह के ग्रहण, रक्षण और सार-सम्हाल में सदा लगे रहने वाले पुरुष का मन उसी में व्याकुल रहता है, तब स्वाध्याय छूट जाने से शुभध्यान कैसे हो सकता है?" ६२
परिग्रहजन्य आकुलताओं को स्पष्ट करते हुए टीकाकार अपराजित सूरि लिखते हैं-"इष्ट परिग्रह को खोजने में कष्ट होता है। वह मिल भी जाय, तो उसके स्वामी
६२. गंथस्स गहण-रक्खण-सारवणाणि णियदं करेमाणो।
विक्खित्तमणो ज्झाणं उवेदि कह मुक्कसज्झाओ॥ ११५८॥ भगवती-आराधना।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org