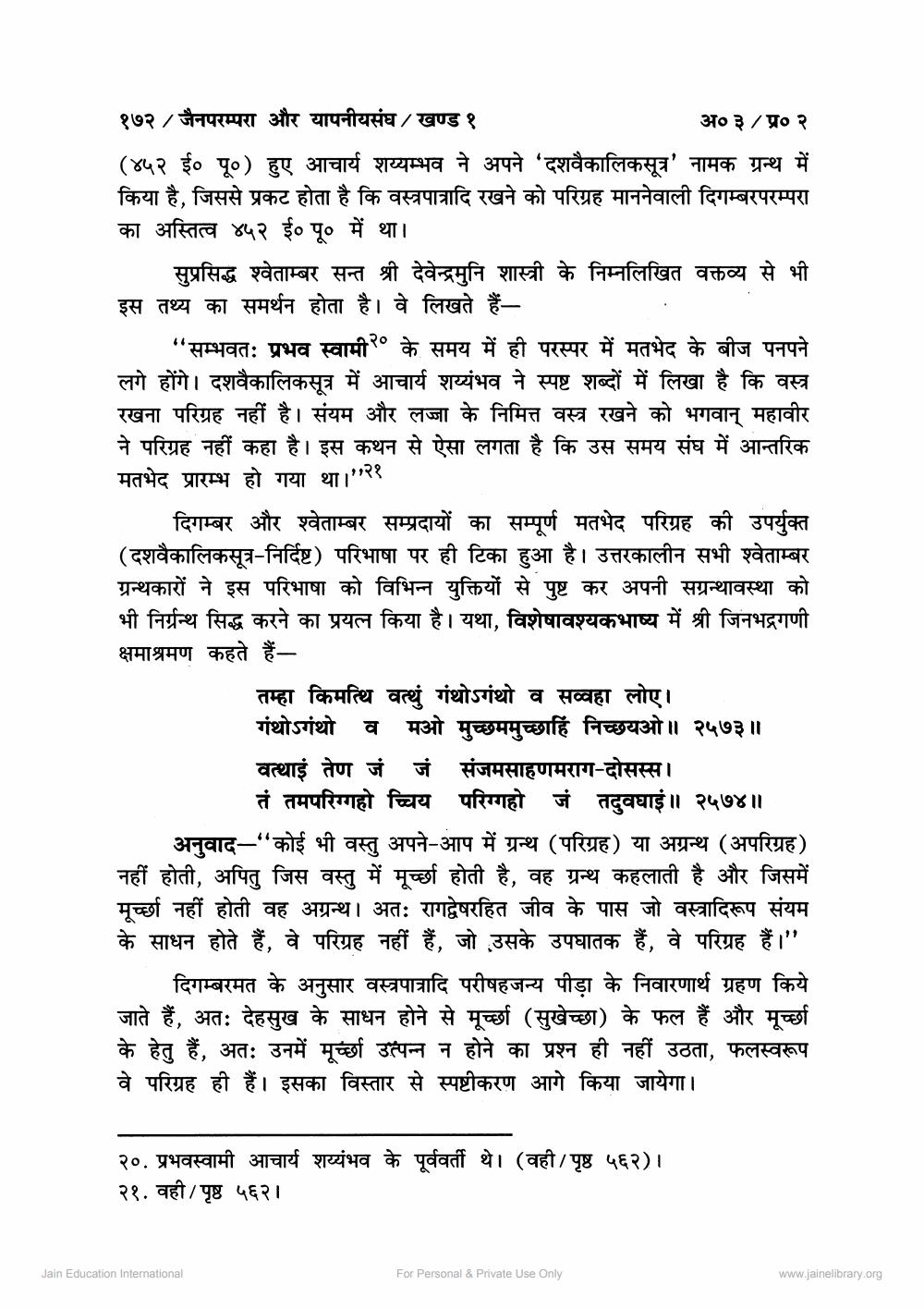________________
१७२ / जैनपरम्परा और यापनीयसंघ / खण्ड १
अ०३ / प्र० २
(४५२ ई० पू०) हुए आचार्य शय्यम्भव ने अपने 'दशवैकालिकसूत्र' नामक ग्रन्थ में किया है, जिससे प्रकट होता है कि वस्त्रपात्रादि रखने को परिग्रह माननेवाली दिगम्बरपरम्परा का अस्तित्व ४५२ ई० पू० में था ।
सुप्रसिद्ध श्वेताम्बर सन्त श्री देवेन्द्रमुनि शास्त्री के निम्नलिखित वक्तव्य से भी इस तथ्य का समर्थन होता है। वे लिखते हैं
" सम्भवतः प्रभव स्वामी २० के समय में ही परस्पर में मतभेद के बीज पनपने लगे होंगे। दशवैकालिकसूत्र में आचार्य शय्यंभव ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वस्त्र रखना परिग्रह नहीं है । संयम और लज्जा के निमित्त वस्त्र रखने को भगवान् महावीर ने परिग्रह नहीं कहा है । इस कथन से ऐसा लगता है कि उस समय संघ में आन्तरिक मतभेद प्रारम्भ हो गया था । " २१
दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों का सम्पूर्ण मतभेद परिग्रह की उपर्युक्त (दशवैकालिकसूत्र-निर्दिष्ट) परिभाषा पर ही टिका हुआ है। उत्तरकालीन सभी श्वेताम्बर ग्रन्थकारों ने इस परिभाषा को विभिन्न युक्तियों से पुष्ट कर अपनी सग्रन्थावस्था को भी निर्ग्रन्थ सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । यथा, विशेषावश्यकभाष्य में श्री जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण कहते हैं
तम्हा किमत्थि वत्थं गंथोऽगंथो व सव्वहा लोए । गंथोऽगंथो व मओ मुच्छममुच्छाहिं निच्छयओ ॥ २५७३ ॥
वत्थाइं तेण जं जं संजमसाहणमराग-दोसस्स । तं तमपरिग्गहो च्चिय परिग्गहो जं तदुवघाई ॥ २५७४ ॥
अनुवाद - "कोई भी वस्तु अपने-आप में ग्रन्थ (परिग्रह ) या अग्रन्थ (अपरिग्रह ) नहीं होती, अपितु जिस वस्तु में मूर्च्छा होती है, वह ग्रन्थ कहलाती है और जिसमें मूर्च्छा नहीं होती वह अग्रन्थ । अतः रागद्वेषरहित जीव के पास जो वस्त्रादिरूप संयम के साधन होते हैं, वे परिग्रह नहीं हैं, जो उसके उपघातक हैं, वे परिग्रह हैं । "
दिगम्बरमत के अनुसार वस्त्रपात्रादि परीषहजन्य पीड़ा के निवारणार्थ ग्रहण किये जाते हैं, अतः देहसुख के साधन होने से मूर्च्छा (सुखेच्छा) के फल हैं और मूर्च्छा के हेतु हैं, अतः उनमें मूर्च्छा उत्पन्न न होने का प्रश्न ही नहीं उठता, फलस्वरूप वे परिग्रह ही हैं। इसका विस्तार से स्पष्टीकरण आगे किया जायेगा ।
Jain Education International
२०.
प्रभवस्वामी आचार्य शय्यंभव के पूर्ववर्ती थे । ( वही / पृष्ठ ५६२) । २९. वही / पृष्ठ ५६२ ।
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org