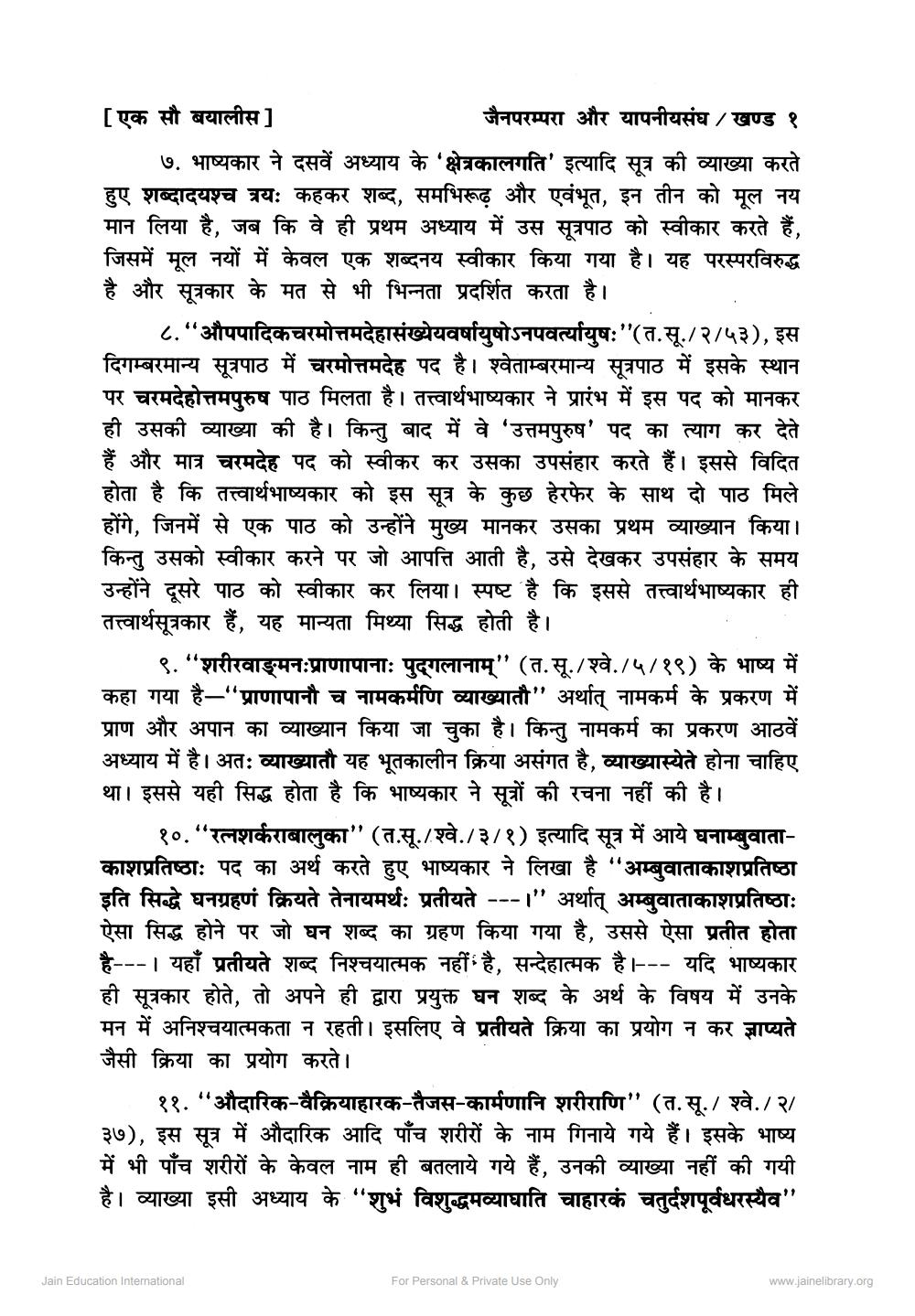________________
[एक सौ बयालीस]
जैनपरम्परा और यापनीयसंघ / खण्ड १ ७. भाष्यकार ने दसवें अध्याय के 'क्षेत्रकालगति' इत्यादि सूत्र की व्याख्या करते हुए शब्दादयश्च त्रयः कहकर शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत, इन तीन को मूल नय मान लिया है, जब कि वे ही प्रथम अध्याय में उस सूत्रपाठ को स्वीकार करते हैं, जिसमें मूल नयों में केवल एक शब्दनय स्वीकार किया गया है। यह परस्परविरुद्ध है और सूत्रकार के मत से भी भिन्नता प्रदर्शित करता है।
८. "औपपादिकचरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायुषोऽनपवायुषः"(त.सू./२/५३), इस दिगम्बरमान्य सूत्रपाठ में चरमोत्तमदेह पद है। श्वेताम्बरमान्य सूत्रपाठ में इसके स्थान पर चरमदेहोत्तमपुरुष पाठ मिलता है। तत्त्वार्थभाष्यकार ने प्रारंभ में इस पद को मानकर ही उसकी व्याख्या की है। किन्तु बाद में वे 'उत्तमपुरुष' पद का त्याग कर देते हैं और मात्र चरमदेह पद को स्वीकर कर उसका उपसंहार करते हैं। इससे विदित होता है कि तत्त्वार्थभाष्यकार को इस सूत्र के कुछ हेरफेर के साथ दो पाठ मिले होंगे, जिनमें से एक पाठ को उन्होंने मुख्य मानकर उसका प्रथम व्याख्यान किया। किन्तु उसको स्वीकार करने पर जो आपत्ति आती है, उसे देखकर उपसंहार के समय उन्होंने दूसरे पाठ को स्वीकार कर लिया। स्पष्ट है कि इससे तत्त्वार्थभाष्यकार ही तत्त्वार्थसूत्रकार हैं, यह मान्यता मिथ्या सिद्ध होती है।
९. "शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम्" (त. सू./श्वे./५/१९) के भाष्य में कहा गया है-"प्राणापानौ च नामकर्मणि व्याख्यातौ" अर्थात् नामकर्म के प्रकरण में प्राण और अपान का व्याख्यान किया जा चुका है। किन्तु नामकर्म का प्रकरण आठवें अध्याय में है। अतः व्याख्यातौ यह भूतकालीन क्रिया असंगत है, व्याख्यास्येते होना चाहिए था। इससे यही सिद्ध होता है कि भाष्यकार ने सूत्रों की रचना नहीं की है।
१०. "रत्नशर्कराबालुका" (त.सू./श्वे./३/१) इत्यादि सूत्र में आये घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः पद का अर्थ करते हुए भाष्यकार ने लिखा है "अम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा इति सिद्धे घनग्रहणं क्रियते तेनायमर्थः प्रतीयते ---।" अर्थात् अम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः ऐसा सिद्ध होने पर जो घन शब्द का ग्रहण किया गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है--- । यहाँ प्रतीयते शब्द निश्चयात्मक नहीं है, सन्देहात्मक है।--- यदि भाष्यकार ही सूत्रकार होते, तो अपने ही द्वारा प्रयुक्त घन शब्द के अर्थ के विषय में उनके मन में अनिश्चयात्मकता न रहती। इसलिए वे प्रतीयते क्रिया का प्रयोग न कर ज्ञाप्यते जैसी क्रिया का प्रयोग करते।
११. "औदारिक-वैक्रियाहारक-तैजस-कार्मणानि शरीराणि" (त. सू./ श्वे./२/ ३७), इस सूत्र में औदारिक आदि पाँच शरीरों के नाम गिनाये गये हैं। इसके भाष्य में भी पाँच शरीरों के केवल नाम ही बतलाये गये हैं, उनकी व्याख्या नहीं की गयी है। व्याख्या इसी अध्याय के "शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं चतुर्दशपूर्वधरस्यैव"
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org