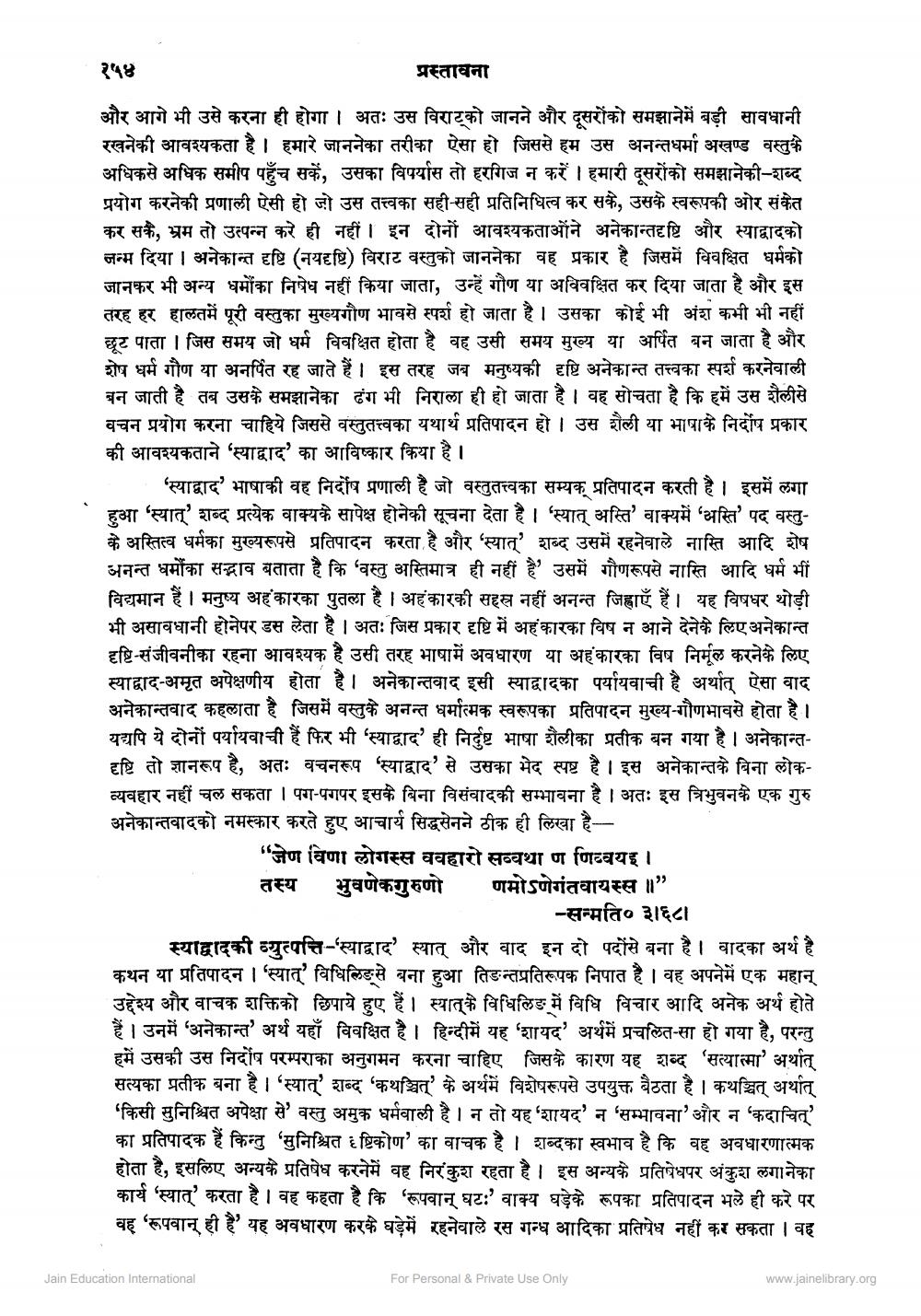________________
२५४
प्रस्तावना
और आगे भी उसे करना ही होगा। अतः उस विराटको जानने और दूसरोंको समझाने में बड़ी सावधानी रखनेकी आवश्यकता है। हमारे जाननेका तरीका ऐसा हो जिससे हम उस अनन्तधर्मा अखण्ड वस्तुके अधिकसे अधिक समीप पहुँच सकें, उसका विपर्यास तो हरगिज न करें । हमारी दूसरोंको समझानेकी-शब्द प्रयोग करनेकी प्रणाली ऐसी हो जो उस तत्त्वका सही-सही प्रतिनिधित्व कर सके, उसके स्वरूपकी ओर संकेत कर सके, भ्रम तो उत्पन्न करे ही नहीं। इन दोनों आवश्यकताओंने अनेकान्तदृष्टि और स्याद्वादको जन्म दिया । अनेकान्त दृष्टि (नयष्टि) विराट वस्तुको जाननेका वह प्रकार है जिसमें विवक्षित धर्मको जानकर भी अन्य धर्मोका निषेध नहीं किया जाता, उन्हें गौण या अविवक्षित कर दिया जाता है और इस तरह हर हालतमें पूरी वस्तुका मुख्यगौण भावसे स्पर्श हो जाता है। उसका कोई भी अंश कभी भी नहीं छूट पाता । जिस समय जो धर्म विवक्षित होता है वह उसी समय मुख्य या अर्पित बन जाता है और शेष धर्म गौण या अनर्पित रह जाते हैं। इस तरह जब मनुष्यकी दृष्टि अनेकान्त तत्त्वका स्पर्श करनेवाली बन जाती है तब उसके समझानेका ढंग भी निराला ही हो जाता है। वह सोचता है कि हमें उस शैलीसे वचन प्रयोग करना चाहिये जिससे वस्तुतत्त्वका यथार्थ प्रतिपादन हो। उस शैली या भाषाके निर्दोष प्रकार की आवश्यकताने 'स्याद्वाद' का आविष्कार किया है।
- 'स्याद्वाद' भाषाकी वह निर्दोष प्रणाली है जो वस्तुतत्त्वका सम्यक् प्रतिपादन करती है। इसमें लगा हुआ 'स्यात्' शब्द प्रत्येक वाक्यके सापेक्ष होनेकी सूचना देता है । 'स्यात् अस्ति' वाक्यमें 'अस्ति' पद वस्तुके अस्तित्व धर्मका मुख्यरूपसे प्रतिपादन करता है और 'स्यात्' शब्द उसमें रहनेवाले नास्ति आदि शेष अनन्त धर्मोंका सद्भाव बताता है कि 'वस्तु अस्तिमात्र ही नहीं है उसमें गौणरूपसे नास्ति आदि धर्म भी विद्यमान हैं । मनुष्य अहंकारका पुतला है । अहंकारकी सहस्र नहीं अनन्त जिह्वाएँ हैं। यह विषधर थोड़ी भी असावधानी होनेपर डस लेता है । अतः जिस प्रकार दृष्टि में अहंकारका विष न आने देनेके लिए अनेकान्त दृष्टि-संजीवनीका रहना आवश्यक है उसी तरह भाषामें अवधारण या अहंकारका विष निर्मूल करनेके लिए स्याद्वाद-अमृत अपेक्षणीय होता है। अनेकान्तवाद इसी स्याद्वादका पर्यायवाची है अर्थात् ऐसा वाद अनेकान्तवाद कहलाता है जिसमें वस्तुके अनन्त धर्मात्मक स्वरूपका प्रतिपादन मुख्य-गौणभावसे होता है। यद्यपि ये दोनों पर्यायवाची हैं फिर भी 'स्याद्वाद' ही निर्दष्ट भाषा शैलीका प्रतीक बन गया है। अनेकान्तदृष्टि तो ज्ञानरूप है, अतः वचनरूप 'स्याद्वाद' से उसका भेद स्पष्ट है । इस अनेकान्तके बिना लोकव्यवहार नहीं चल सकता । पग-पगपर इसके बिना विसंवादकी सम्भावना है । अतः इस त्रिभुवनके एक गुरु अनेकान्तवादको नमस्कार करते हुए आचार्य सिद्धसेनने ठीक ही लिखा है
"जेण विणा लोगस्स ववहारो सव्वथा ण णिव्वयइ । तस्य भुवणेकगुरुणो णमोऽणेगंतवायरस ॥”
-सन्मति०३१६८ स्याद्वादकी व्युत्पत्ति-'स्याद्वाद' स्यात् और वाद इन दो पदोंसे बना है। वादका अर्थ है कथन या प्रतिपादन । 'स्यात् विधिलिङ्से बना हुआ तिङन्तप्रतिरूपक निपात है । वह अपनेमें एक महान् उद्देश्य और वाचक शक्तिको छिपाये हुए हैं। स्यात्के विधिलिङ में विधि विचार आदि अनेक अर्थ होते हैं। उनमें 'अनेकान्त' अर्थ यहाँ विवक्षित है। हिन्दीमें यह 'शायद' अर्थमें प्रचलित-सा हो गया है, परन्तु हमें उसकी उस निर्दोष परम्पराका अनुगमन करना चाहिए जिसके कारण यह शब्द 'सत्यात्मा' अर्थात् सत्यका प्रतीक बना है । 'स्यात्' शब्द 'कथञ्चित्' के अर्थमें विशेषरूपसे उपयुक्त बैठता है । कथञ्चित् अर्थात् 'किसी सुनिश्चित अपेक्षा से वस्तु अमुक धर्मवाली है। न तो यह 'शायद' न 'सम्भावना' और न 'कदाचित्' का प्रतिपादक हैं किन्तु 'सुनिश्चित दृष्टिकोण' का वाचक है। शब्दका स्वभाव है कि वह अवधारणात्मक होता है, इसलिए अन्यके प्रतिषेध करनेमें वह निरंकुश रहता है। इस अन्यके प्रतिषेधपर अंकुश लगानेका कार्य 'स्यात् करता है। वह कहता है कि 'रूपवान् घटः' वाक्य घड़ेके रूपका प्रतिपादन भले ही करे पर वह 'रूपवान् ही है' यह अवधारण करके घड़ेमें रहनेवाले रस गन्ध आदिका प्रतिषेध नहीं कर सकता | वह
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org