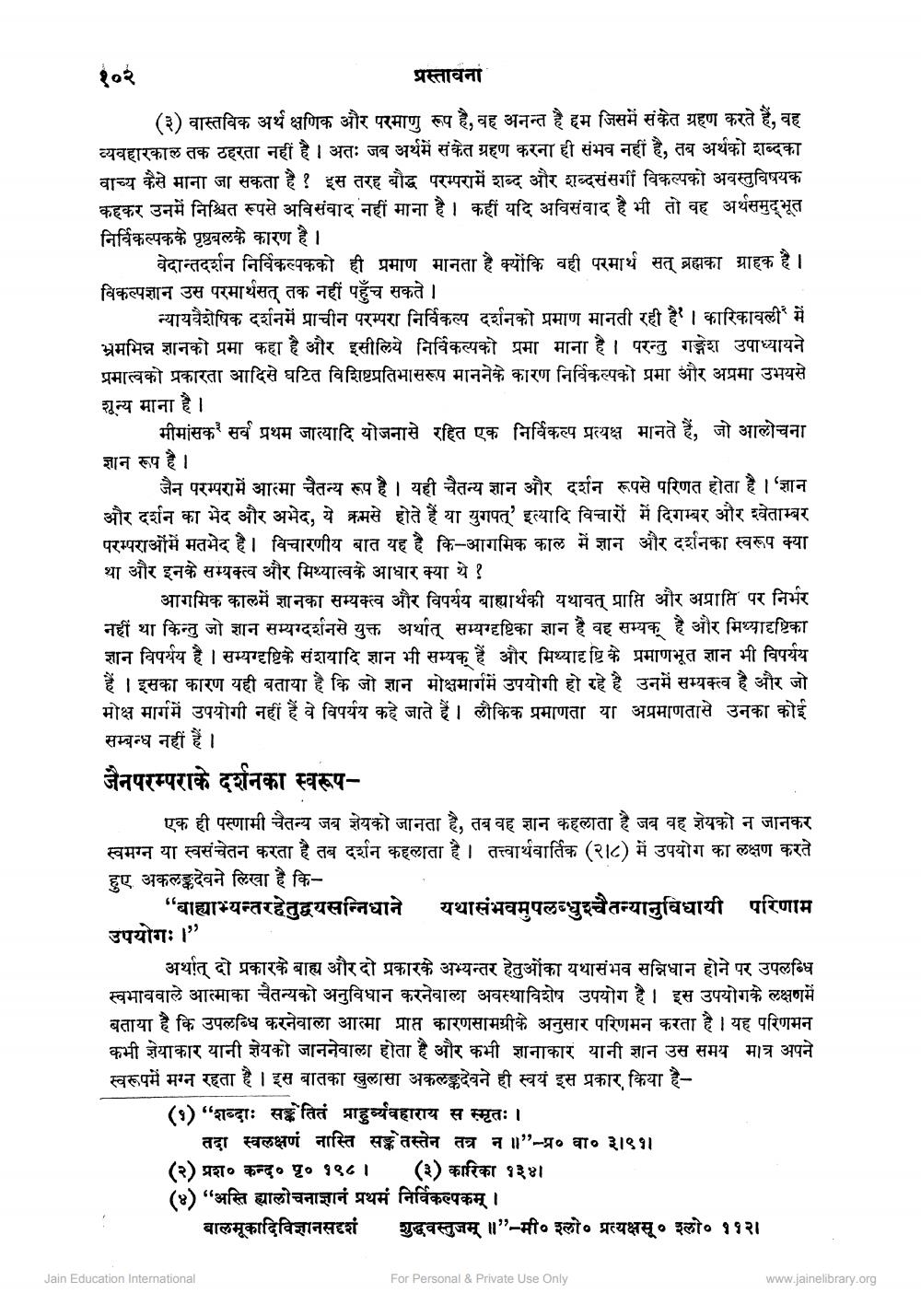________________
प्रस्तावना
___ (३) वास्तविक अर्थ क्षणिक और परमाणु रूप है, वह अनन्त है हम जिसमें संकेत ग्रहण करते हैं, वह व्यवहारकाल तक ठहरता नहीं है । अतः जब अर्थमें संकेत ग्रहण करना ही संभव नहीं है, तब अर्थको शब्दका वाच्य कैसे माना जा सकता है ? इस तरह बौद्ध परम्परामें शब्द और शब्दसंसर्गी विकल्पको अवस्तुविषयक कहकर उनमें निश्चित रूपसे अविसंवाद नहीं माना है। कहीं यदि अविसंवाद है भी तो वह अर्थसमुद्भूत निर्विकल्पकके पृष्ठबलके कारण है।
वेदान्तदर्शन निर्विकल्पकको ही प्रमाण मानता है क्योंकि वही परमार्थ सत् ब्रह्मका ग्राहक है । विकल्पज्ञान उस परमार्थसत् तक नहीं पहुँच सकते ।
न्यायवैशेषिक दर्शन में प्राचीन परम्परा निर्विकल्प दर्शनको प्रमाण मानती रही है । कारिकावली में भ्रमभिन्न ज्ञानको प्रमा कहा है और इसीलिये निर्विकल्पको प्रमा माना है । परन्तु गङ्गेश उपाध्यायने प्रमात्वको प्रकारता आदिसे घटित विशिष्टप्रतिभासरूप माननेके कारण निर्विकल्पको प्रमा और अप्रमा उभयसे शून्य माना है।
मीमांसकसर्व प्रथम जात्यादि योजनासे रहित एक निर्विकल्प प्रत्यक्ष मानते हैं, जो आलोचना ज्ञान रूप है।
जैन परम्परामें आत्मा चैतन्य रूप है । यही चैतन्य ज्ञान और दर्शन रूपसे परिणत होता है । 'ज्ञान और दर्शन का भेद और अभेद, ये क्रमसे होते हैं या युगपत्' इत्यादि विचारों में दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्पराओंमें मतभेद है। विचारणीय बात यह है कि-आगमिक काल में ज्ञान और दर्शनका स्वरूप क्या था और इनके सम्यक्त्व और मिथ्यात्वके आधार क्या थे ?
आगमिक कालमें ज्ञानका सम्यक्त्व और विपर्यय बाह्यार्थकी यथावत् प्राप्ति और अप्राप्ति पर निर्भर नहीं था किन्तु जो ज्ञान सम्यग्दर्शनसे युक्त अर्थात् सम्यग्दृष्टिका ज्ञान है वह सम्यक् है और मिथ्यादृष्टिका ज्ञान विपर्यय है । सम्यग्दृष्टिके संशयादि ज्ञान भी सम्यक् हैं और मिथ्यादृष्टि के प्रमाणभूत ज्ञान भी विपर्यय हैं । इसका कारण यही बताया है कि जो ज्ञान मोक्षमार्गमें उपयोगी हो रहे है उनमें सम्यक्त्व है और जो मोक्ष मार्गमें उपयोगी नहीं हैं वे विपर्यय कहे जाते हैं। लौकिक प्रमाणता या अप्रमाणतासे उनका कोई सम्बन्ध नहीं हैं। जैनपरम्पराके दर्शनका स्वरूप
एक ही परणामी चैतन्य जब ज्ञेयको जानता है, तब वह ज्ञान कहलाता है जब वह ज्ञेयको न जानकर स्वमग्न या स्वसंचेतन करता है तब दर्शन कहलाता है। तत्वार्थवार्तिक (२।८) में उपयोग का लक्षण करते हुए अकलङ्कदेवने लिखा है कि
"बाह्याभ्यन्तरहेतुद्वयसन्निधाने यथासंभवमुपलब्धुश्चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोगः।"
____ अर्थात् दो प्रकारके बाह्य और दो प्रकारके अभ्यन्तर हेतुओंका यथासंभव सन्निधान होने पर उपलब्धि स्वभाववाले आत्माका चैतन्यको अनुविधान करनेवाला अवस्था विशेष उपयोग है। इस उपयोगके लक्षणों बताया है कि उपलब्धि करनेवाला आत्मा प्राप्त कारणसामग्रीके अनुसार परिणमन करता है। यह परिणमन कभी ज्ञेयाकार यानी ज्ञेयको जाननेवाला होता है और कभी ज्ञानाकार यानी ज्ञान उस समय मात्र अपने स्वरूपमें मग्न रहता है । इस बातका खुलासा अकलङ्कदेवने ही स्वयं इस प्रकार किया है
(१) "शब्दाः सङ्केतितं प्राहुर्व्यवहाराय स स्मृतः ।
तदा स्वलक्षणं नास्ति सङ्केतस्तेन तत्र न ॥"-प्र० वा. ३॥९॥ (२) प्रश० कन्द. पृ० १९८ । (३) कारिका १३४॥ (४) "अस्ति ह्यालोचनाज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम् ।
बालमूकादिविज्ञानसदृशं शुद्धवस्तुजम् ॥"-मी० श्लो. प्रत्यक्षसू० श्लो. ११२॥
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org