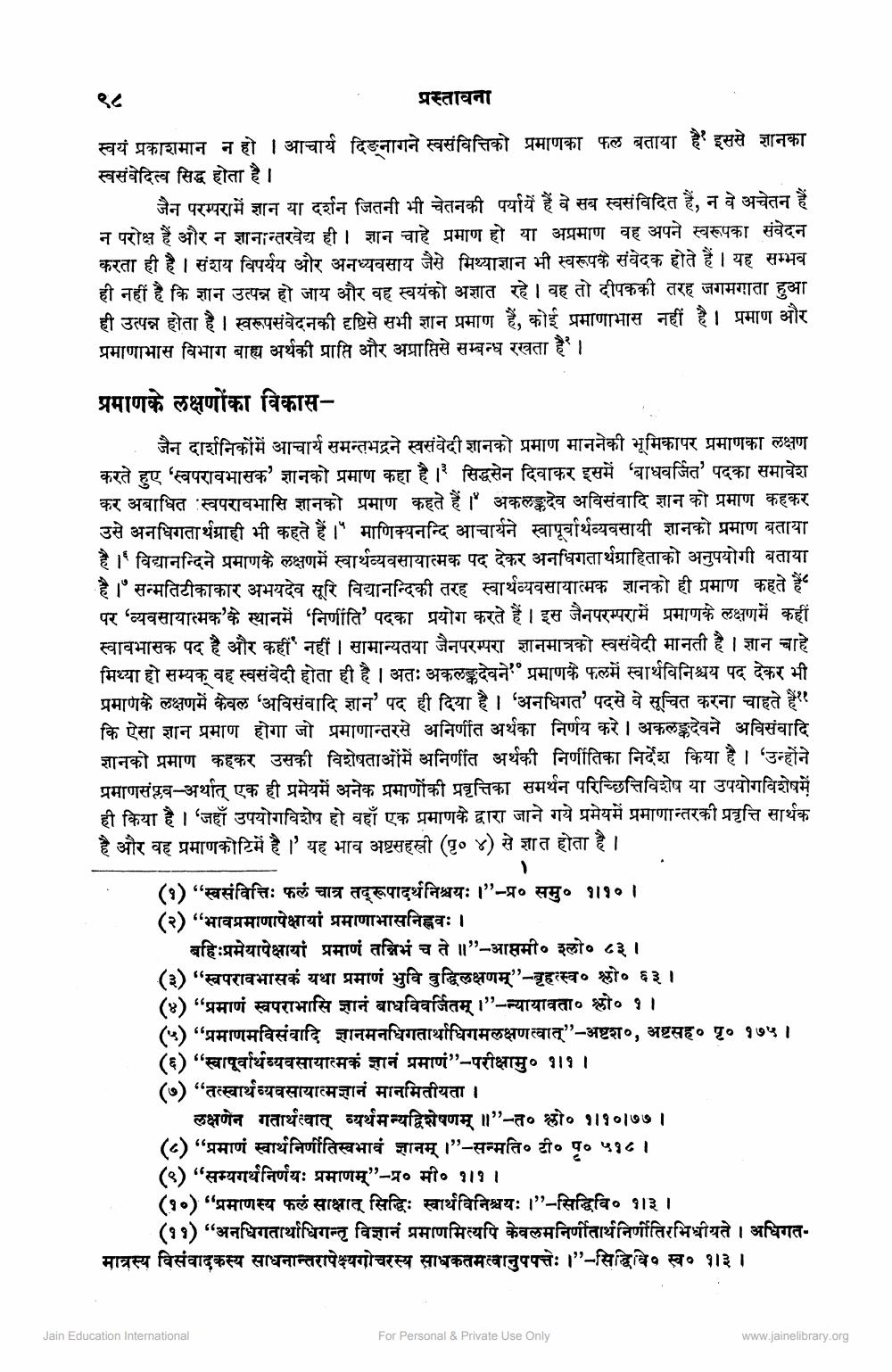________________
प्रस्तावना
स्वयं प्रकाशमान न हो । आचार्य दिङ्नागने स्वसंवित्तिको प्रमाणका फल बताया है इससे ज्ञानका स्वसंवेदित्व सिद्ध होता है।
जैन परम्परामें ज्ञान या दर्शन जितनी भी चेतनकी पर्यायें हैं वे सब स्वसंविदित हैं, न वे अचेतन हैं न परोक्ष हैं और न ज्ञानान्तरवेद्य ही। ज्ञान चाहे प्रमाण हो या अप्रमाण वह अपने स्वरूपका संवेदन करता ही है । संशय विपर्यय और अनध्यवसाय जैसे मिथ्याज्ञान भी स्वरूपके संवेदक होते हैं । यह सम्भव ही नहीं है कि ज्ञान उत्पन्न हो जाय और वह स्वयंको अज्ञात रहे । वह तो दीपककी तरह जगमगाता हुआ ही उत्पन्न होता है । स्वरूपसंवेदनकी दृष्टि से सभी ज्ञान प्रमाण हैं, कोई प्रमाणाभास नहीं है। प्रमाण और प्रमाणाभास विभाग बाह्य अर्थकी प्राप्ति और अप्राप्तिसे सम्बन्ध रखता है।
प्रमाणके लक्षणोंका विकास
जैन दार्शनिकोंमें आचार्य समन्तभद्रने स्वसंवेदी ज्ञानको प्रमाण माननेकी भूमिकापर प्रमाणका लक्षण करते हुए 'स्वपरावभासक' ज्ञानको प्रमाण कहा है । सिद्धसेन दिवाकर इसमें 'बाधवर्जित' पदका समावेश कर अबाधित ‘स्वपरावभासि ज्ञानको प्रमाण कहते हैं। अकलङ्कदेव अविसंवादि ज्ञान को प्रमाण कहकर उसे अनधिगतार्थग्राही भी कहते हैं । माणिक्यनन्दि आचार्यने स्वापूर्वार्थव्यवसायी ज्ञानको प्रमाण बताया है। विद्यानन्दिने प्रमाणके लक्षणमें स्वार्थव्यवसायात्मक पद देकर अनधिगतार्थग्राहिताको अनुपयोगी बताया है । सन्मतिटीकाकार अभयदेव सूरि विद्यानन्दिकी तरह स्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञानको ही प्रमाण कहते हैं। पर 'व्यवसायात्मक'के स्थानमें 'निणीति' पदका प्रयोग करते हैं । इस जैनपरम्परामें प्रमाणके लक्षणमें कहीं स्वावभासक पद है और कहीं नहीं । सामान्यतया जैनपरम्परा ज्ञानमात्रको स्वसंवेदी मानती है । ज्ञान चाहे मिथ्या हो सम्यक् वह स्वसंवेदी होता ही है । अतः अकलङ्कदेवने" प्रमाणके फलमें स्वार्थविनिश्चय पद देकर भी प्रमाणके लक्षणमें केवल 'अविसंवादि ज्ञान' पद ही दिया है। 'अनधिगत' पदसे वे सूचित करना चाहते है। कि ऐसा ज्ञान प्रमाण होगा जो प्रमाणान्तरसे अनिर्णीत अर्थका निर्णय करे । अकलङ्कदेवने अविसंवादि ज्ञानको प्रमाण कहकर उसकी विशेषताओंमें अनिर्णीत अर्थकी निणीतिका निर्देश किया है । 'उन्होंने प्रमाणसंप्लव-अर्थात् एक ही प्रमेयमें अनेक प्रमाणोंकी प्रवृत्तिका समर्थन परिच्छित्तिविशेष या उपयोगविशेषमें ही किया है । 'जहाँ उपयोगविशेष हो वहाँ एक प्रमाणके द्वारा जाने गये प्रमेयमें प्रमाणान्तरकी प्रवृत्ति सार्थक है और वह प्रमाणकोटिमें है।' यह भाव अष्टसहस्री (पृ० ४) से ज्ञात होता है।
(१) "स्वसंवित्तिः फलं चात्र तद्पादर्थनिश्चयः ।"-प्र० समु. १।१०। ) "भावप्रमाणापेक्षायां प्रमाणाभासनिवः ।
बहिःप्रमेयापेक्षायां प्रमाणं तन्निभं च ते ॥"-आप्तमी० श्लो० ८३ । (३) "स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्"-बृहरस्व० श्लो० ६३ । ) "प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं बाधविवर्जितम् ।"-न्यायावता० श्लो०१।
) "प्रमाणमविसंवादि ज्ञानमनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात्"-अष्टश०, अष्टसह. पृ० १७५। (६) "स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणं"-परीक्षामु० १।। (७) "तत्स्वार्थव्यवसायात्मज्ञानं मानमितीयता । __ लक्षणेन गतार्थत्वात् व्यर्थमन्यद्विशेषणम् ॥"-त० श्लो० ११०७७ । (6) "प्रमाणं स्वार्थनिर्णीतिस्वभावं ज्ञानम् ।"-सन्मति० टी० पृ० ५१८ । (९) "सम्यगर्थनिर्णयः प्रमाणम्"-प्र० मी० ११। (१०)"प्रमाणस्य फलं साक्षात् सिद्धिः स्वार्थविनिश्चयः।"-सिद्धिवि. १३ ।
(११) “अनधिगतार्थाधिगन्तृ विज्ञानं प्रमाणमित्यपि केवलमनिर्णीतार्थनिर्णोतिरभिधीयते । अधिगत. मात्रस्य विसंवादकस्य साधनान्तरापेक्ष्यगोचरस्य साधकतमत्वानुपपत्तेः।"-सिद्धिविक स्व० १३ ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org