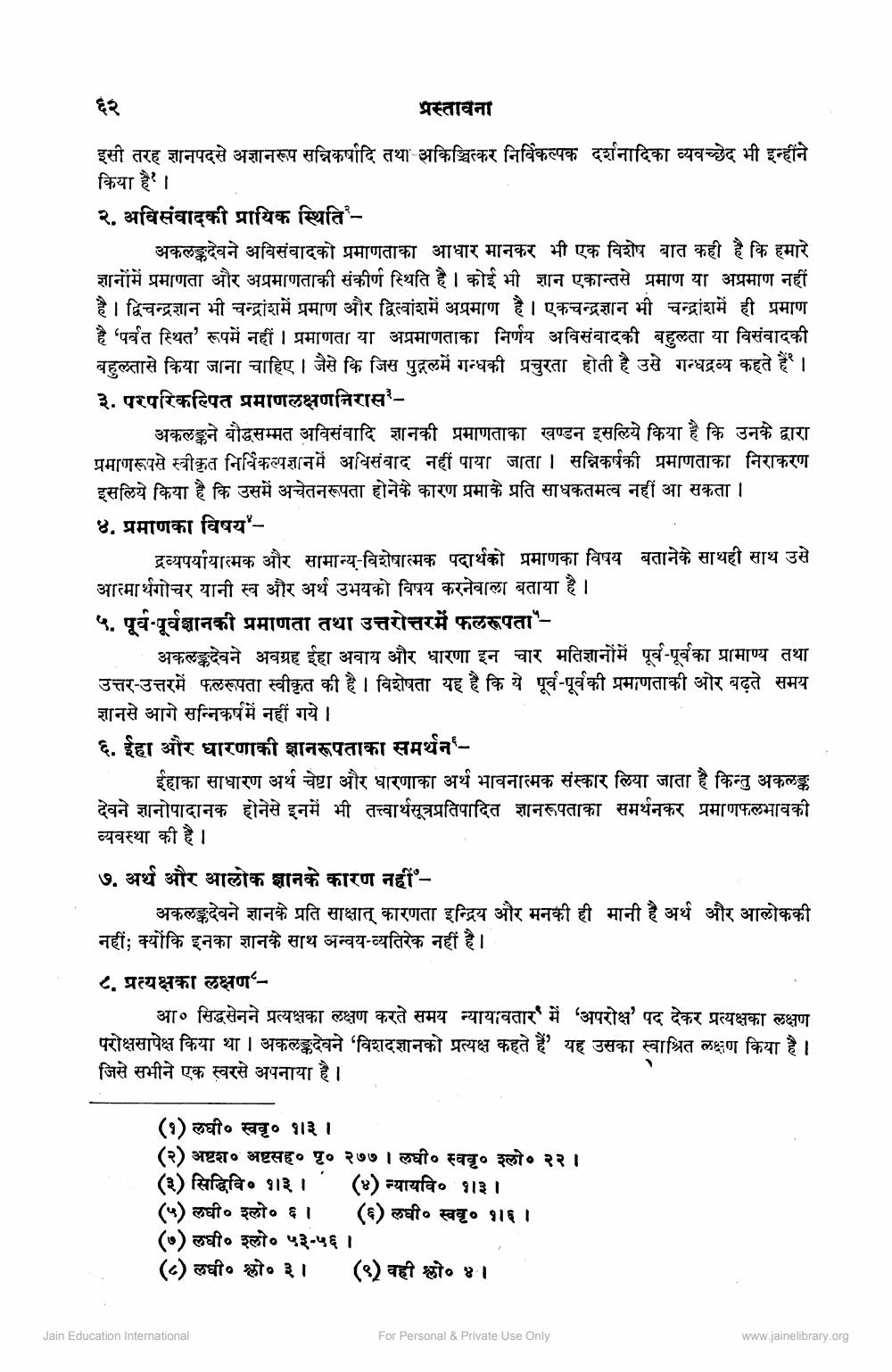________________
६२
प्रस्तावना
इसी तरह ज्ञानपदसे अज्ञानरूप सन्निकर्षादि तथा अकिञ्चित्कर निर्विकल्पक दर्शनादिका व्यवच्छेद भी इन्हींने किया है' ।
२. अविसंवादकी प्रायिक स्थिति :
अकलङ्कदेवने अविसंवादको प्रमाणताका आधार मानकर भी एक विशेष बात कही है कि हमारे ज्ञानोंमें प्रमाणता और अप्रमाणताकी संकीर्ण स्थिति है । कोई भी ज्ञान एकान्तसे प्रमाण या अप्रमाण नहीं है | द्विचन्द्रज्ञान भी चन्द्रांशमें प्रमाण और द्वित्वांश में अप्रमाण है । एकचन्द्रज्ञान भी चन्द्रांश में ही प्रमाण है 'पर्वत स्थित' रूपमें नहीं । प्रमाणता या अप्रमाणताका निर्णय अविसंवादकी बहुलता या विसंवादकी बहुलतासे किया जाना चाहिए। जैसे कि जिस पुद्गलमें गन्धकी प्रचुरता होती है उसे गन्धद्रव्य कहते हैं । ३. परपरिकल्पित प्रमाणलक्षणनिरास'
अकलङ्कने बौद्धसम्मत अविसंवादि ज्ञानकी प्रमाणताका खण्डन इसलिये किया है कि उनके द्वारा प्रमाणरूप से स्वीकृत निर्विकल्पज्ञान में अविसंवाद नहीं पाया जाता । सन्निकर्षकी प्रमाणताका निराकरण इसलिये किया है कि उसमें अचेतनरूपता होने के कारण प्रमाके प्रति साधकतमत्व नहीं आ सकता । ४. प्रमाणका विषय -
द्रव्यपर्यायात्मक और सामान्य विशेषात्मक पदार्थको प्रमाणका विषय बतानेके साथही साथ उसे आत्मार्थगोचर यानी स्व और अर्थ उभयको विषय करनेवाला बताया है ।
५. पूर्व - पूर्वज्ञान की प्रमाणता तथा उत्तरोत्तर में फलरूपता -
अकलङ्कदेवने अवग्रह हा अवाय और धारणा इन चार मतिज्ञानों में पूर्व - पूर्वका प्रामाण्य तथा उत्तर- उत्तर में फलरूपता स्वीकृत की है । विशेषता यह है कि ये पूर्व-पूर्व की प्रमाणता की ओर बढ़ते समय ज्ञानसे आगे सन्निकर्ष में नहीं गये ।
६. ईहा और धारणाकी ज्ञानरूपताका समर्थन'
ईहाका साधारण अर्थ चेष्टा और धारणाका अर्थ भावनात्मक संस्कार लिया जाता है किन्तु अकलङ्क देवने ज्ञानोपादानक होनेसे इनमें भी तत्त्वार्थसूत्रप्रतिपादित ज्ञानरूपताका समर्थनकर प्रमाणफलभाव की व्यवस्था की है ।
७. अर्थ और आलोक ज्ञानके कारण नहीं -
अकलङ्कदेवने ज्ञानके प्रति साक्षात् कारणता इन्द्रिय और मनकी ही मानी है अर्थ और आलोककी नहीं; क्योंकि इनका ज्ञानके साथ अन्वयव्यतिरेक नहीं है ।
८. प्रत्यक्षका लक्षण'
आ० सिद्धसेनने प्रत्यक्षका लक्षण करते समय न्यायावतार' में 'अपरोक्ष' पद देकर प्रत्यक्षका लक्षण परोक्षसापेक्ष किया था । अकलङ्कदेवने 'विशदज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं' यह उसका स्वाश्रित लक्षण किया है । जिसे सभीने एक स्वरसे अपनाया है ।
、
( १ ) लघी० स्ववृ० १३ ॥
(२) अष्टश० अष्टसह० पृ० २७७ । लघी० स्ववृ० श्लो० २२ ।
(४) न्यायवि० १ । ३ ।
(६) लघी० स्ववृ० ११६ ॥
(३) सिद्धिवि० १।३ । (५) लघी० श्लो० ६ । (७) लघी० श्लो० ५३-५६ (८) लघी० लो० ३ ।
Jain Education International
।
(९) वही श्लो० ४ ।
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org