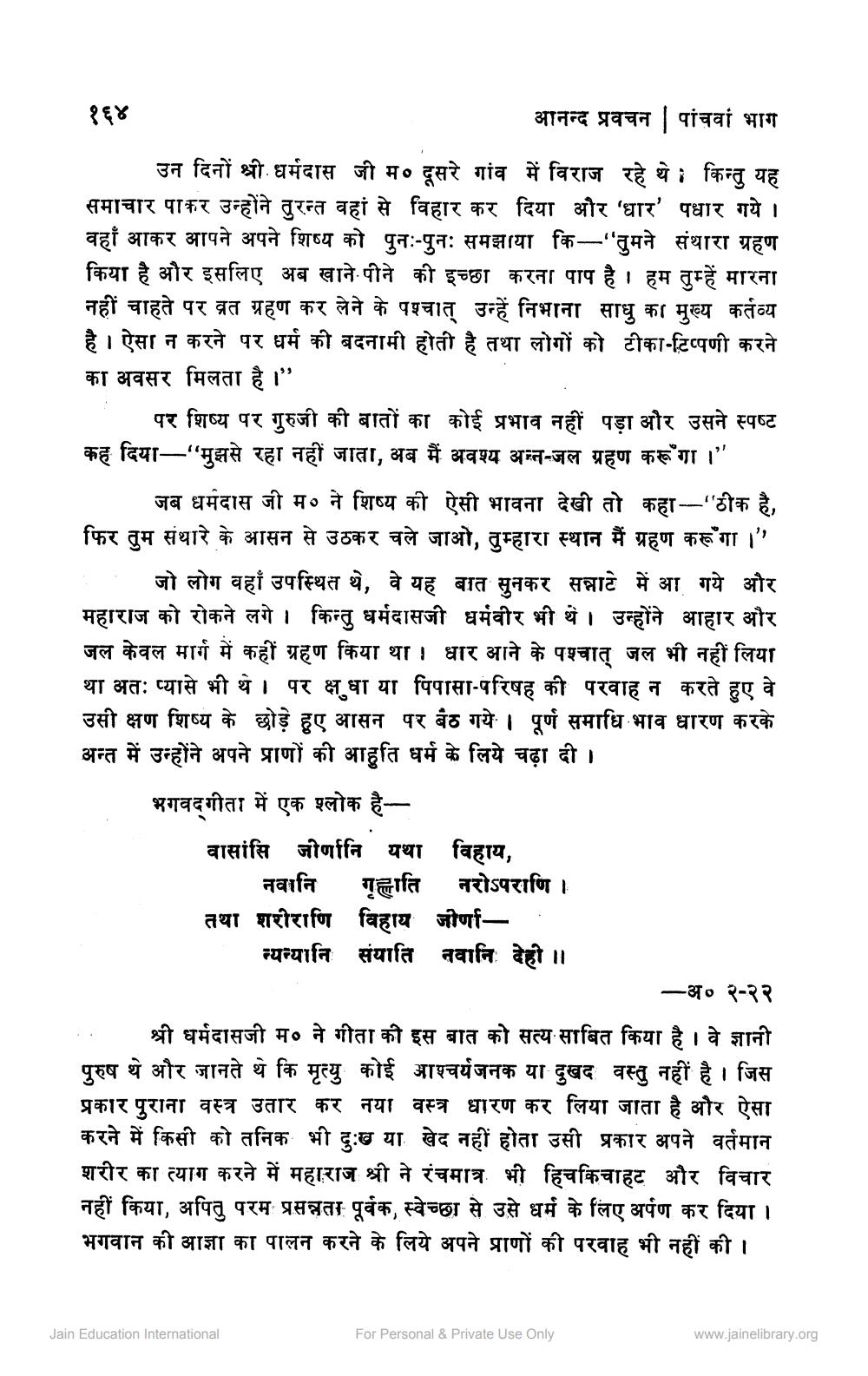________________
१६४
आनन्द प्रवचन | पांचवां भाग
उन दिनों श्री धर्मदास जी म० दूसरे गांव में विराज रहे थे। किन्तु यह समाचार पाकर उन्होंने तुरन्त वहां से विहार कर दिया और 'धार' पधार गये । वहाँ आकर आपने अपने शिष्य को पुनः-पुनः समझाया कि-"तुमने संथारा ग्रहण किया है और इसलिए अब खाने पीने की इच्छा करना पाप है। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते पर व्रत ग्रहण कर लेने के पश्चात् उन्हें निभाना साधु का मुख्य कर्तव्य है। ऐसा न करने पर धर्म की बदनामी होती है तथा लोगों को टीका-टिप्पणी करने का अवसर मिलता है।"
पर शिष्य पर गुरुजी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने स्पष्ट कह दिया- "मुझसे रहा नहीं जाता, अब मैं अवश्य अन्न-जल ग्रहण करूंगा।"
जब धर्मदास जी म० ने शिष्य की ऐसी भावना देखी तो कहा-"ठीक है, फिर तुम संथारे के आसन से उठकर चले जाओ, तुम्हारा स्थान मैं ग्रहण करूंगा।'
जो लोग वहाँ उपस्थित थे, वे यह बात सुनकर सन्नाटे में आ गये और महाराज को रोकने लगे। किन्तु धर्मदासजी धर्मवीर भी थे। उन्होंने आहार और जल केवल मार्ग में कहीं ग्रहण किया था। धार आने के पश्चात् जल भी नहीं लिया था अतः प्यासे भी थे। पर क्ष धा या पिपासा-परिषह की परवाह न करते हुए वे उसी क्षण शिष्य के छोड़े हुए आसन पर बैठ गये । पूर्ण समाधि भाव धारण करके अन्त में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति धर्म के लिये चढ़ा दी। भगवद्गीता में एक श्लोक हैवासांसि जीर्णानि यथा विहाय,
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥
-अ० २-२२ श्री धर्मदासजी म० ने गीता की इस बात को सत्य साबित किया है। वे ज्ञानी पुरुष थे और जानते थे कि मृत्यु कोई आश्चर्यजनक या दुखद वस्तु नहीं है । जिस प्रकार पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र धारण कर लिया जाता है और ऐसा करने में किसी को तनिक भी दुःख या खेद नहीं होता उसी प्रकार अपने वर्तमान शरीर का त्याग करने में महाराज श्री ने रंचमात्र भी हिचकिचाहट और विचार नहीं किया, अपितु परम प्रसन्नता पूर्वक, स्वेच्छा से उसे धर्म के लिए अर्पण कर दिया। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिये अपने प्राणों की परवाह भी नहीं की।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org