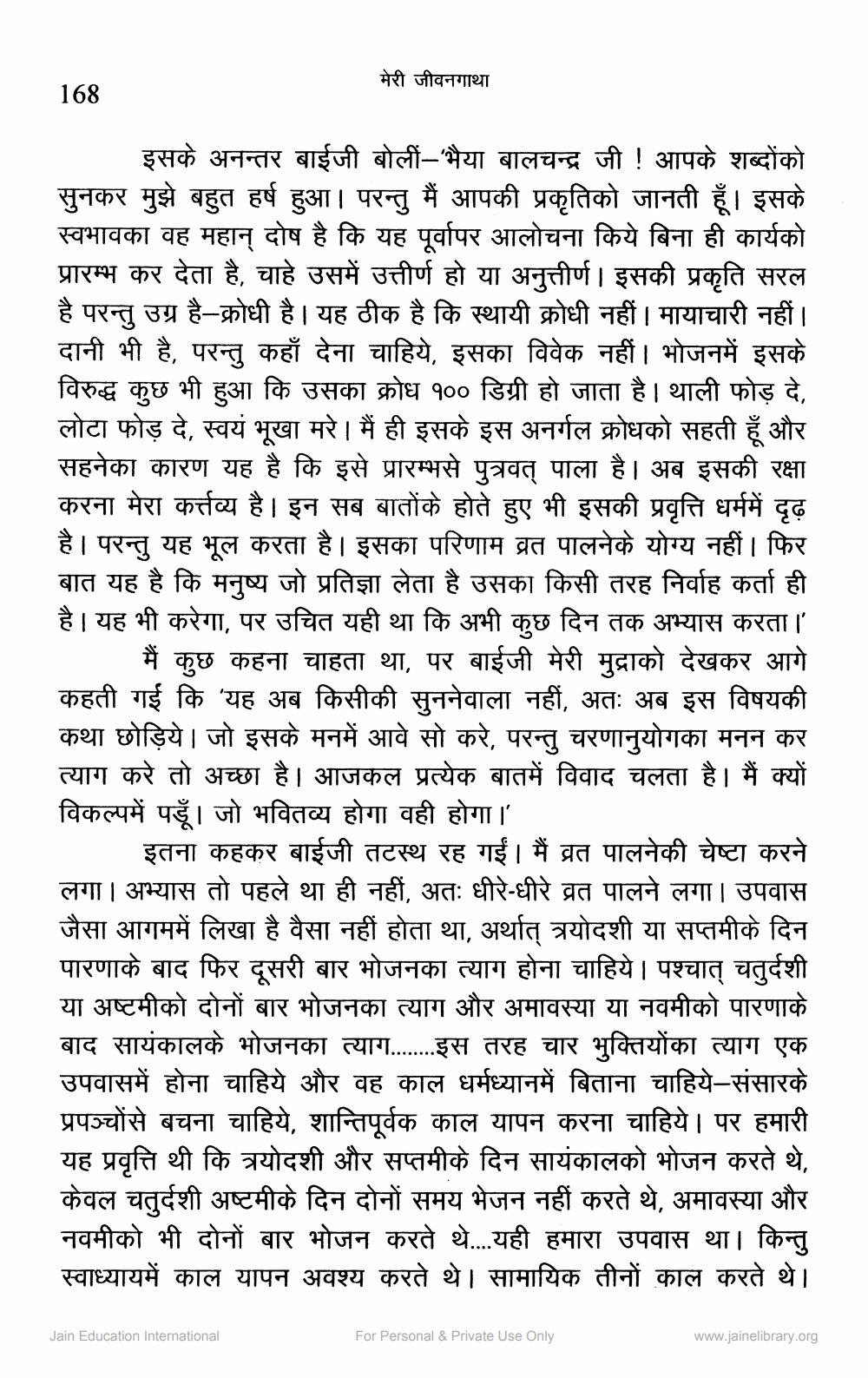________________
मेरी जीवनगाथा
168
इसके अनन्तर बाईजी बोलीं-"भैया बालचन्द्र जी ! आपके शब्दोंको सुनकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। परन्तु मैं आपकी प्रकृतिको जानती हूँ। इसके स्वभावका वह महान् दोष है कि यह पूर्वापर आलोचना किये बिना ही कार्यको प्रारम्भ कर देता है, चाहे उसमें उत्तीर्ण हो या अनुत्तीर्ण । इसकी प्रकृति सरल है परन्तु उग्र है-क्रोधी है। यह ठीक है कि स्थायी क्रोधी नहीं। मायाचारी नहीं। दानी भी है, परन्तु कहाँ देना चाहिये, इसका विवेक नहीं। भोजनमें इसके विरुद्ध कुछ भी हुआ कि उसका क्रोध १०० डिग्री हो जाता है। थाली फोड़ दे, लोटा फोड़ दे, स्वयं भूखा मरे । मैं ही इसके इस अनर्गल क्रोधको सहती हूँ और सहनेका कारण यह है कि इसे प्रारम्भसे पुत्रवत् पाला है। अब इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इन सब बातोंके होते हुए भी इसकी प्रवृत्ति धर्ममें दृढ़ है। परन्तु यह भूल करता है। इसका परिणाम व्रत पालनेके योग्य नहीं। फिर बात यह है कि मनुष्य जो प्रतिज्ञा लेता है उसका किसी तरह निर्वाह कर्ता ही है। यह भी करेगा, पर उचित यही था कि अभी कुछ दिन तक अभ्यास करता।'
मैं कुछ कहना चाहता था, पर बाईजी मेरी मुद्राको देखकर आगे कहती गई कि 'यह अब किसीकी सुननेवाला नहीं, अतः अब इस विषयकी कथा छोड़िये । जो इसके मनमें आवे सो करे, परन्तु चरणानुयोगका मनन कर त्याग करे तो अच्छा है। आजकल प्रत्येक बातमें विवाद चलता है। मैं क्यों विकल्पमें पडूं। जो भवितव्य होगा वही होगा।'
इतना कहकर बाईजी तटस्थ रह गईं। मैं व्रत पालनेकी चेष्टा करने लगा। अभ्यास तो पहले था ही नहीं, अतः धीरे-धीरे व्रत पालने लगा। उपवास जैसा आगममें लिखा है वैसा नहीं होता था, अर्थात् त्रयोदशी या सप्तमीके दिन पारणाके बाद फिर दूसरी बार भोजनका त्याग होना चाहिये। पश्चात् चतुर्दशी या अष्टमीको दोनों बार भोजनका त्याग और अमावस्या या नवमीको पारणाके बाद सायंकालके भोजनका त्याग........इस तरह चार भूक्तियोंका त्याग एक उपवासमें होना चाहिये और वह काल धर्मध्यानमें बिताना चाहिये-संसारके प्रपञ्चोंसे बचना चाहिये, शान्तिपूर्वक काल यापन करना चाहिये। पर हमारी यह प्रवृत्ति थी कि त्रयोदशी और सप्तमीके दिन सायंकालको भोजन करते थे, केवल चतुर्दशी अष्टमीके दिन दोनों समय भेजन नहीं करते थे, अमावस्या और नवमीको भी दोनों बार भोजन करते थे....यही हमारा उपवास था। किन्तु स्वाध्यायमें काल यापन अवश्य करते थे। सामायिक तीनों काल करते थे।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org