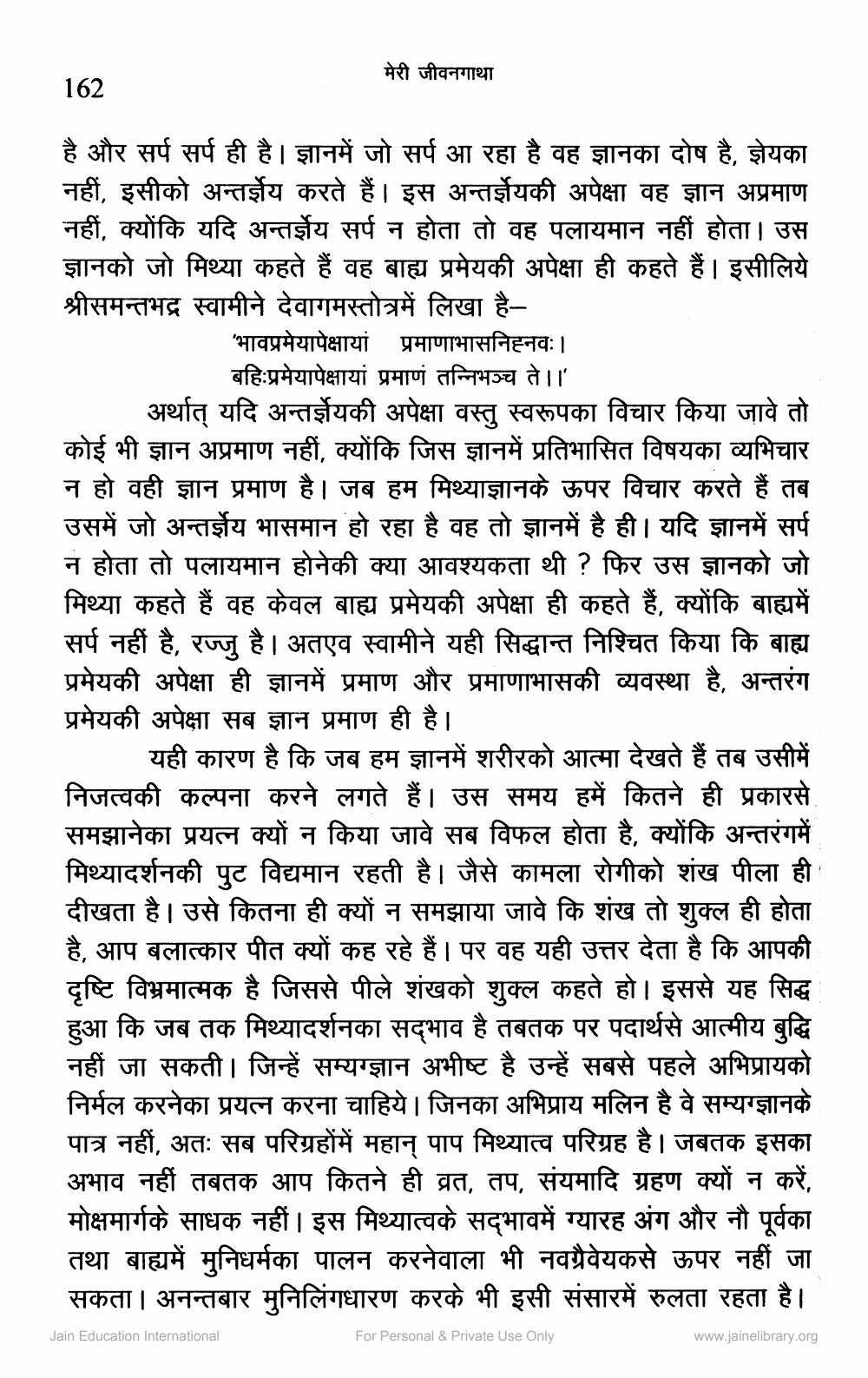________________
मेरी जीवनगाथा
162
है और सर्प सर्प ही है। ज्ञानमें जो सर्प आ रहा है वह ज्ञानका दोष है, ज्ञेयका नहीं, इसीको अन्तर्जेय करते हैं। इस अन्त यकी अपेक्षा वह ज्ञान अप्रमाण नहीं, क्योंकि यदि अन्तर्जेय सर्प न होता तो वह पलायमान नहीं होता। उस ज्ञानको जो मिथ्या कहते हैं वह बाह्य प्रमेयकी अपेक्षा ही कहते हैं। इसीलिये श्रीसमन्तभद्र स्वामीने देवागमस्तोत्रमें लिखा है
"भावप्रमेयापेक्षायां प्रमाणाभासनिह्नवः ।
__बहिःप्रमेयापेक्षायां प्रमाणं तन्निभञ्च ते।।' ___ अर्थात् यदि अन्तर्जेयकी अपेक्षा वस्तु स्वरूपका विचार किया जावे तो कोई भी ज्ञान अप्रमाण नहीं, क्योंकि जिस ज्ञानमें प्रतिभासित विषयका व्यभिचार न हो वही ज्ञान प्रमाण है। जब हम मिथ्याज्ञानके ऊपर विचार करते हैं तब उसमें जो अन्तर्जेय भासमान हो रहा है वह तो ज्ञानमें है ही। यदि ज्ञानमें सर्प न होता तो पलायमान होनेकी क्या आवश्यकता थी ? फिर उस ज्ञानको जो मिथ्या कहते हैं वह केवल बाह्य प्रमेयकी अपेक्षा ही कहते हैं, क्योंकि बाह्यमें सर्प नहीं है, रज्जु है। अतएव स्वामीने यही सिद्धान्त निश्चित किया कि बाह्य प्रमेयकी अपेक्षा ही ज्ञानमें प्रमाण और प्रमाणाभासकी व्यवस्था है, अन्तरंग प्रमेयकी अपेक्षा सब ज्ञान प्रमाण ही है।
यही कारण है कि जब हम ज्ञानमें शरीरको आत्मा देखते हैं तब उसीमें निजत्वकी कल्पना करने लगते हैं। उस समय हमें कितने ही प्रकारसे समझानेका प्रयत्न क्यों न किया जावे सब विफल होता है, क्योंकि अन्तरंगमें मिथ्यादर्शनकी पुट विद्यमान रहती है। जैसे कामला रोगीको शंख पीला ही दीखता है। उसे कितना ही क्यों न समझाया जावे कि शंख तो शुक्ल ही होता है, आप बलात्कार पीत क्यों कह रहे हैं। पर वह यही उत्तर देता है कि आपकी दृष्टि विभ्रमात्मक है जिससे पीले शंखको शुक्ल कहते हो। इससे यह सिद्ध हुआ कि जब तक मिथ्यादर्शनका सद्भाव है तबतक पर पदार्थसे आत्मीय बुद्धि नहीं जा सकती। जिन्हें सम्यग्ज्ञान अभीष्ट है उन्हें सबसे पहले अभिप्रायको निर्मल करनेका प्रयत्न करना चाहिये। जिनका अभिप्राय मलिन है वे सम्यग्ज्ञानके पात्र नहीं, अतः सब परिग्रहोंमें महान् पाप मिथ्यात्व परिग्रह है। जबतक इसका अभाव नहीं तबतक आप कितने ही व्रत, तप, संयमादि ग्रहण क्यों न करें, मोक्षमार्गके साधक नहीं। इस मिथ्यात्वके सद्भावमें ग्यारह अंग और नौ पूर्वका तथा बाह्यमें मुनिधर्मका पालन करनेवाला भी नवग्रैवेयकसे ऊपर नहीं जा सकता। अनन्तबार मुनिलिंगधारण करके भी इसी संसारमें रुलता रहता है।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org