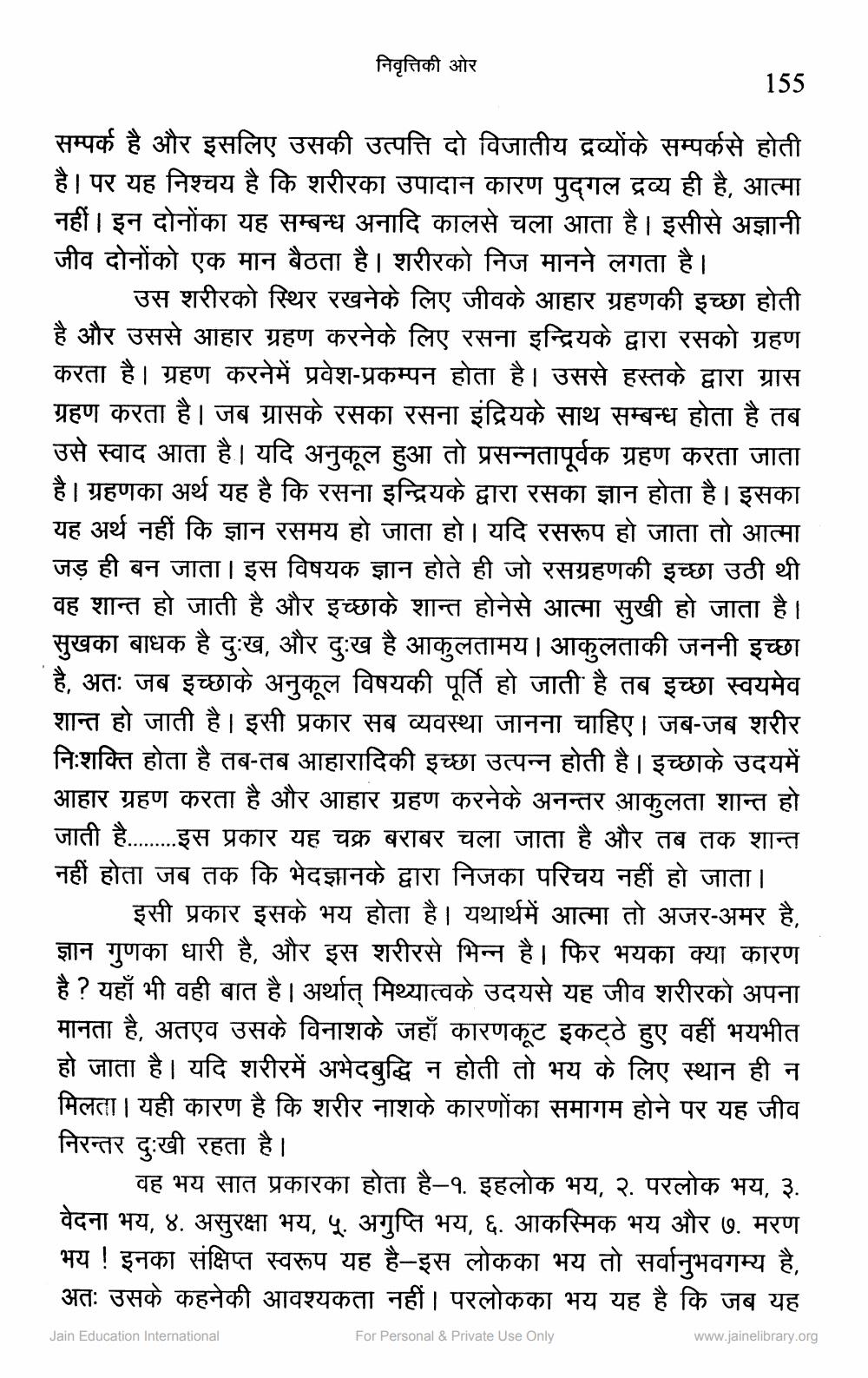________________
निवृत्तिकी ओर
155
सम्पर्क है और इसलिए उसकी उत्पत्ति दो विजातीय द्रव्योंके सम्पर्कसे होती है। पर यह निश्चय है कि शरीरका उपादान कारण पुद्गल द्रव्य ही है, आत्मा नहीं। इन दोनोंका यह सम्बन्ध अनादि कालसे चला आता है। इसीसे अज्ञानी जीव दोनोंको एक मान बैठता है। शरीरको निज मानने लगता है।
उस शरीरको स्थिर रखनेके लिए जीवके आहार ग्रहणकी इच्छा होती है और उससे आहार ग्रहण करनेके लिए रसना इन्द्रियके द्वारा रसको ग्रहण करता है। ग्रहण करनेमें प्रवेश-प्रकम्पन होता है। उससे हस्तके द्वारा ग्रास ग्रहण करता है। जब ग्रासके रसका रसना इंद्रियके साथ सम्बन्ध होता है तब उसे स्वाद आता है। यदि अनुकूल हुआ तो प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करता जाता है। ग्रहणका अर्थ यह है कि रसना इन्द्रियके द्वारा रसका ज्ञान होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञान रसमय हो जाता हो । यदि रसरूप हो जाता तो आत्मा जड़ ही बन जाता। इस विषयक ज्ञान होते ही जो रसग्रहणकी इच्छा उठी थी वह शान्त हो जाती है और इच्छाके शान्त होनेसे आत्मा सुखी हो जाता है। सुखका बाधक है दुःख, और दुःख है आकुलतामय । आकुलताकी जननी इच्छा है, अतः जब इच्छाके अनुकूल विषयकी पूर्ति हो जाती है तब इच्छा स्वयमेव शान्त हो जाती है। इसी प्रकार सब व्यवस्था जानना चाहिए। जब-जब शरीर निःशक्ति होता है तब-तब आहारादिकी इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छाके उदयमें आहार ग्रहण करता है और आहार ग्रहण करनेके अनन्तर आकुलता शान्त हो जाती है.........इस प्रकार यह चक्र बराबर चला जाता है और तब तक शान्त नहीं होता जब तक कि भेदज्ञानके द्वारा निजका परिचय नहीं हो जाता।
इसी प्रकार इसके भय होता है। यथार्थमें आत्मा तो अजर-अमर है, ज्ञान गुणका धारी है, और इस शरीरसे भिन्न है। फिर भयका क्या कारण है ? यहाँ भी वही बात है। अर्थात् मिथ्यात्वके उदयसे यह जीव शरीरको अपना मानता है, अतएव उसके विनाशके जहाँ कारणकट इकट्ठे हुए वहीं भयभीत हो जाता है। यदि शरीरमें अभेदबुद्धि न होती तो भय के लिए स्थान ही न मिलता । यही कारण है कि शरीर नाशके कारणोंका समागम होने पर यह जीव निरन्तर दुःखी रहता है।
वह भय सात प्रकारका होता है-१. इहलोक भय, २. परलोक भय, ३. वेदना भय, ४. असुरक्षा भय, ५. अगुप्ति भय, ६. आकस्मिक भय और ७. मरण भय ! इनका संक्षिप्त स्वरूप यह है-इस लोकका भय तो सर्वानुभवगम्य है, अतः उसके कहनेकी आवश्यकता नहीं। परलोकका भय यह है कि जब यह
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org