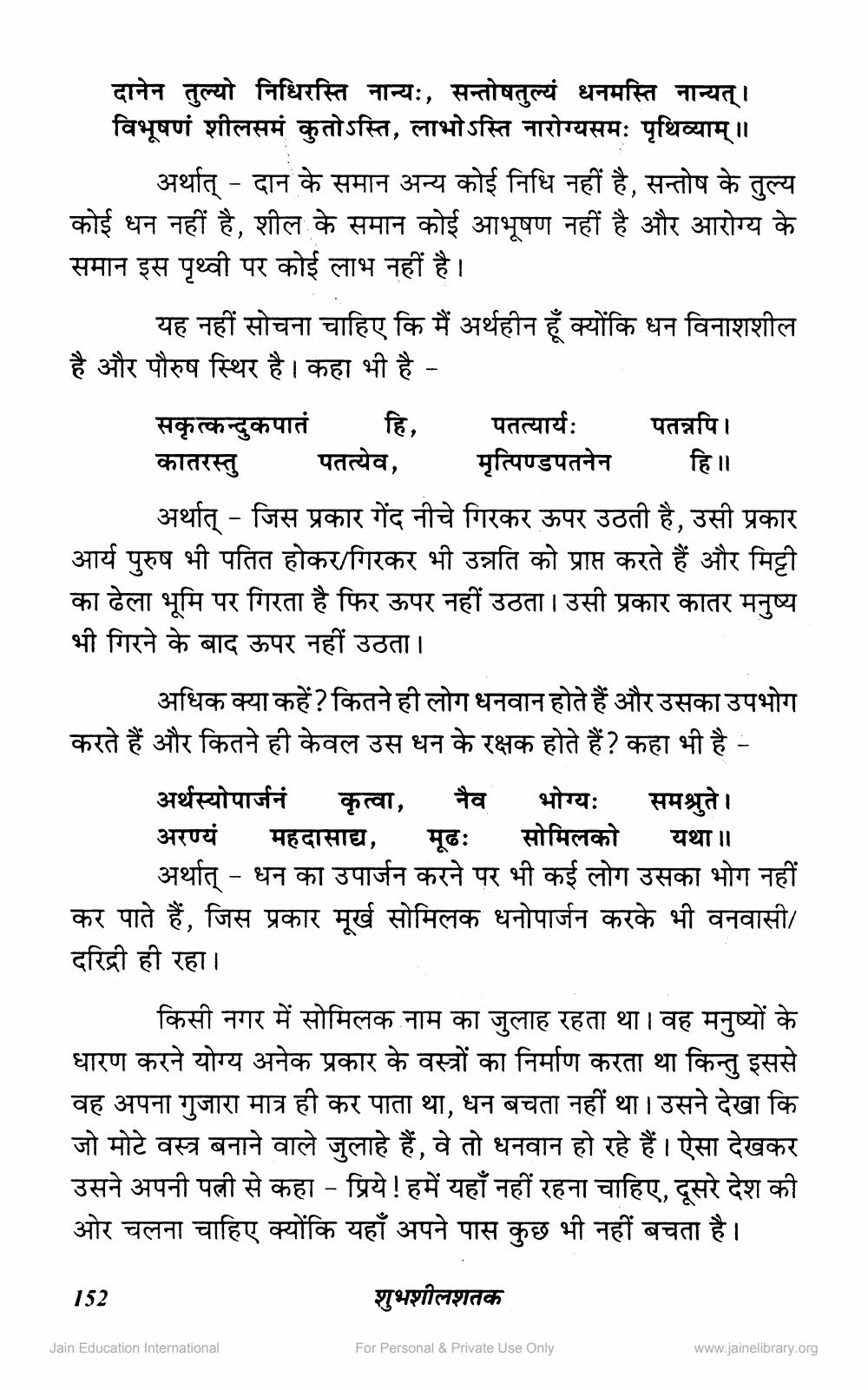________________
दानेन तुल्यो निधिरस्ति नान्यः, सन्तोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत्। विभूषणं शीलसमं कुतोऽस्ति, लाभोऽस्ति नारोग्यसमः पृथिव्याम्॥
___ अर्थात् - दान के समान अन्य कोई निधि नहीं है, सन्तोष के तुल्य कोई धन नहीं है, शील के समान कोई आभूषण नहीं है और आरोग्य के समान इस पृथ्वी पर कोई लाभ नहीं है।
___ यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं अर्थहीन हूँ क्योंकि धन विनाशशील है और पौरुष स्थिर है। कहा भी है -
सकृत्कन्दकपातं हि, पतत्यार्यः पतन्नपि। कातरस्तु पतत्येव, मृत्पिण्डपतनेन हि॥
अर्थात् - जिस प्रकार गेंद नीचे गिरकर ऊपर उठती है, उसी प्रकार आर्य पुरुष भी पतित होकर/गिरकर भी उन्नति को प्राप्त करते हैं और मिट्टी का ढेला भूमि पर गिरता है फिर ऊपर नहीं उठता। उसी प्रकार कातर मनुष्य भी गिरने के बाद ऊपर नहीं उठता।
__ अधिक क्या कहें? कितने ही लोग धनवान होते हैं और उसका उपभोग करते हैं और कितने ही केवल उस धन के रक्षक होते हैं? कहा भी है -
अर्थस्योपार्जनं कृत्वा, नैव भोग्यः समश्रुते। अरण्यं महदासाद्य, मूढः सोमिलको यथा ॥
अर्थात् - धन का उपार्जन करने पर भी कई लोग उसका भोग नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार मूर्ख सोमिलक धनोपार्जन करके भी वनवासी/ दरिद्री ही रहा।
किसी नगर में सोमिलक नाम का जुलाह रहता था। वह मनुष्यों के धारण करने योग्य अनेक प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करता था किन्तु इससे वह अपना गुजारा मात्र ही कर पाता था, धन बचता नहीं था। उसने देखा कि जो मोटे वस्त्र बनाने वाले जुलाहे हैं, वे तो धनवान हो रहे हैं। ऐसा देखकर उसने अपनी पत्नी से कहा – प्रिये ! हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, दूसरे देश की ओर चलना चाहिए क्योंकि यहाँ अपने पास कुछ भी नहीं बचता है।
152
शुभशीलशतक
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org