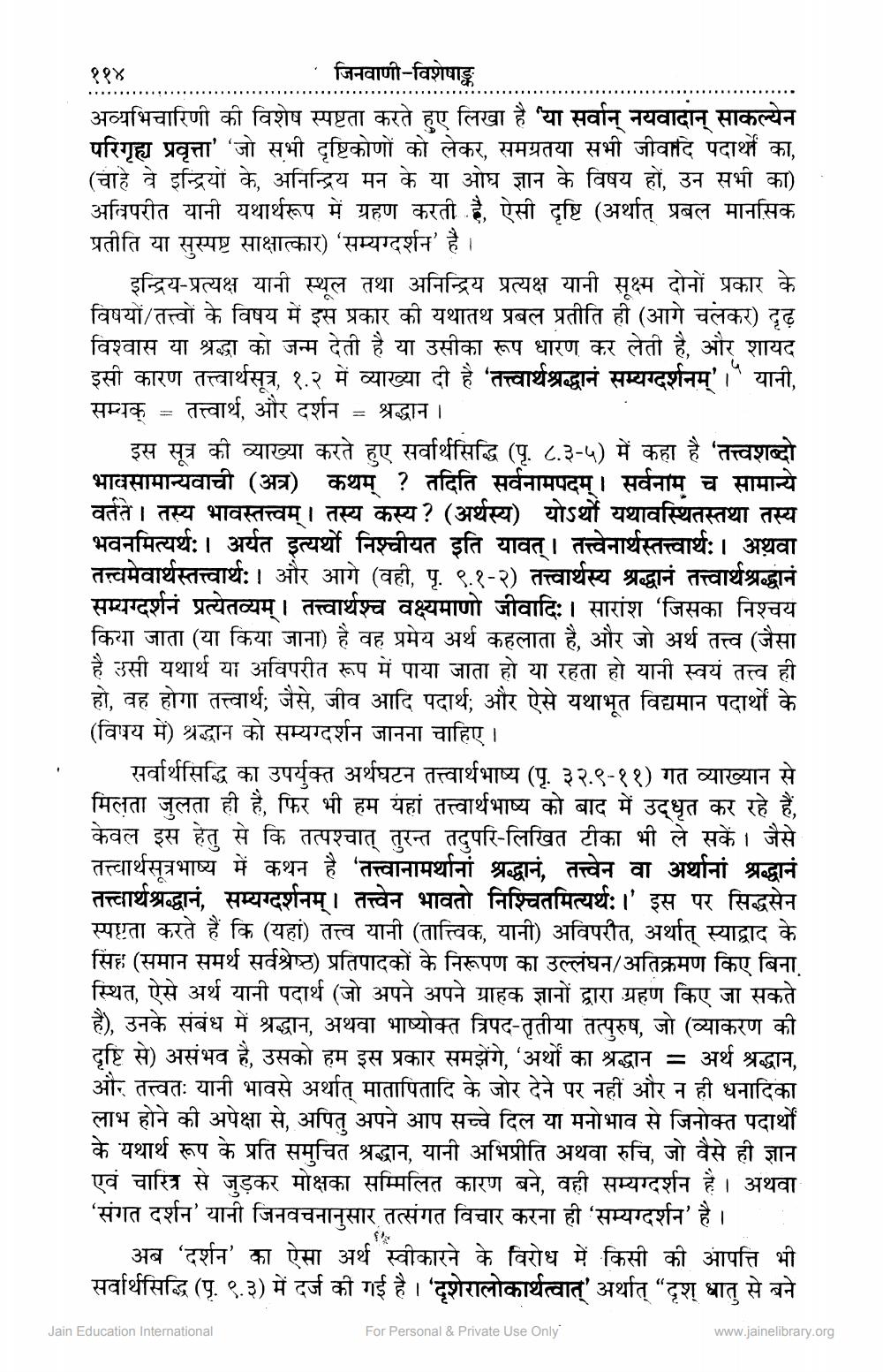________________
११४
• जिनवाणी-विशेषाङ्क अव्यभिचारिणी की विशेष स्पष्टता करते हुए लिखा है "या सर्वान् नयवादान् साकल्येन परिगृह्य प्रवृत्ता' 'जो सभी दृष्टिकोणों को लेकर, समग्रतया सभी जीवादे पदार्थों का, (चाहे वे इन्द्रियों के, अनिन्द्रिय मन के या ओघ ज्ञान के विषय हों, उन सभी का) अविपरीत यानी यथार्थरूप में ग्रहण करती है, ऐसी दृष्टि (अर्थात् प्रबल मानसिक प्रतीति या सुस्पष्ट साक्षात्कार) 'सम्यग्दर्शन' है।
इन्द्रिय-प्रत्यक्ष यानी स्थूल तथा अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष यानी सूक्ष्म दोनों प्रकार के विषयों/तत्त्वों के विषय में इस प्रकार की यथातथ प्रबल प्रतीति ही (आगे चलकर) दृढ़ विश्वास या श्रद्धा को जन्म देती है या उसीका रूप धारण कर लेती है, और शायद इसी कारण तत्त्वार्थसूत्र, १.२ में व्याख्या दी है 'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्'। यानी, सम्यक् = तत्त्वार्थ, और दर्शन = श्रद्धान ।
इस सूत्र की व्याख्या करते हुए सर्वार्थसिद्धि (पृ. ८.३-५) में कहा है 'तत्त्वशब्दो भावसामान्यवाची (अत्र) कथम् ? तदिति सर्वनामपदम्। सर्वनाम च सामान्ये वर्तते। तस्य भावस्तत्त्वम्। तस्य कस्य? (अर्थस्य) योऽर्थो यथावस्थितस्तथा तस्य भवनमित्यर्थः । अर्यत इत्यर्थो निश्चीयत इति यावत्। तत्त्वेनार्थस्तत्त्वार्थः । अथवा तत्त्वमेवार्थस्तत्त्वार्थः। और आगे (वही, पृ. ९.१-२) तत्त्वार्थस्य श्रद्धानं तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं प्रत्येतव्यम् । तत्त्वार्थश्च वक्ष्यमाणो जीवादिः। सारांश ‘जिसका निश्चय किया जाता (या किया जाना) है वह प्रमेय अर्थ कहलाता है, और जो अर्थ तत्त्व (जैसा है उसी यथार्थ या अविपरीत रूप में पाया जाता हो या रहता हो यानी स्वयं तत्त्व ही हो, वह होगा तत्त्वार्थ; जैसे, जीव आदि पदार्थ; और ऐसे यथाभूत विद्यमान पदार्थों के (विषय में) श्रद्धान को सम्यग्दर्शन जानना चाहिए।
सर्वार्थसिद्धि का उपर्युक्त अर्थघटन तत्त्वार्थभाष्य (पृ. ३२.९-११) गत व्याख्यान से मिलता जुलता ही है, फिर भी हम यहां तत्त्वार्थभाष्य को बाद में उद्धृत कर रहे हैं, केवल इस हेतु से कि तत्पश्चात् तुरन्त तदुपरि-लिखित टीका भी ले सकें। जैसे तत्त्वार्थसूत्रभाष्य में कथन है 'तत्त्वानामर्थानां श्रद्धानं, तत्त्वेन वा अर्थानां श्रद्धानं तत्त्वार्थश्रद्धानं, सम्यग्दर्शनम्। तत्त्वेन भावतो निश्चितमित्यर्थः।' इस पर सिद्धसेन स्पष्टता करते हैं कि (यहां) तत्त्व यानी (तात्त्विक, यानी) अविपरीत, अर्थात् स्याद्वाद के सिंह (समान समर्थ सर्वश्रेष्ठ) प्रतिपादकों के निरूपण का उल्लंघन/अतिक्रमण किए बिना स्थित, ऐसे अर्थ यानी पदार्थ (जो अपने अपने ग्राहक ज्ञानों द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं), उनके संबंध में श्रद्धान, अथवा भाष्योक्त त्रिपद-तृतीया तत्पुरुष, जो (व्याकरण की दृष्टि से) असंभव है, उसको हम इस प्रकार समझेंगे, ‘अर्थों का श्रद्धान = अर्थ श्रद्धान, और तत्त्वतः यानी भावसे अर्थात् मातापितादि के जोर देने पर नहीं और न ही धनादिका लाभ होने की अपेक्षा से, अपितु अपने आप सच्चे दिल या मनोभाव से जिनोक्त पदार्थों के यथार्थ रूप के प्रति समुचित श्रद्धान, यानी अभिप्रीति अथवा रुचि, जो वैसे ही ज्ञान एवं चारित्र से जुड़कर मोक्षका सम्मिलित कारण बने, वही सम्यग्दर्शन है। अथवा 'संगत दर्शन' यानी जिनवचनानुसार तत्संगत विचार करना ही ‘सम्यग्दर्शन' है।
अब 'दर्शन' का ऐसा अर्थ स्वीकारने के विरोध में किसी की आपत्ति भी सर्वार्थसिद्धि (पृ. ९.३) में दर्ज की गई है । 'दृशेरालोकार्थत्वात्' अर्थात् “दृश् धातु से बने
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org