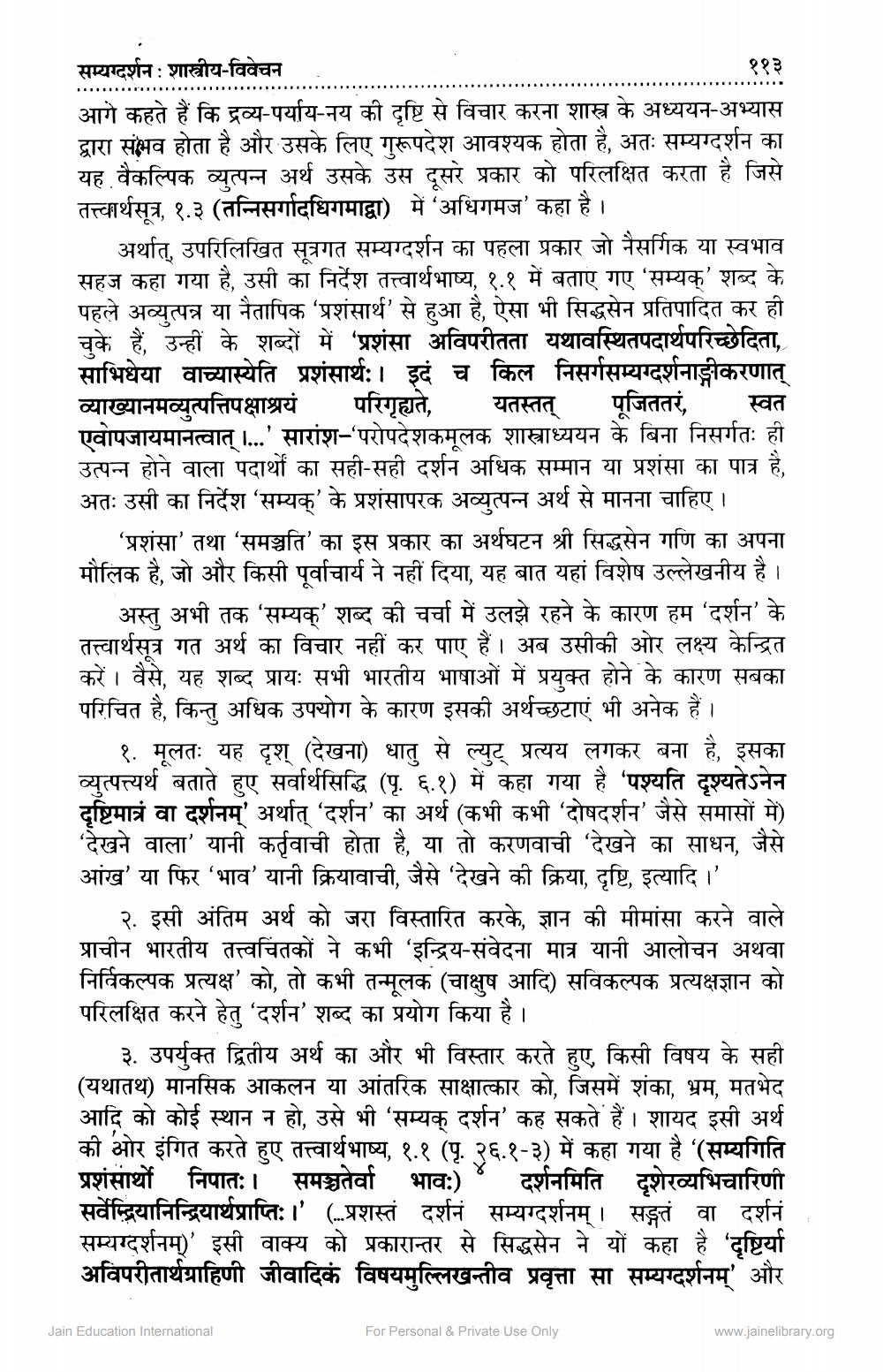________________
सम्यग्दर्शन : शास्त्रीय-विवेचन
११३ आगे कहते हैं कि द्रव्य-पर्याय-नय की दृष्टि से विचार करना शास्त्र के अध्ययन-अभ्यास द्वारा संभव होता है और उसके लिए गुरूपदेश आवश्यक होता है, अतः सम्यग्दर्शन का यह वैकल्पिक व्युत्पन्न अर्थ उसके उस दूसरे प्रकार को परिलक्षित करता है जिसे तत्त्वार्थसूत्र, १.३ (तन्निसर्गादधिगमाद्वा) में 'अधिगमज' कहा है। __ अर्थात्, उपरिलिखित सूत्रगत सम्यग्दर्शन का पहला प्रकार जो नैसर्गिक या स्वभाव सहज कहा गया है, उसी का निर्देश तत्त्वार्थभाष्य, १.१ में बताए गए 'सम्यक्' शब्द के पहले अव्युत्पन्न या नैतापिक 'प्रशंसार्थ' से हुआ है, ऐसा भी सिद्धसेन प्रतिपादित कर ही चुके हैं, उन्हीं के शब्दों में 'प्रशंसा अविपरीतता यथावस्थितपदार्थपरिच्छेदिता, साभिधेया वाच्यास्येति प्रशंसार्थः। इदं च किल निसर्गसम्यग्दर्शनाङ्गीकरणात् व्याख्यानमव्युत्पत्तिपक्षाश्रयं परिगृह्यते, यतस्तत् पूजिततरं, स्वत एवोपजायमानत्वात्।...' सारांश-'परोपदेशकमूलक शास्त्राध्ययन के बिना निसर्गतः ही उत्पन्न होने वाला पदार्थों का सही-सही दर्शन अधिक सम्मान या प्रशंसा का पात्र है, अतः उसी का निर्देश 'सम्यक्' के प्रशंसापरक अव्युत्पन्न अर्थ से मानना चाहिए।
‘प्रशंसा' तथा 'समञ्चति' का इस प्रकार का अर्थघटन श्री सिद्धसेन गणि का अपना मौलिक है, जो और किसी पूर्वाचार्य ने नहीं दिया, यह बात यहां विशेष उल्लेखनीय है ।
अस्तु अभी तक 'सम्यक्' शब्द की चर्चा में उलझे रहने के कारण हम 'दर्शन' के तत्त्वार्थसूत्र गत अर्थ का विचार नहीं कर पाए हैं। अब उसीकी ओर लक्ष्य केन्द्रित करें। वैसे, यह शब्द प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त होने के कारण सबका परिचित है, किन्तु अधिक उपयोग के कारण इसकी अर्थच्छटाएं भी अनेक हैं।
१. मूलतः यह दृश् (देखना) धातु से ल्युट प्रत्यय लगकर बना है, इसका व्युत्पत्त्यर्थ बताते हुए सर्वार्थसिद्धि (पृ. ६.१) में कहा गया है ‘पश्यति दृश्यतेऽनेन दृष्टिमात्रं वा दर्शनम्' अर्थात् 'दर्शन' का अर्थ (कभी कभी 'दोषदर्शन' जैसे समासों में) 'देखने वाला' यानी कर्तृवाची होता है, या तो करणवाची ‘देखने का साधन, जैसे आंख' या फिर 'भाव' यानी क्रियावाची, जैसे देखने की क्रिया, दृष्टि, इत्यादि ।'
२. इसी अंतिम अर्थ को जरा विस्तारित करके, ज्ञान की मीमांसा करने वाले प्राचीन भारतीय तत्त्वचिंतकों ने कभी 'इन्द्रिय-संवेदना मात्र यानी आलोचन अथवा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष' को, तो कभी तन्मूलक (चाक्षुष आदि) सविकल्पक प्रत्यक्षज्ञान को परिलक्षित करने हेतु 'दर्शन' शब्द का प्रयोग किया है।
३. उपर्युक्त द्वितीय अर्थ का और भी विस्तार करते हुए, किसी विषय के सही (यथातथ) मानसिक आकलन या आंतरिक साक्षात्कार को, जिसमें शंका, भ्रम, मतभेद आदि को कोई स्थान न हो, उसे भी ‘सम्यक् दर्शन' कह सकते हैं। शायद इसी अर्थ की ओर इंगित करते हुए तत्त्वार्थभाष्य, १.१ (पृ. २६.१-३) में कहा गया है ‘(सम्यगिति प्रशंसार्थो निपातः। समञ्चतेर्वा भाव:) दर्शनमिति दृशेरव्यभिचारिणी सर्वेन्द्रियानिन्द्रियार्थप्राप्तिः।' (...प्रशस्तं दर्शनं सम्यग्दर्शनम्। सङ्गतं वा दर्शनं सम्यग्दर्शनम्)' इसी वाक्य को प्रकारान्तर से सिद्धसेन ने यों कहा है 'दृष्टिर्या अविपरीतार्थग्राहिणी जीवादिकं विषयमुल्लिखन्तीव प्रवृत्ता सा सम्यग्दर्शनम्' और
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org