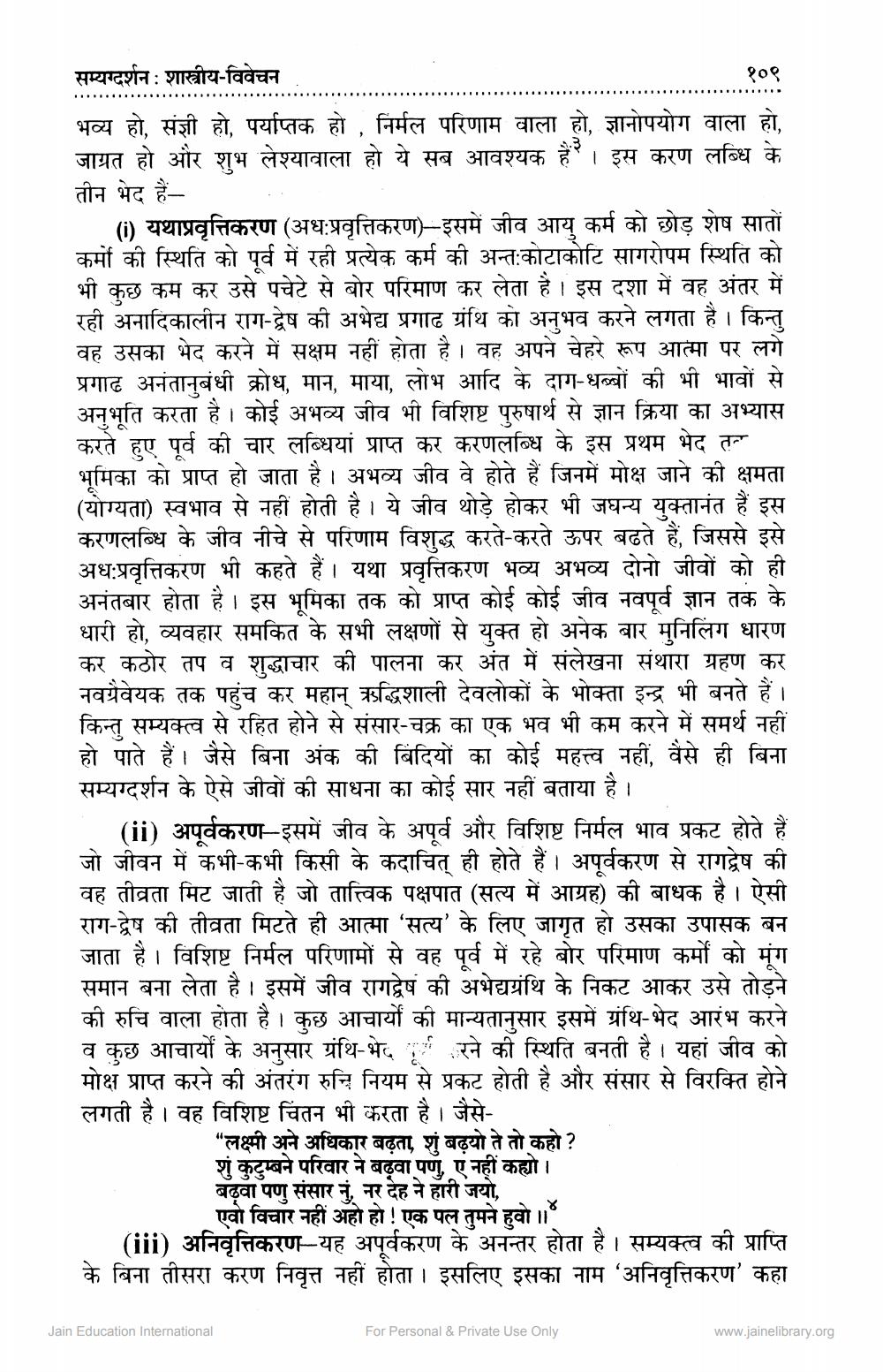________________
.............१०९
सम्यग्दर्शन : शास्त्रीय-विवेचन भव्य हो, संज्ञी हो, पर्याप्तक हो , निर्मल परिणाम वाला हो, ज्ञानोपयोग वाला हो, जाग्रत हो और शुभ लेश्यावाला हो ये सब आवश्यक हैं । इस करण लब्धि के तीन भेद हैं
(i) यथाप्रवृत्तिकरण (अध:प्रवृत्तिकरण)-इसमें जीव आय कर्म को छोड़ शेष सातों कर्मो की स्थिति को पूर्व में रही प्रत्येक कर्म की अन्त:कोटाकोटि सागरोपम स्थिति को भी कुछ कम कर उसे पचेटे से बोर परिमाण कर लेता है। इस दशा में वह अंतर में रही अनादिकालीन राग-द्वेष की अभेद्य प्रगाढ ग्रंथि को अनुभव करने लगता है। किन्तु वह उसका भेद करने में सक्षम नहीं होता है। वह अपने चेहरे रूप आत्मा पर लगे प्रगाढ अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के दाग-धब्बों की भी भावों से अनुभूति करता है। कोई अभव्य जीव भी विशिष्ट पुरुषार्थ से ज्ञान क्रिया का अभ्यास करते हुए पूर्व की चार लब्धियां प्राप्त कर करणलब्धि के इस प्रथम भेद तर भूमिका को प्राप्त हो जाता है। अभव्य जीव वे होते हैं जिनमें मोक्ष जाने की क्षमता (योग्यता) स्वभाव से नहीं होती है। ये जीव थोड़े होकर भी जघन्य युक्तानंत हैं इस करणलब्धि के जीव नीचे से परिणाम विशुद्ध करते-करते ऊपर बढते हैं, जिससे इसे अध:प्रवृत्तिकरण भी कहते हैं। यथा प्रवृत्तिकरण भव्य अभव्य दोनो जीवों को ही अनंतबार होता है। इस भूमिका तक को प्राप्त कोई कोई जीव नवपूर्व ज्ञान तक के धारी हो, व्यवहार समकित के सभी लक्षणों से युक्त हो अनेक बार मुनिलिंग धारण कर कठोर तप व शुद्धाचार की पालना कर अंत में संलेखना संथारा ग्रहण कर नवग्रैवेयक तक पहुंच कर महान् ऋद्धिशाली देवलोकों के भोक्ता इन्द्र भी बनते हैं। किन्तु सम्यक्त्व से रहित होने से संसार-चक्र का एक भव भी कम करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। जैसे बिना अंक की बिंदियों का कोई महत्त्व नहीं, वैसे ही बिना सम्यग्दर्शन के ऐसे जीवों की साधना का कोई सार नहीं बताया है।
(ii) अपूर्वकरण इसमें जीव के अपूर्व और विशिष्ट निर्मल भाव प्रकट होते हैं जो जीवन में कभी-कभी किसी के कदाचित् ही होते हैं। अपूर्वकरण से रागद्वेष की वह तीव्रता मिट जाती है जो तात्त्विक पक्षपात (सत्य में आग्रह) की बाधक है। ऐसी राग-द्वेष की तीव्रता मिटते ही आत्मा 'सत्य' के लिए जागृत हो उसका उपासक बन जाता है। विशिष्ट निर्मल परिणामों से वह पूर्व में रहे बोर परिमाण कर्मों को मूंग समान बना लेता है। इसमें जीव रागद्वेष की अभेद्यग्रंथि के निकट आकर उसे तोड़ने की रुचि वाला होता है। कुछ आचार्यों की मान्यतानुसार इसमें ग्रंथि-भेद आरंभ करने व कुछ आचार्यों के अनुसार ग्रंथि-भेद से रने की स्थिति बनती है। यहां जीव को मोक्ष प्राप्त करने की अंतरंग रुचि नियम से प्रकट होती है और संसार से विरक्ति होने लगती है। वह विशिष्ट चिंतन भी करता है। जैसे
"लक्ष्मी अने अधिकार बढ़ता, शुं बढ़यो ते तो कहो? शुं कुटुम्बने परिवार ने बढ़वा पणु, ए नहीं कह्यो। बढ़वा पणु संसार नु, नर देह ने हारी जयो,
एवो विचार नहीं अहो हो ! एक पल तुमने हुवो ॥ (iii) अनिवृत्तिकरण यह अपूर्वकरण के अनन्तर होता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना तीसरा करण निवृत्त नहीं होता। इसलिए इसका नाम ‘अनिवृत्तिकरण' कहा
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org