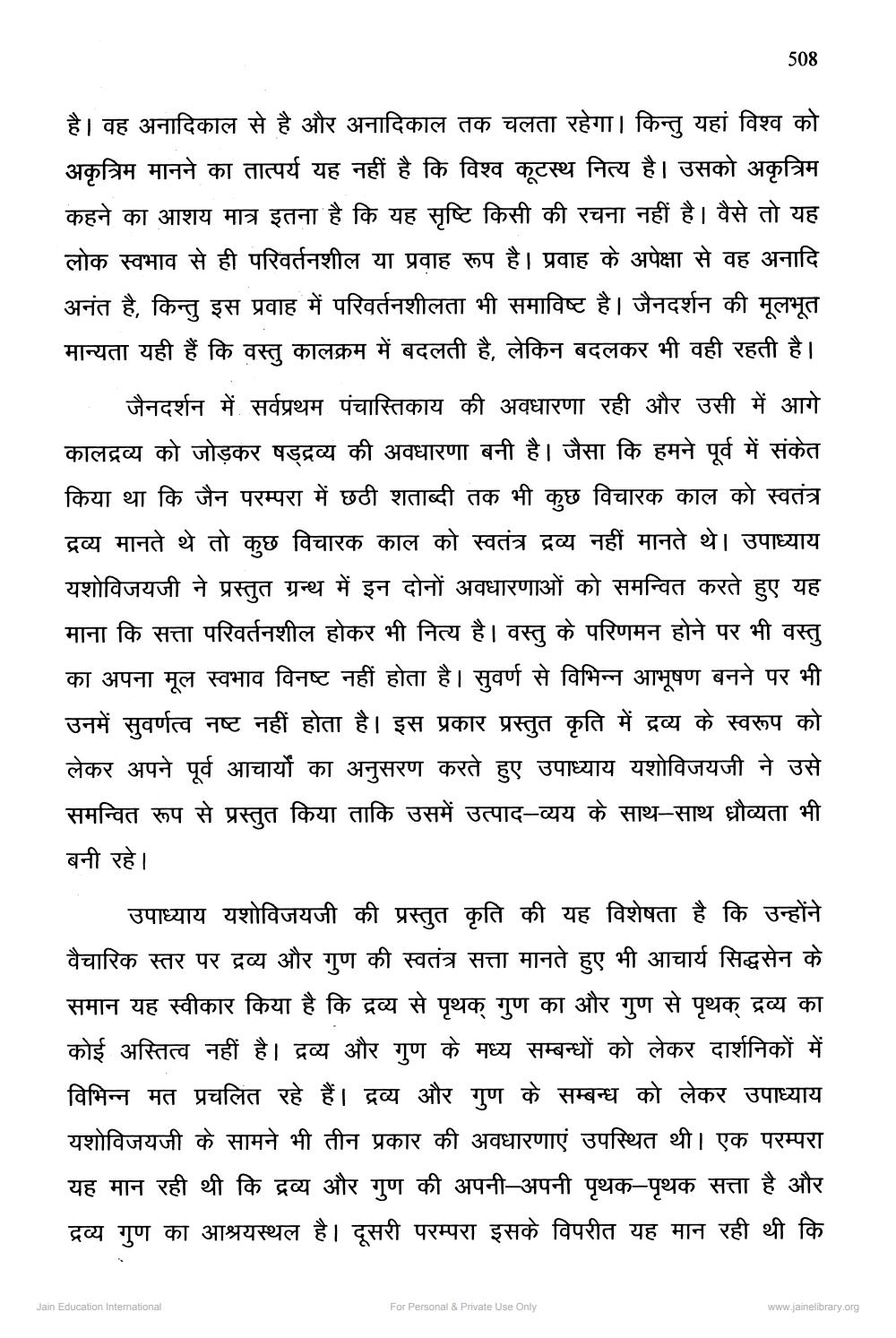________________
508
है। वह अनादिकाल से है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। किन्तु यहां विश्व को अकृत्रिम मानने का तात्पर्य यह नहीं है कि विश्व कूटस्थ नित्य है। उसको अकृत्रिम कहने का आशय मात्र इतना है कि यह सृष्टि किसी की रचना नहीं है। वैसे तो यह लोक स्वभाव से ही परिवर्तनशील या प्रवाह रूप है। प्रवाह के अपेक्षा से वह अनादि अनंत है, किन्तु इस प्रवाह में परिवर्तनशीलता भी समाविष्ट है। जैनदर्शन की मूलभूत मान्यता यही हैं कि वस्तु कालक्रम में बदलती है, लेकिन बदलकर भी वही रहती है।
जैनदर्शन में सर्वप्रथम पंचास्तिकाय की अवधारणा रही और उसी में आगे कालद्रव्य को जोड़कर षड्द्रव्य की अवधारणा बनी है। जैसा कि हमने पूर्व में संकेत किया था कि जैन परम्परा में छठी शताब्दी तक भी कुछ विचारक काल को स्वतंत्र द्रव्य मानते थे तो कुछ विचारक काल को स्वतंत्र द्रव्य नहीं मानते थे। उपाध्याय यशोविजयजी ने प्रस्तुत ग्रन्थ में इन दोनों अवधारणाओं को समन्वित करते हुए यह माना कि सत्ता परिवर्तनशील होकर भी नित्य है। वस्तु के परिणमन होने पर भी वस्तु का अपना मूल स्वभाव विनष्ट नहीं होता है। सुवर्ण से विभिन्न आभूषण बनने पर भी उनमें सुवर्णत्व नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार प्रस्तुत कृति में द्रव्य के स्वरूप को लेकर अपने पूर्व आचार्यों का अनुसरण करते हुए उपाध्याय यशोविजयजी ने उसे समन्वित रूप से प्रस्तुत किया ताकि उसमें उत्पाद–व्यय के साथ-साथ ध्रौव्यता भी बनी रहे।
उपाध्याय यशोविजयजी की प्रस्तुत कृति की यह विशेषता है कि उन्होंने वैचारिक स्तर पर द्रव्य और गुण की स्वतंत्र सत्ता मानते हुए भी आचार्य सिद्धसेन के समान यह स्वीकार किया है कि द्रव्य से पृथक् गुण का और गुण से पृथक् द्रव्य का कोई अस्तित्व नहीं है। द्रव्य और गुण के मध्य सम्बन्धों को लेकर दार्शनिकों में विभिन्न मत प्रचलित रहे हैं। द्रव्य और गुण के सम्बन्ध को लेकर उपाध्याय यशोविजयजी के सामने भी तीन प्रकार की अवधारणाएं उपस्थित थी। एक परम्परा यह मान रही थी कि द्रव्य और गुण की अपनी-अपनी पृथक-पृथक सत्ता है और द्रव्य गुण का आश्रयस्थल है। दूसरी परम्परा इसके विपरीत यह मान रही थी कि
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org