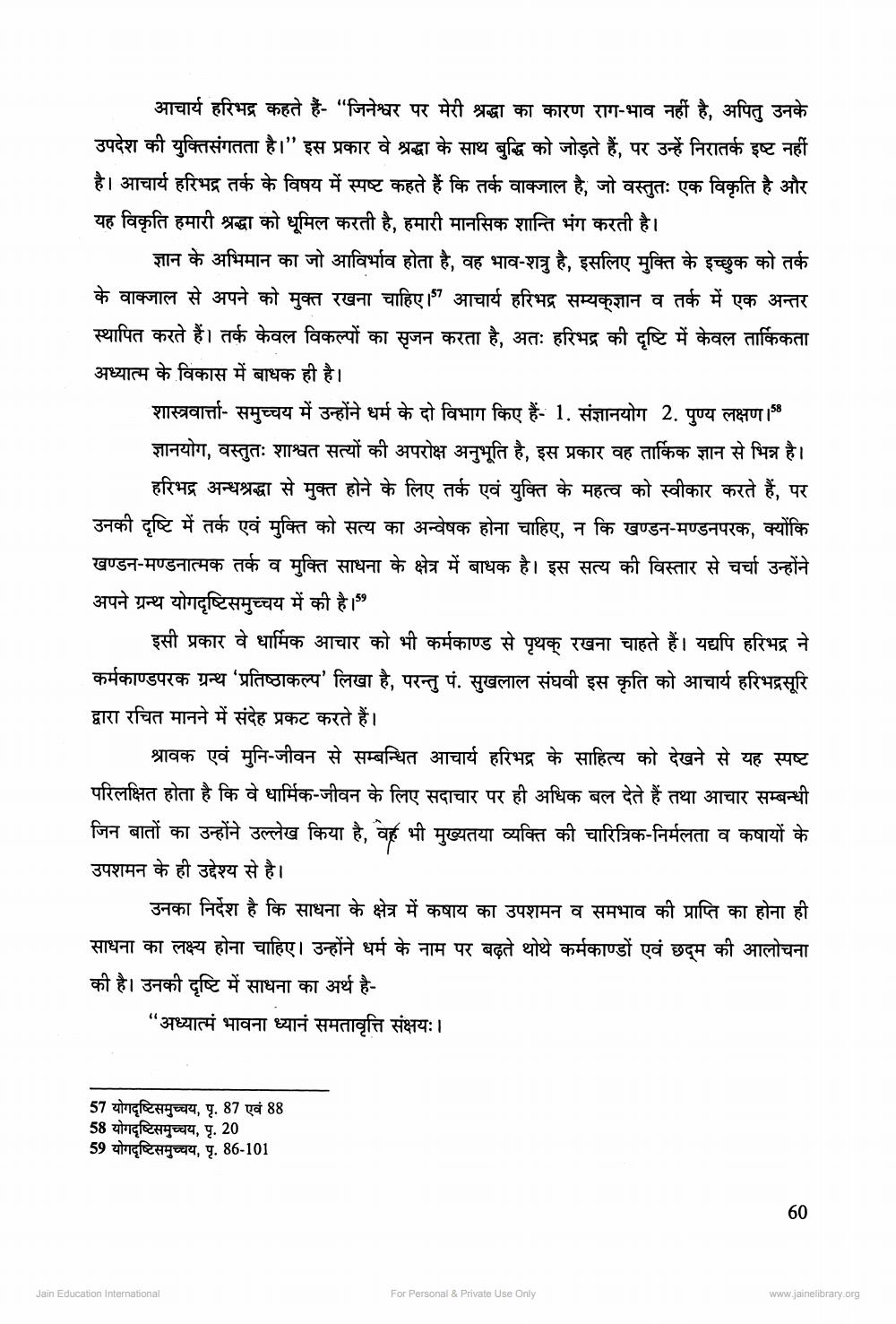________________
आचार्य हरिभद्र कहते हैं- "जिनेश्वर पर मेरी श्रद्धा का कारण राग-भाव नहीं है, अपितु उनके उपदेश की युक्तिसंगतता है।" इस प्रकार वे श्रद्धा के साथ बुद्धि को जोड़ते हैं, पर उन्हें निरातर्क इष्ट नहीं है। आचार्य हरिभद्र तर्क के विषय में स्पष्ट कहते हैं कि तर्क वाक्जाल है, जो वस्तुतः एक विकृति है और यह विकृति हमारी श्रद्धा को धूमिल करती है, हमारी मानसिक शान्ति भंग करती है।
ज्ञान के अभिमान का जो आविर्भाव होता है, वह भाव- शत्रु है, इसलिए मुक्ति के इच्छुक को तर्क के वाक्जाल से अपने को मुक्त रखना चाहिए। 57 आचार्य हरिभद्र सम्यक्ज्ञान व तर्क में एक अन्तर स्थापित करते हैं। तर्क केवल विकल्पों का सृजन करता है, अतः हरिभद्र की दृष्टि में केवल तार्किकता अध्यात्म के विकास में बाधक ही है।
शास्त्रवार्त्ता- समुच्चय में उन्होंने धर्म के दो विभाग किए हैं- 1. संज्ञानयोग 2. पुण्य लक्षण | 58 ज्ञानयोग, वस्तुतः शाश्वत सत्यों की अपरोक्ष अनुभूति है, इस प्रकार वह तार्किक ज्ञान से भिन्न है। हरिभद्र अन्धश्रद्धा से मुक्त होने के लिए तर्क एवं युक्ति के महत्व को स्वीकार करते हैं, पर उनकी दृष्टि में तर्क एवं मुक्ति को सत्य का अन्वेषक होना चाहिए, न कि खण्डन- मण्डनपरक, क्योंकि खण्डन-मण्डनात्मक तर्क व मुक्ति साधना के क्षेत्र में बाधक है। इस सत्य की विस्तार से चर्चा उन्होंने अपने ग्रन्थ योगदृष्टिसमुच्चय में की है। 59
इसी प्रकार वे धार्मिक आचार को भी कर्मकाण्ड से पृथक् रखना चाहते हैं । यद्यपि हरिभद्र ने कर्मकाण्डपरक ग्रन्थ 'प्रतिष्ठाकल्प' लिखा है, परन्तु पं. सुखलाल संघवी इस कृति को आचार्य हरिभद्रसूरि द्वारा रचित मानने में संदेह प्रकट करते हैं ।
श्रावक एवं मुनि-जीवन से सम्बन्धित आचार्य हरिभद्र के साहित्य को देखने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वे धार्मिक जीवन के लिए सदाचार पर ही अधिक बल देते हैं तथा आचार सम्बन्धी जिन बातों का उन्होंने उल्लेख किया है, वह भी मुख्यतया व्यक्ति की चारित्रिक निर्मलता व कषायों उपशमन के ही उद्देश्य से है ।
उनका निर्देश है कि साधना के क्षेत्र में कषाय का उपशमन व समभाव की प्राप्ति का होना ही साधना का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने धर्म के नाम पर बढ़ते थोथे कर्मकाण्डों एवं छद्म की आलोचना की है। उनकी दृष्टि में साधना का अर्थ है
" अध्यात्मं भावना ध्यानं समतावृत्ति संक्षयः ।
57 योगदृष्टिसमुच्चय, पृ. 87 एवं 88
58 योगदृष्टिसमुच्चय, पृ. 20
59 योगदृष्टिसमुच्चय, पृ. 86-101
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
60
www.jainelibrary.org