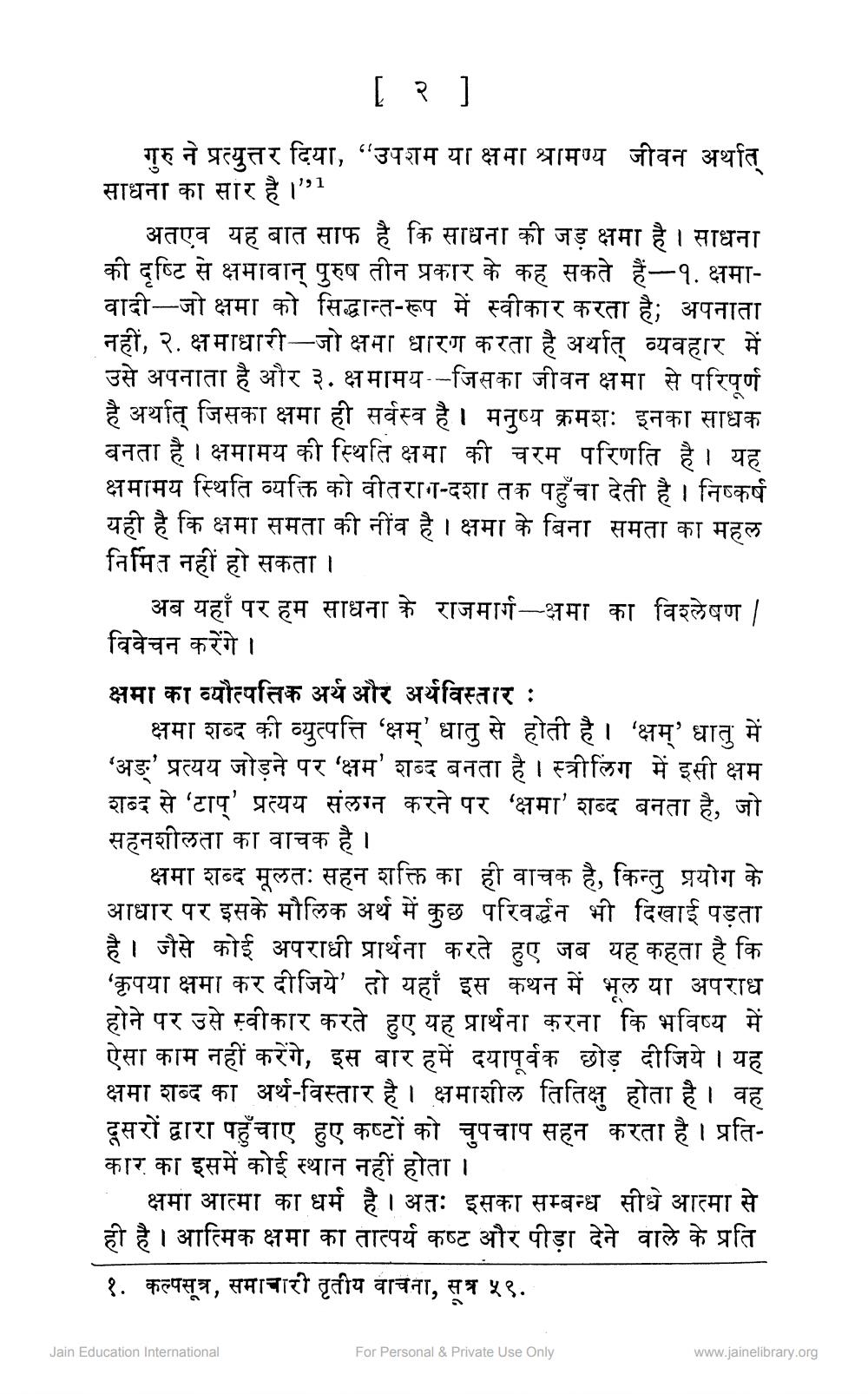________________
[
२ ]
गरु ने प्रत्युत्तर दिया, "उपशम या क्षमा श्रामण्य जीवन अर्थात साधना का सार है।"1
अतएव यह बात साफ है कि साधना की जड़ क्षमा है। साधना की दष्टि से क्षमावान् पुरुष तीन प्रकार के कह सकते हैं-१. क्षमावादी-जो क्षमा को सिद्धान्त-रूप में स्वीकार करता है; अपनाता नहीं, २. क्षमाधारी—जो क्षमा धारण करता है अर्थात् व्यवहार में उसे अपनाता है और ३. क्षमामय -जिसका जीवन क्षमा से परिपूर्ण है अर्थात् जिसका क्षमा ही सर्वस्व है। मनुष्य क्रमश: इनका साधक बनता है । क्षमामय की स्थिति क्षमा की चरम परिणति है। यह क्षमामय स्थिति व्यक्ति को वीतराग-दशा तक पहुँचा देती है। निष्कर्ष यही है कि क्षमा समता की नींव है । क्षमा के बिना समता का महल निर्मित नहीं हो सकता। ___ अब यहाँ पर हम साधना के राजमार्ग क्षमा का विश्लेषण | विवेचन करेंगे। क्षमा का व्यौत्पत्तिक अर्थ और अर्थविस्तार :
क्षमा शब्द की व्युत्पत्ति 'क्षम्' धातु से होती है। 'क्षम्' धातु में 'अ' प्रत्यय जोड़ने पर 'क्षम' शब्द बनता है । स्त्रीलिंग में इसी क्षम शब्द से 'टाप्' प्रत्यय संलग्न करने पर 'क्षमा' शब्द बनता है, जो सहनशीलता का वाचक है ।
क्षमा शब्द मूलतः सहन शक्ति का ही वाचक है, किन्तु प्रयोग के आधार पर इसके मौलिक अर्थ में कुछ परिवर्द्धन भी दिखाई पड़ता है। जैसे कोई अपराधी प्रार्थना करते हुए जब यह कहता है कि 'कृपया क्षमा कर दीजिये' तो यहाँ इस कथन में भूल या अपराध होने पर उसे स्वीकार करते हुए यह प्रार्थना करना कि भविष्य में ऐसा काम नहीं करेंगे, इस बार हमें दयापूर्वक छोड़ दीजिये । यह क्षमा शब्द का अर्थ-विस्तार है। क्षमाशील तितिक्षु होता है। वह दूसरों द्वारा पहुँचाए हुए कष्टों को चुपचाप सहन करता है। प्रतिकार का इसमें कोई स्थान नहीं होता। - क्षमा आत्मा का धर्म है। अतः इसका सम्बन्ध सीधे आत्मा से ही है । आत्मिक क्षमा का तात्पर्य कष्ट और पीड़ा देने वाले के प्रति १. कल्पसूत्र, समाचारी तृतीय वाचना, सत्र ५९.
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org