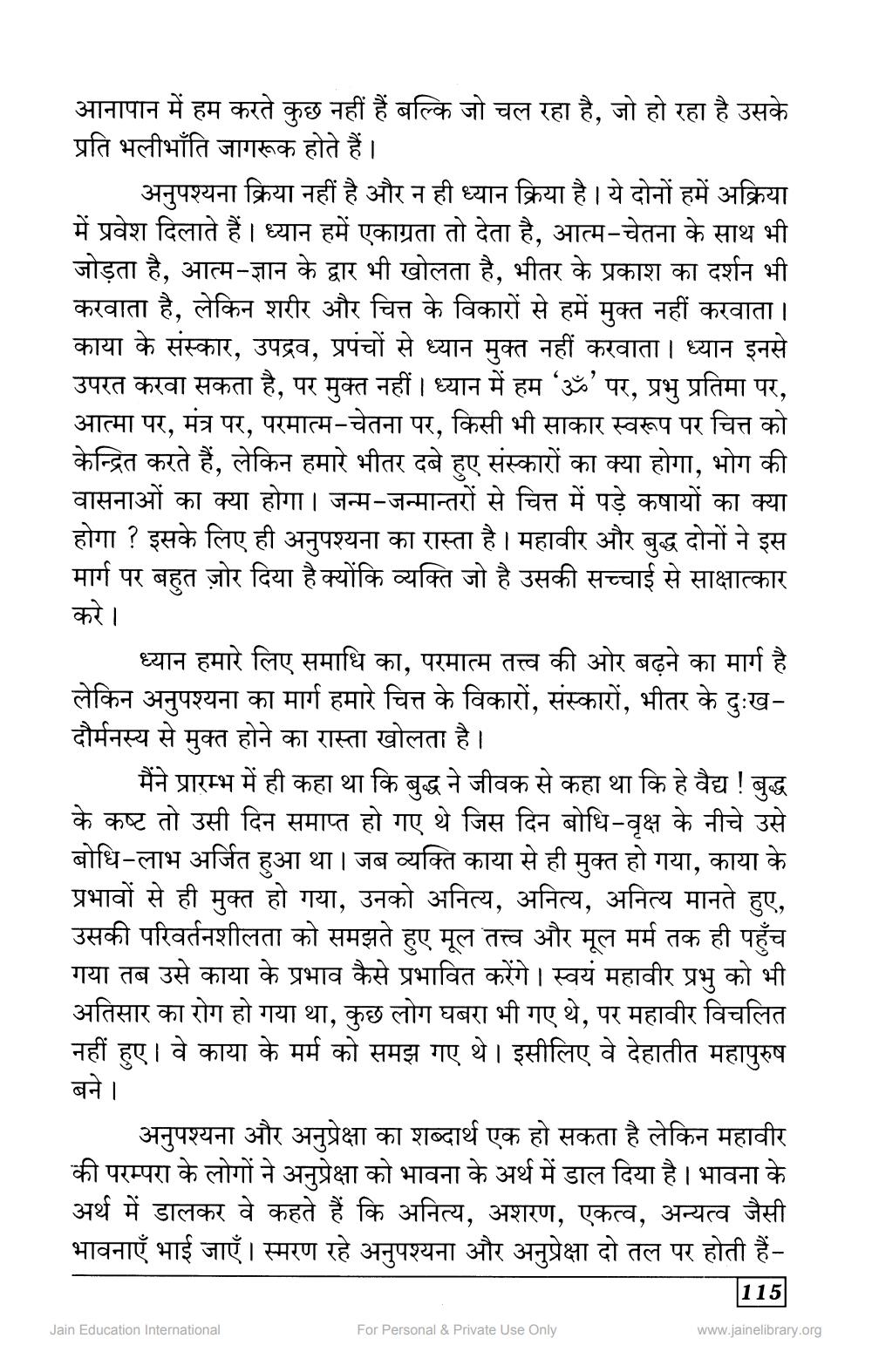________________
आनापान में हम करते कुछ नहीं हैं बल्कि जो चल रहा है, जो हो रहा है उसके प्रति भलीभाँति जागरूक होते हैं।
अनुपश्यना क्रिया नहीं है और न ही ध्यान क्रिया है। ये दोनों हमें अक्रिया में प्रवेश दिलाते हैं। ध्यान हमें एकाग्रता तो देता है, आत्म-चेतना के साथ भी जोड़ता है, आत्म-ज्ञान के द्वार भी खोलता है, भीतर के प्रकाश का दर्शन भी करवाता है, लेकिन शरीर और चित्त के विकारों से हमें मुक्त नहीं करवाता। काया के संस्कार, उपद्रव, प्रपंचों से ध्यान मुक्त नहीं करवाता। ध्यान इनसे उपरत करवा सकता है, पर मुक्त नहीं। ध्यान में हम 'ॐ' पर, प्रभु प्रतिमा पर, आत्मा पर, मंत्र पर, परमात्म-चेतना पर, किसी भी साकार स्वरूप पर चित्त को केन्द्रित करते हैं, लेकिन हमारे भीतर दबे हुए संस्कारों का क्या होगा, भोग की वासनाओं का क्या होगा। जन्म-जन्मान्तरों से चित्त में पड़े कषायों का क्या होगा ? इसके लिए ही अनुपश्यना का रास्ता है। महावीर और बुद्ध दोनों ने इस मार्ग पर बहुत ज़ोर दिया है क्योंकि व्यक्ति जो है उसकी सच्चाई से साक्षात्कार करे।
ध्यान हमारे लिए समाधि का, परमात्म तत्त्व की ओर बढ़ने का मार्ग है लेकिन अनुपश्यना का मार्ग हमारे चित्त के विकारों, संस्कारों, भीतर के दुःखदौर्मनस्य से मुक्त होने का रास्ता खोलता है।
मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि बुद्ध ने जीवक से कहा था कि हे वैद्य ! बुद्ध के कष्ट तो उसी दिन समाप्त हो गए थे जिस दिन बोधि-वृक्ष के नीचे उसे बोधि-लाभ अर्जित हुआ था। जब व्यक्ति काया से ही मुक्त हो गया, काया के प्रभावों से ही मुक्त हो गया, उनको अनित्य, अनित्य, अनित्य मानते हुए, उसकी परिवर्तनशीलता को समझते हुए मूल तत्त्व और मूल मर्म तक ही पहुँच गया तब उसे काया के प्रभाव कैसे प्रभावित करेंगे। स्वयं महावीर प्रभु को भी अतिसार का रोग हो गया था, कुछ लोग घबरा भी गए थे, पर महावीर विचलित नहीं हुए। वे काया के मर्म को समझ गए थे। इसीलिए वे देहातीत महापुरुष बने।
अनुपश्यना और अनुप्रेक्षा का शब्दार्थ एक हो सकता है लेकिन महावीर की परम्परा के लोगों ने अनुप्रेक्षा को भावना के अर्थ में डाल दिया है। भावना के अर्थ में डालकर वे कहते हैं कि अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व जैसी भावनाएँ भाई जाएँ। स्मरण रहे अनुपश्यना और अनुप्रेक्षा दो तल पर होती हैं
[115
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org