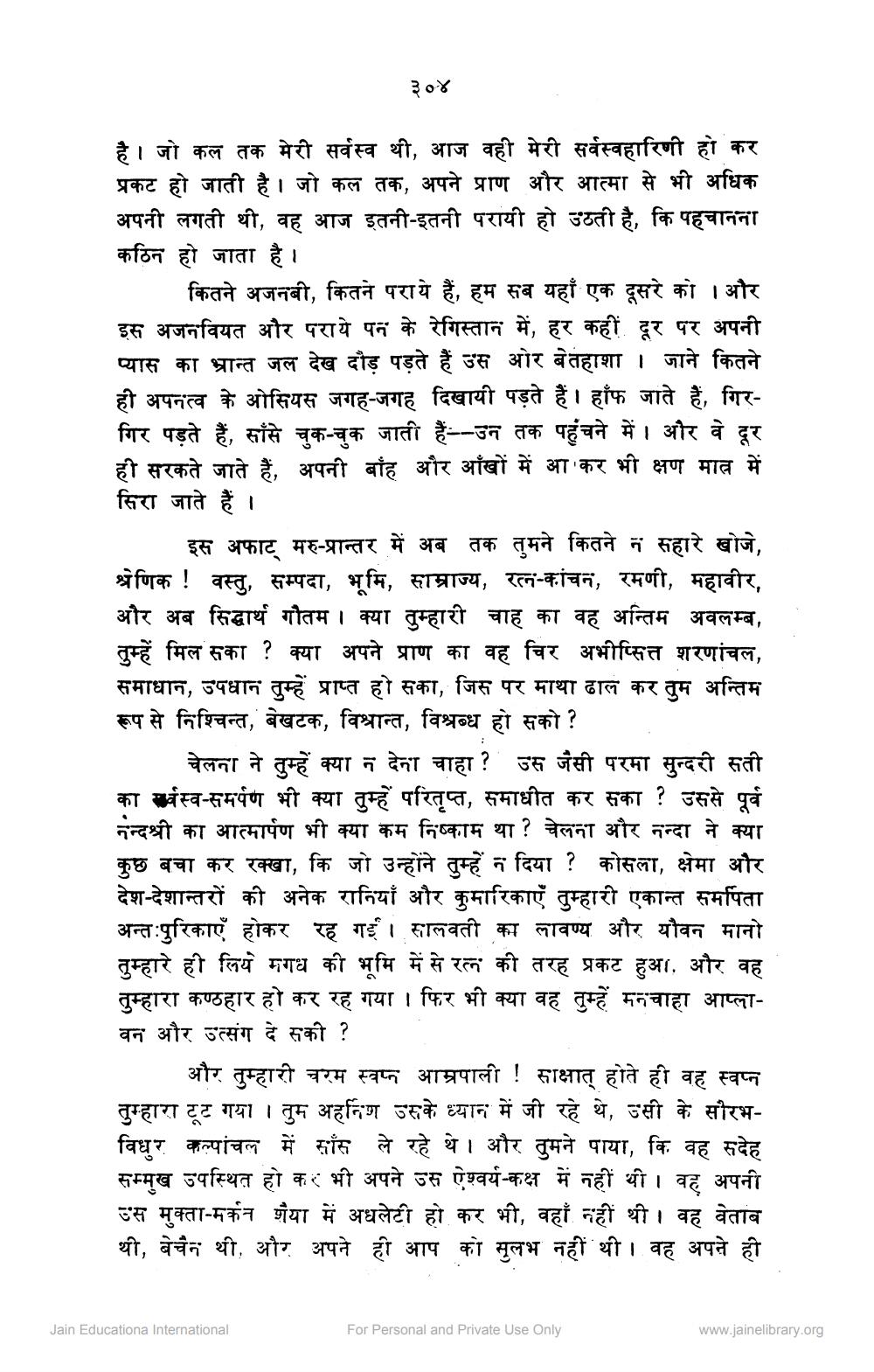________________
३०४
है । जो कल तक मेरी सर्वस्व थी, आज वही मेरी सर्वस्वहारिणी हो कर प्रकट हो जाती है। जो कल तक, अपने प्राण और आत्मा से भी अधिक अपनी लगती थी, वह आज इतनी इतनी परायी हो उठती है, कि पहचानना कठिन हो जाता है ।
कितने अजनबी, कितने पराये हैं, हम सब यहाँ एक दूसरे को । और इस अजनवियत और पराये पन के रेगिस्तान में, हर कहीं दूर पर अपनी प्यास का भ्रान्त जल देख दौड़ पड़ते हैं उस ओर बेतहाशा । जाने कितने ही अपनत्व के ओसियस जगह-जगह दिखायी पड़ते हैं । हाँफ जाते हैं, गिरगिर पड़ते हैं, साँसे चुकचुक जाती हैं-- उन तक पहुंचने में और वे दूर ही सरकते जाते हैं, अपनी बाँह और आँखों में आ कर भी क्षण मात्र में सिरा जाते हैं ।
1
इस अफाट मरु- प्रान्तर में अब तक तुमने कितने न सहारे खोजे, श्रेणिक ! वस्तु, सम्पदा, भूमि, साम्राज्य, रत्न-कांचन, रमणी, महावीर, और अब सिद्धार्थ गौतम । क्या तुम्हारी चाह का वह अन्तिम अवलम्ब, तुम्हें मिल सका ? क्या अपने प्राण का वह चिर अभीप्सित्त शरणांचल, समाधान, उपधान तुम्हें प्राप्त हो सका, जिस पर माथा ढाल कर तुम अन्तिम रूप से निश्चिन्त, बेखटक, विश्रान्त, विश्रब्ध हो सको ?
चेलना ने तुम्हें क्या न देना चाहा ? उस जैसी परमा सुन्दरी सती का सर्वस्व समर्पण भी क्या तुम्हें परितृप्त, समाधीत कर सका ? उससे पूर्व नन्दश्री का आत्मार्पण भी क्या कम निष्काम था ? चेलना और नन्दा ने क्या कुछ बचा कर रक्खा, कि जो उन्होंने तुम्हें न दिया ? कोसला, क्षेमा और देश-देशान्तरों की अनेक रानियाँ और कुमारिकाएँ तुम्हारी एकान्त समर्पिता अन्तःपुरिकाएँ होकर रह गईं । सालवती का लावण्य और यौवन मानो तुम्हारे ही लिये मगध की भूमि में से रत्न की तरह प्रकट हुआ और वह तुम्हारा कण्ठहार हो कर रह गया । फिर भी क्या वह तुम्हें मनचाहा आपलावन और उत्संग दे सकी ?
और तुम्हारी चरम स्वप्न आम्रपाली ! साक्षात् होते ही वह स्वप्न तुम्हारा टूट गया । तुम अहर्निश उसके ध्यान में जी रहे थे, उसी के सौरभविधुर कल्पांचल में साँस ले रहे थे । और तुमने पाया कि वह रुदेह सम्मुख उपस्थित हो कर भी अपने उस ऐश्वर्य कक्ष में नहीं थी । वह अपनी उस मुक्ता-मर्कन शैया में अधलेटी हो कर भी, वहाँ नहीं थी । वह वेतांब थी, बेचैन थी, और अपने ही आप को सुलभ नहीं थी । वह अपने ही
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org