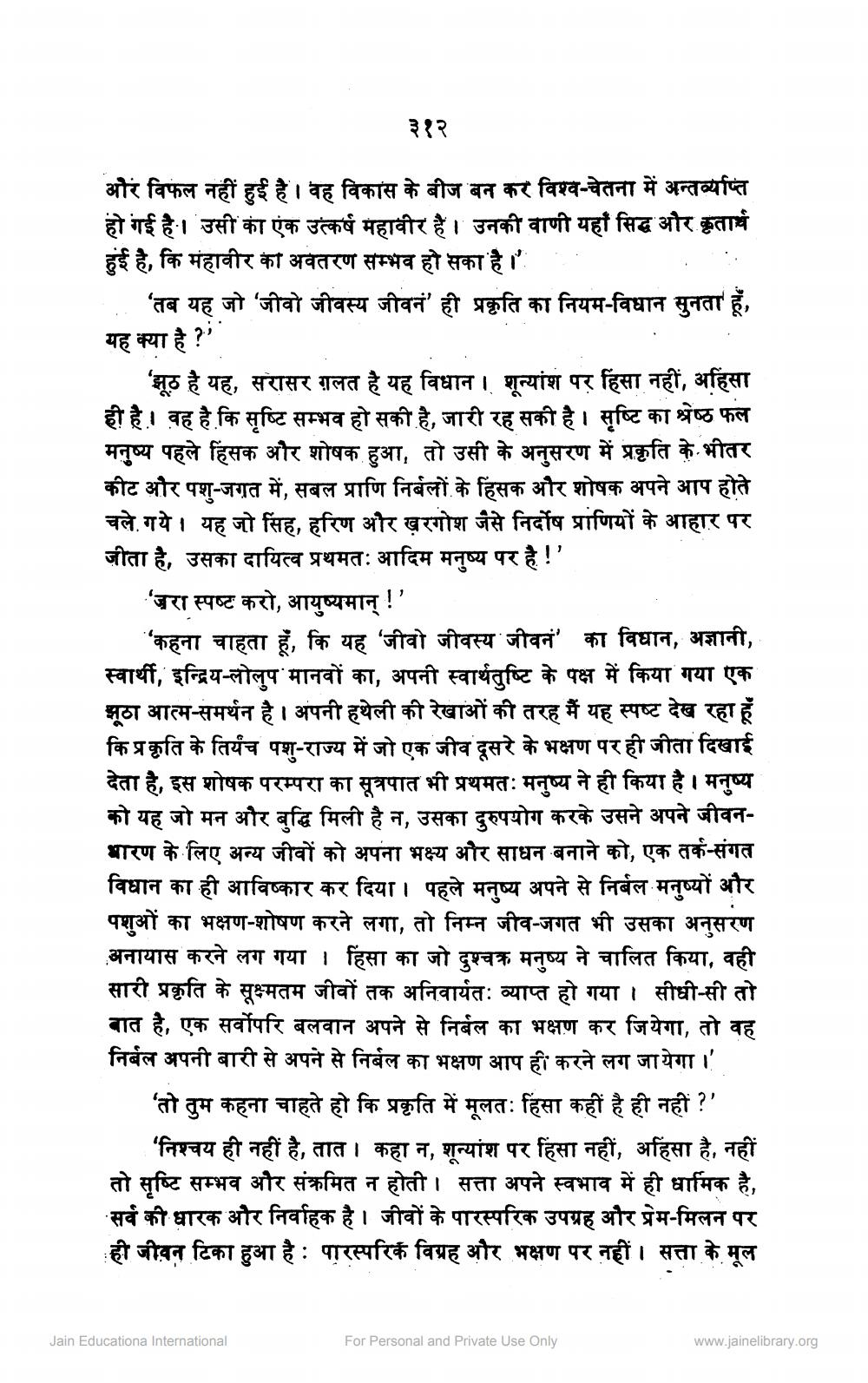________________
३१२
और विफल नहीं हुई हैं। वह विकास के बीज बन कर विश्व चेतना में अन्तर्व्याप्त गई है । उसी का एक उत्कर्ष महावीर हैं। उनकी वाणी यहाँ सिद्ध और कृतार्थ हुई है, कि महावीर का अवतरण सम्भव हो सका है ।"
'तब यह जो 'जीवो जीवस्य जीवनं' ही प्रकृति का नियम - विधान सुनता हूँ, यह क्या है ?"
'झूठ है यह, सरासर गलत है यह विधान । शून्यांश पर हिंसा नहीं, अहिंसा ही है । वह है कि सृष्टि सम्भव हो सकी है, जारी रह सकी है। सृष्टि का श्रेष्ठ फल मनुष्य पहले हिंसक और शोषक हुआ, तो उसी के अनुसरण में प्रकृति के भीतर की और पशु-जगत में, सबल प्राणि निर्बलों के हिंसक और शोषक अपने आप होते चले गये । यह जो सिंह, हरिण और खरगोश जैसे निर्दोष प्राणियों के आहार पर जीता है, उसका दायित्व प्रथमतः आदिम मनुष्य पर है ! '
'जरा स्पष्ट करो, आयुष्यमान् ! '
" कहना चाहता हूँ, कि यह 'जीवो जीवस्य जीवनं' का विधान, अज्ञानी, स्वार्थी, इन्द्रिय- लोलुप मानवों का अपनी स्वार्थतुष्टि के पक्ष में किया गया एक झूठा आत्म-समर्थन है । अपनी हथेली की रेखाओं की तरह मैं यह स्पष्ट देख रहा हूँ कि प्रकृति के तिर्यंच पशु-राज्य में जो एक जीव दूसरे के भक्षण पर ही जीता दिखाई देता है, इस शोषक परम्परा का सूत्रपात भी प्रथमतः मनुष्य ने ही किया है । मनुष्य it यह जो मन और बुद्धि मिली है न, उसका दुरुपयोग करके उसने अपने जीवनधारण के लिए अन्य जीवों को अपना भक्ष्य और साधन बनाने को, एक तर्क-संगत विधान का ही आविष्कार कर दिया। पहले मनुष्य अपने से निर्बल मनुष्यों और पशुओं का भक्षण-शोषण करने लगा, तो निम्न जीव-जगत भी उसका अनुसरण अनायास करने लग गया । हिंसा का जो दुश्चक्र मनुष्य ने चालित किया, वही सारी प्रकृति के सूक्ष्मतम जीवों तक अनिवार्यतः व्याप्त हो गया । सीधी-सी तो बात है, एक सर्वोपरि बलवान अपने से निर्बल का भक्षण कर जियेगा, तो वह निर्बल अपनी बारी से अपने से निर्बल का भक्षण आप ही करने लग जायेगा ।'
'तो तुम कहना चाहते हो कि प्रकृति में मूलत: हिंसा कहीं है ही नहीं ? '
'निश्चय ही नहीं है, तात । कहा न, शून्यांश पर हिंसा नहीं, अहिंसा है, नहीं तो सृष्टि सम्भव और संक्रमित न होती। सत्ता अपने स्वभाव में ही धार्मिक है, सर्व की धारक और निर्वाहक है । जीवों के पारस्परिक उपग्रह और प्रेम-मिलन पर ही जीवन टिका हुआ है : पारस्परिक विग्रह और भक्षण पर नहीं । सत्ता के मूल
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org