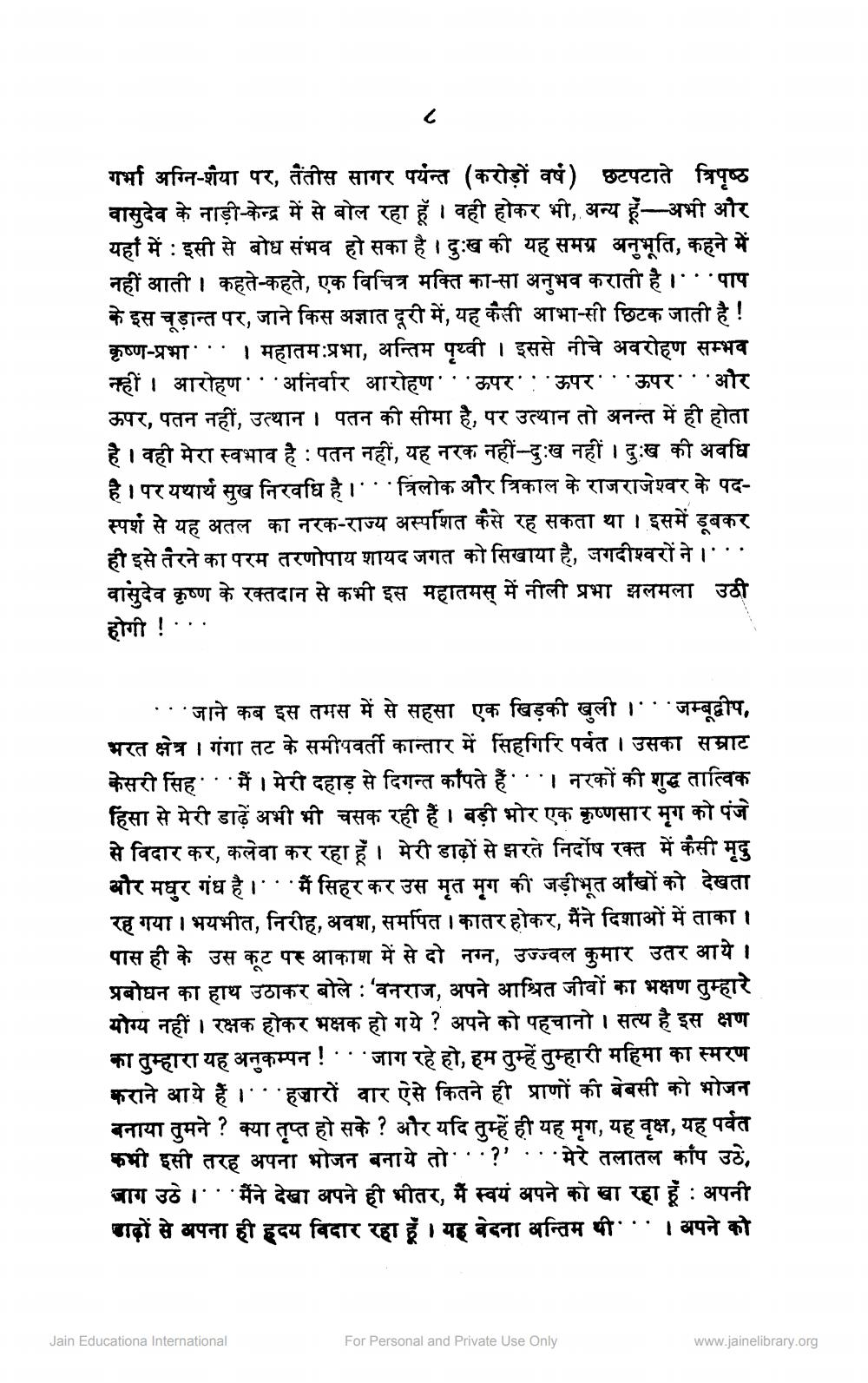________________
८
कृष्ण-प्रभा
गर्भा अग्नि-शैया पर, तैंतीस सागर पर्यन्त ( करोड़ों वर्षं) छटपटाते त्रिपृष्ठ वासुदेव के नाड़ी केन्द्र में से बोल रहा हूँ । वही होकर भी, अन्य हूँ-अभी और यहाँ में: इसी से बोध संभव हो सका है। दुःख की यह समग्र अनुभूति, कहने में नहीं आती । कहते-कहते, एक विचित्र मक्ति का-सा अनुभव कराती है । " • पाप के इस चूड़ान्त पर, जाने किस अज्ञात दूरी में, यह कैसी आभा-सी छिटक जाती है ! । महातम : प्रभा, अन्तिम पृथ्वी । इससे नीचे अवरोहण सम्भव नहीं । आरोहण अनिर्वार आरोहण 'ऊपर' : ऊपर ऊपर और ऊपर, पतन नहीं, उत्थान । पतन की सीमा है, पर उत्थान तो अनन्त में ही होता है । वही मेरा स्वभाव है : पतन नहीं, यह नरक नहीं - दुःख नहीं । दुःख की अवधि है । पर यथार्थ सुख निरवधि है । त्रिलोक और त्रिकाल के राजराजेश्वर के पदस्पर्श से यह अतल का नरक - राज्य अस्पर्शित कैसे रह सकता था । इसमें डूबकर ही इसे तैरने का परम तरणोपाय शायद जगत को सिखाया है, जगदीश्वरों ने । · · · वासुदेव कृष्ण के रक्तदान से कभी इस महातमस् में नीली प्रभा झलमला उठी होगी !
• जाने कब इस तमस में से सहसा एक खिड़की खुली । जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र । गंगा तट के समीपवर्ती कान्तार में सिंहगिरि पर्वत । उसका सम्राट केसरी सिंह मैं । मेरी दहाड़ से दिगन्त काँपते हैं ' । नरकों की शुद्ध तात्विक हिंसा से मेरी डाढ़ें अभी भी चसक रही हैं। बड़ी भोर एक कृष्णसार मृग को पंजे से विदार कर कलेवा कर रहा हूँ। मेरी डाढ़ों से झरते निर्दोष रक्त में कैसी मृदु और मधुर गंध है। मैं सिहर कर उस मृत मृग की जड़ीभूत आँखों को देखता रह गया । भयभीत, निरीह, अवश, समर्पित । कातर होकर, मैंने दिशाओं में ताका । पास ही के उस कूट पर आकाश में से दो नग्न, उज्ज्वल कुमार उतर आये । प्रबोधन का हाथ उठाकर बोले : 'वनराज, अपने आश्रित जीवों का भक्षण तुम्हारे योग्य नहीं । रक्षक होकर भक्षक हो गये ? अपने को पहचानो । सत्य है इस क्षण का तुम्हारा यह अनुकम्पन ! 'जाग रहे हो, हम तुम्हें तुम्हारी महिमा का स्मरण कराने आये हैं । हजारों वार ऐसे कितने ही प्राणों की बेबसी को भोजन बनाया तुमने ? क्या तृप्त हो सके ? और यदि तुम्हें ही यह मृग, यह वृक्ष, यह पर्वत कभी इसी तरह अपना भोजन बनाये तो ?' मेरे तलातल कांप उठे, जाग उठे । 'मैंने देखा अपने ही भीतर, मैं स्वयं अपने को खा रहा हूँ : अपनी बाढ़ों से अपना ही हृदय विदार रहा हूँ। यह बेदना अन्तिम थी ' । अपने को
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org