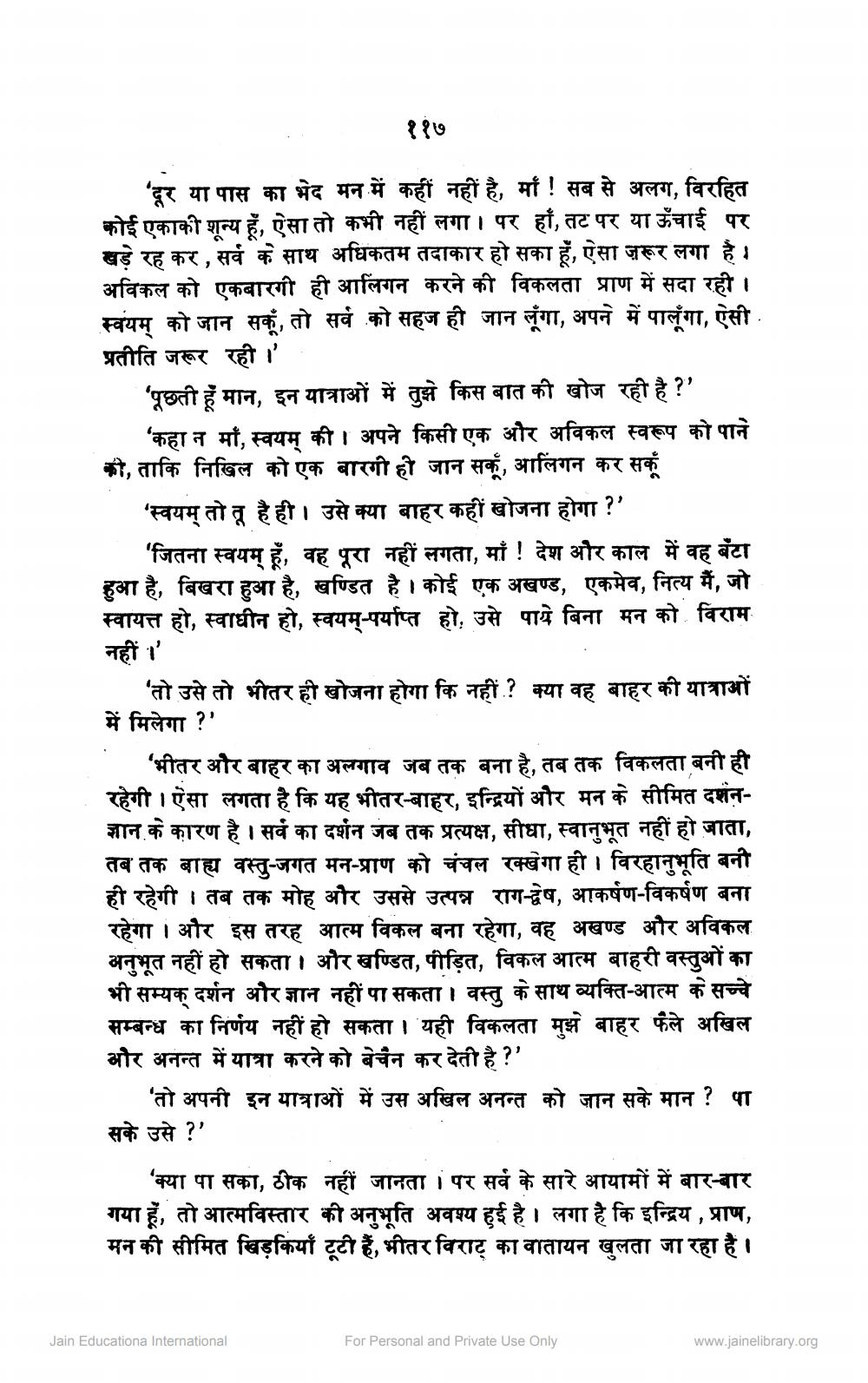________________
११७
'दूर या पास का भेद मन में कहीं नहीं है, माँ ! सब से अलग, विरहित कोई एकाकी शून्य हूँ, ऐसा तो कभी नहीं लगा। पर हाँ, तट पर या ऊँचाई पर खड़े रह कर , सर्व के साथ अधिकतम तदाकार हो सका हूँ, ऐसा ज़रूर लगा है। अविकल को एकबारगी ही आलिंगन करने की विकलता प्राण में सदा रही । स्वयम् को जान सकूँ, तो सर्व को सहज ही जान लूंगा, अपने में पालूँगा, ऐसी. प्रतीति जरूर रही।'
'पूछती हूँ मान, इन यात्राओं में तुझे किस बात की खोज रही है ?'
'कहा न माँ, स्वयम् की। अपने किसी एक और अविकल स्वरूप को पाने की, ताकि निखिल को एक बारगी हो जान सकूँ, आलिंगन कर सकूँ
'स्वयम् तो तू है ही। उसे क्या बाहर कहीं खोजना होगा?'
'जितना स्वयम् हूँ, वह पूरा नहीं लगता, माँ ! देश और काल में वह बँटा हुआ है, बिखरा हुआ है, खण्डित है। कोई एक अखण्ड, एकमेव, नित्य मैं, जो स्वायत्त हो, स्वाधीन हो, स्वयम्-पर्याप्त हो, उसे पाये बिना मन को विराम नहीं।' ___तो उसे तो भीतर ही खोजना होगा कि नहीं ? क्या वह बाहर की यात्राओं में मिलेगा?' ___ 'भीतर और बाहर का अलगाव जब तक बना है, तब तक विकलता बनी ही रहेगी। ऐसा लगता है कि यह भीतर-बाहर, इन्द्रियों और मन के सीमित दर्शनज्ञान के कारण है । सर्व का दर्शन जब तक प्रत्यक्ष, सीधा, स्वानुभूत नहीं हो जाता, तब तक बाह्य वस्तु-जगत मन-प्राण को चंचल रक्खेगा ही। विरहानुभूति बनी ही रहेगी । तब तक मोह और उससे उत्पन्न राग-द्वेष, आकर्षण-विकर्षण बना रहेगा । और इस तरह आत्म विकल बना रहेगा, वह अखण्ड और अविकल अनुभूत नहीं हो सकता। और खण्डित, पीड़ित, विकल आत्म बाहरी वस्तुओं का भी सम्यक् दर्शन और ज्ञान नहीं पा सकता। वस्तु के साथ व्यक्ति-आत्म के सच्चे सम्बन्ध का निर्णय नहीं हो सकता। यही विकलता मुझे बाहर फैले अखिल और अनन्त में यात्रा करने को बेचैन कर देती है ?' ___तो अपनी इन यात्राओं में उस अखिल अनन्त को जान सके मान ? पा सके उसे ?'
'क्या पा सका, ठीक नहीं जानता। पर सर्व के सारे आयामों में बार-बार गया हैं, तो आत्मविस्तार की अनुभूति अवश्य हुई है। लगा है कि इन्द्रिय , प्राण, मन की सीमित खिड़कियाँ टूटी हैं, भीतर विराट का वातायन खुलता जा रहा है।
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org