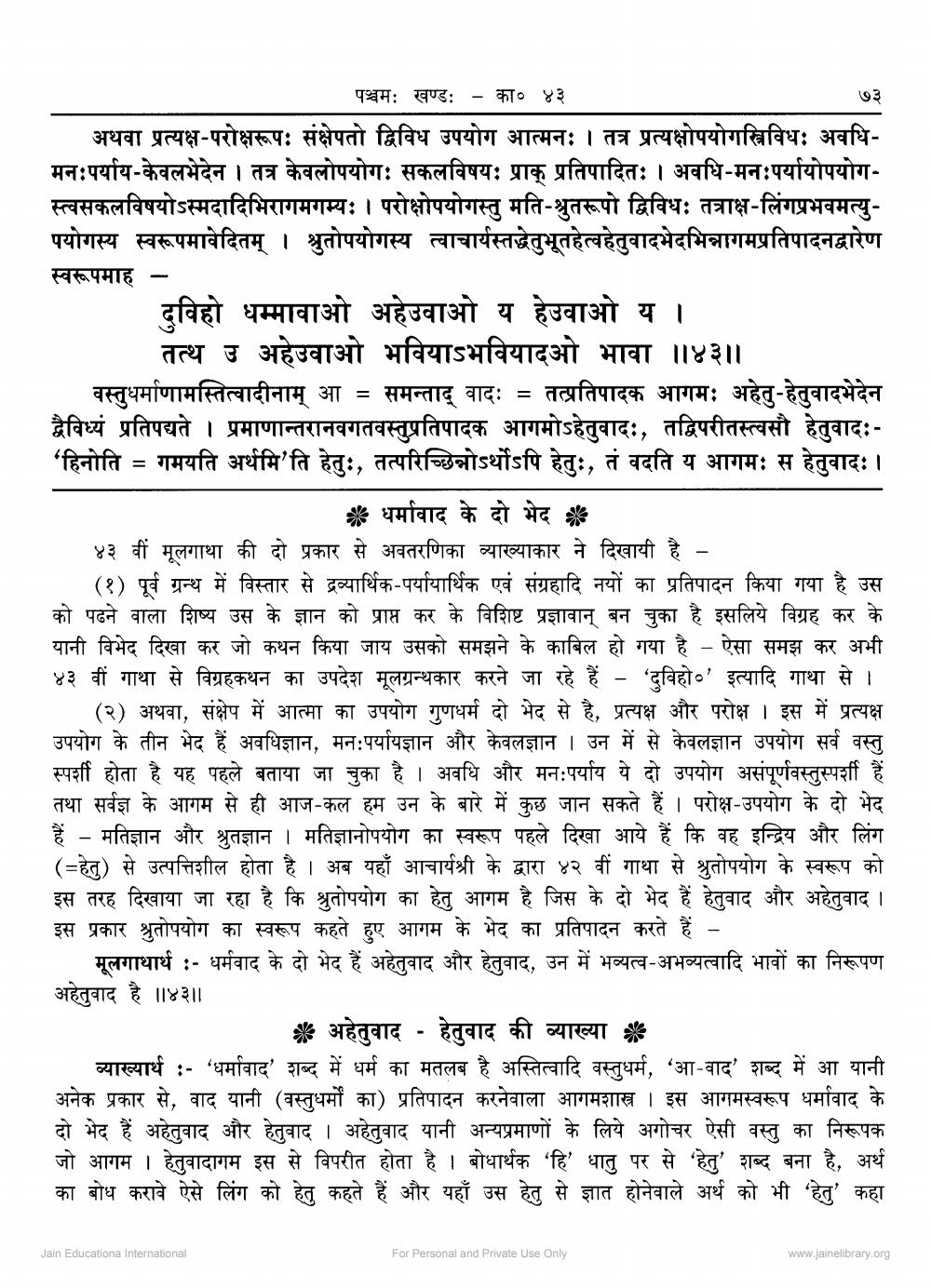________________
पञ्चमः खण्डः - का० ४३
७३
अथवा प्रत्यक्ष-परोक्षरूपः संक्षेपतो द्विविध उपयोग आत्मनः । तत्र प्रत्यक्षोपयोगस्त्रिविधः अवधिमनःपर्याय-केवलभेदेन । तत्र केवलोपयोगः सकलविषयः प्राक् प्रतिपादितः । अवधि-मनःपर्यायोपयोगस्त्वसकलविषयोऽस्मदादिभिरागमगम्यः । परोक्षोपयोगस्तु मति-श्रुतरूपो द्विविधः तत्राक्ष-लिंगप्रभवमत्युपयोगस्य स्वरूपमावेदितम् । श्रुतोपयोगस्य त्वाचार्यस्तद्धेतुभूतहेत्वहेतुवादभेदभिन्नागमप्रतिपादनद्वारेण
स्वरूपमाह ।
दुविहो धम्मावाओ अहेउवाओ य हेउवाओ य ।
तत्थ उ अहेउवाओ भवियाऽभवियादओ भावा ॥४३॥ वस्तुधर्माणामस्तित्वादीनाम् आ = समन्ताद् वादः = तत्प्रतिपादक आगमः अहेतु-हेतुवादभेदेन द्वैविध्यं प्रतिपद्यते । प्रमाणान्तरानवगतवस्तुप्रतिपादक आगमोऽहेतुवादः, तद्विपरीतस्त्वसौ हेतुवादः'हिनोति = गमयति अर्थमिति हेतुः, तत्परिच्छिन्नोऽर्थोऽपि हेतुः, तं वदति य आगमः स हेतुवादः ।
* धर्मावाद के दो भेद * ४३ वी मूलगाथा की दो प्रकार से अवतरणिका व्याख्याकार ने दिखायी है -
(१) पूर्व ग्रन्थ में विस्तार से द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक एवं संग्रहादि नयों का प्रतिपादन किया गया है उस को पढने वाला शिष्य उस के ज्ञान को प्राप्त कर के विशिष्ट प्रज्ञावान् बन चुका है इसलिये विग्रह कर के यानी विभेद दिखा कर जो कथन किया जाय उसको समझने के काबिल हो गया है – ऐसा समझ कर अभी ४३ वीं गाथा से विग्रहकथन का उपदेश मलग्रन्थकार करने जा रहे हैं - 'दविहो०' इत्यादि गा
गाथा से । ___(२) अथवा, संक्षेप में आत्मा का उपयोग गुणधर्म दो भेद से है, प्रत्यक्ष और परोक्ष । इस में प्रत्यक्ष उपयोग के तीन भेद हैं अवधिज्ञान, मन:पर्यायज्ञान और केवलज्ञान । उन में से केवलज्ञान उपयोग सर्व वस्तु स्पर्शी होता है यह पहले बताया जा चुका है । अवधि और मन:पर्याय ये दो उपयोग असंपूर्णवस्तुस्पर्शी हैं तथा सर्वज्ञ के आगम से ही आज-कल हम उन के बारे में कुछ जान सकते हैं । परोक्ष-उपयोग के दो भेद हैं - मतिज्ञान और श्रुतज्ञान । मतिज्ञानोपयोग का स्वरूप पहले दिखा आये हैं कि वह इन्द्रिय और लिंग ( हेतु) से उत्पत्तिशील होता है । अब यहाँ आचार्यश्री के द्वारा ४२ वीं गाथा से श्रुतोपयोग के स्वरूप को इस तरह दिखाया जा रहा है कि श्रुतोपयोग का हेतु आगम है जिस के दो भेद हैं हेतुवाद और अहेतुवाद । इस प्रकार श्रुतोपयोग का स्वरूप कहते हुए आगम के भेद का प्रतिपादन करते हैं - ___ मूलगाथार्थ :- धर्मवाद के दो भेद हैं अहेतुवाद और हेतुवाद, उन में भव्यत्व-अभव्यत्वादि भावों का निरूपण अहेतुवाद है ॥४३॥
* अहेतुवाद - हेतुवाद की व्याख्या * व्याख्यार्थ :- 'धर्मावाद' शब्द में धर्म का मतलब है अस्तित्वादि वस्तुधर्म, 'आ-वाद' शब्द में आ यानी अनेक प्रकार से, वाद यानी (वस्तुधर्मों का) प्रतिपादन करनेवाला आगमशास्त्र । इस आगमस्वरूप धर्मावाद के दो भेद हैं अहेतुवाद और हेतुवाद । अहेतुवाद यानी अन्यप्रमाणों के लिये अगोचर ऐसी वस्तु का निरूपक जो आगम । हेतुवादागम इस से विपरीत होता है । बोधार्थक 'हि' धातु पर से ‘हेतु' शब्द बना है, अर्थ का बोध करावे ऐसे लिंग को हेतु कहते हैं और यहाँ उस हेतु से ज्ञात होनेवाले अर्थ को भी ‘हेतु' कहा
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org