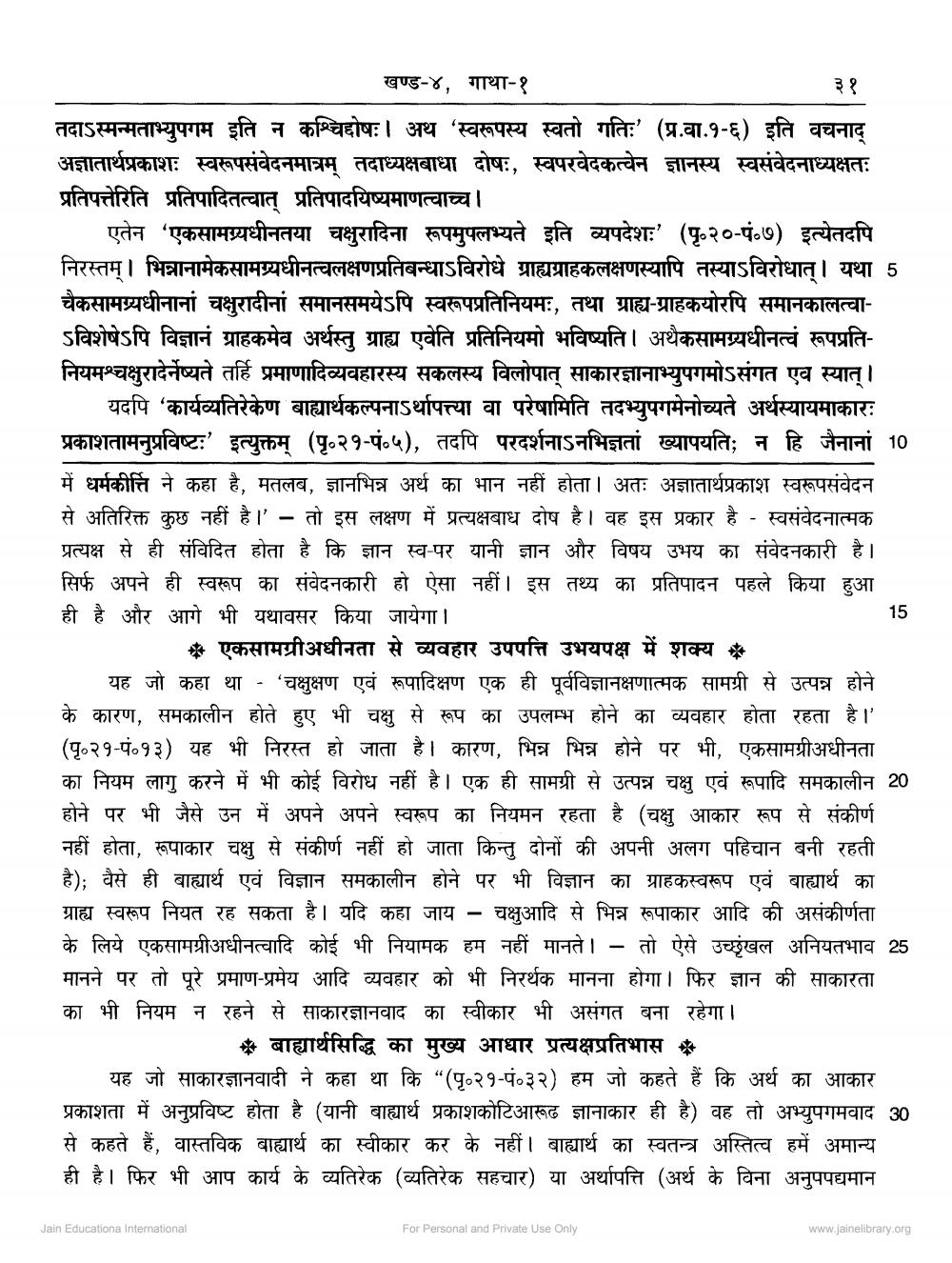________________
खण्ड - ४, गाथा - १
३१
तदाऽस्मन्मताभ्युपगम इति न कश्चिद्दोषः । अथ 'स्वरूपस्य स्वतो गतिः' (प्र. वा. १-६ ) इति वचनाद् अज्ञातार्थप्रकाशः स्वरूपसंवेदनमात्रम् तदाध्यक्षबाधा दोष:, स्वपरवेदकत्वेन ज्ञानस्य स्वसंवेदनाध्यक्षतः प्रतिपत्तेरिति प्रतिपादितत्वात् प्रतिपादयिष्यमाणत्वाच्च ।
एतेन 'एकसामग्र्यधीनतया चक्षुरादिना रूपमुपलभ्यते इति व्यपदेश:' ( पृ०२०-पं० ७) इत्येतदपि निरस्तम्। भिन्नानामेकसामग्र्यधीनत्वलक्षणप्रतिबन्धाऽविरोधे ग्राह्यग्राहकलक्षणस्यापि तस्याऽविरोधात् । यथा 5 चैकसामग्र्यधीनानां चक्षुरादीनां समानसमयेऽपि स्वरूपप्रतिनियमः, तथा ग्राह्य-ग्राहकयोरपि समानकालत्वाविशेषेऽपि विज्ञानं ग्राहकमेव अर्थस्तु ग्राह्य एवेति प्रतिनियमो भविष्यति । अथैकसामग्र्यधीनत्वं रूपप्रतिनियमश्चक्षुरादेष्यते तर्हि प्रमाणादिव्यवहारस्य सकलस्य विलोपात् साकारज्ञानाभ्युपगमोऽसंगत एव स्यात् ।
यदपि 'कार्यव्यतिरेकेण बाह्यार्थकल्पनाऽर्थापत्त्या वा परेषामिति तदभ्युपगमेनोच्यते अर्थस्यायमाकारः प्रकाशतामनुप्रविष्ट:' इत्युक्तम् ( पृ० २१- पं० ५ ), तदपि परदर्शनाऽनभिज्ञतां ख्यापयति; न हि जैनानां 10 में धर्मकीर्ति ने कहा है, मतलब, ज्ञानभिन्न अर्थ का भान नहीं होता । अतः अज्ञातार्थप्रकाश स्वरूपसंवेदन से अतिरिक्त कुछ नहीं है । ' तो इस लक्षण में प्रत्यक्षबाध दोष है । वह इस प्रकार है- स्वसंवेदनात्मक प्रत्यक्ष से ही संविदित होता है कि ज्ञान स्व-पर यानी ज्ञान और विषय उभय का संवेदनकारी है । सिर्फ अपने ही स्वरूप का संवेदनकारी हो ऐसा नहीं । इस तथ्य का प्रतिपादन पहले किया हुआ ही है और आगे भी यथावसर किया जायेगा ।
* एकसामग्री अधीनता से व्यवहार उपपत्ति उभयपक्ष में शक्य **
यह जो कहा था 'चक्षुक्षण एवं रूपादिक्षण एक ही पूर्वविज्ञानक्षणात्मक सामग्री से उत्पन्न होने के कारण, समकालीन होते हुए भी चक्षु से रूप का उपलम्भ होने का व्यवहार होता रहता है।' ( पृ०२१-पं०१३) यह भी निरस्त हो जाता है । कारण, भिन्न भिन्न होने पर भी, एकसामग्री अधीनता का नियम लागु करने में भी कोई विरोध नहीं है। एक ही सामग्री से उत्पन्न चक्षु एवं रूपादि समकालीन 20 होने पर भी जैसे उन में अपने अपने स्वरूप का नियमन रहता है ( चक्षु आकार रूप से संकीर्ण नहीं होता, रूपाकार चक्षु से संकीर्ण नहीं हो जाता किन्तु दोनों की अपनी अलग पहिचान बनी रहती है); वैसे ही बाह्यार्थ एवं विज्ञान समकालीन होने पर भी विज्ञान का ग्राहकस्वरूप एवं बाह्यार्थ का ग्राह्य स्वरूप नियत रह सकता है। यदि कहा जाय चक्षुआदि से भिन्न रूपाकार आदि की असंकीर्णता के लिये एकसामग्री अधीनत्वादि कोई भी नियामक हम नहीं मानते । तो ऐसे उच्छृंखल अनियतभाव 25 मानने पर तो पूरे प्रमाण- प्रमेय आदि व्यवहार को भी निरर्थक मानना होगा। फिर ज्ञान की साकारता का भी नियम न रहने से साकारज्ञानवाद का स्वीकार भी असंगत बना रहेगा ।
Jain Educationa International
15
-
* बाह्यार्थसिद्धि का मुख्य आधार प्रत्यक्षप्रतिभास
यह जो साकारज्ञानवादी ने कहा था कि “ ( पृ० २१- पं० ३२ ) हम जो कहते हैं कि अर्थ का आकार प्रकाशता में अनुप्रविष्ट होता है (यानी बाह्यार्थ प्रकाशकोटिआरूढ ज्ञानाकार ही है) वह तो अभ्युपगमवाद 30 से कहते हैं, वास्तविक बाह्यार्थ का स्वीकार कर के नहीं । बाह्यार्थ का स्वतन्त्र अस्तित्व हमें अमान्य ही है। फिर भी आप कार्य के व्यतिरेक (व्यतिरेक सहचार) या अर्थापत्ति ( अर्थ के विना अनुपपद्यमान
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org