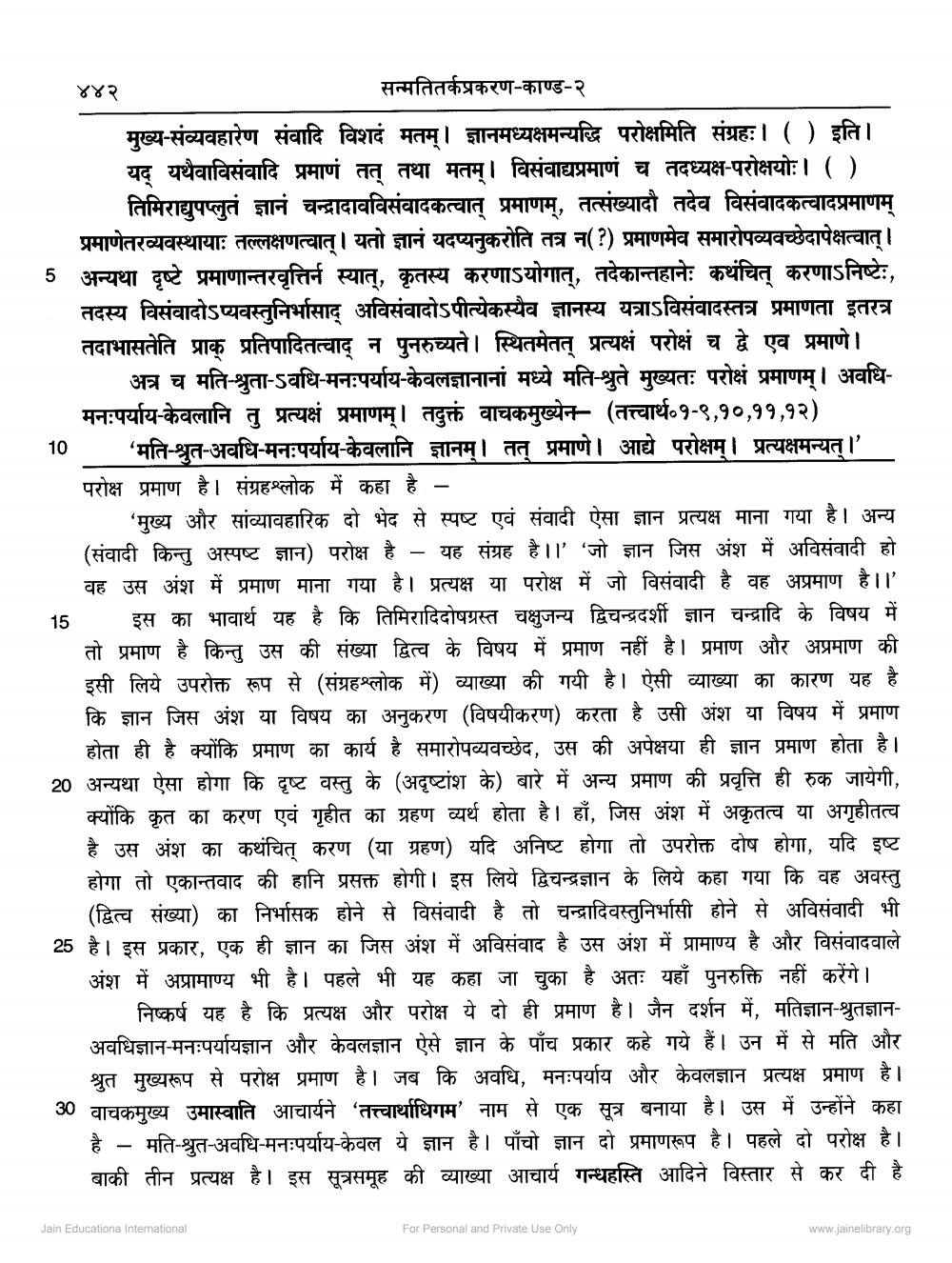________________
सन्मतितर्कप्रकरण - काण्ड - २
मुख्य-संव्यवहारेण संवादि विशदं मतम् । ज्ञानमध्यक्षमन्यद्धि परोक्षमिति संग्रह: । ( ) इति । यद् यथैवाविसंवादि प्रमाणं तत् तथा मतम् । विसंवाद्यप्रमाणं च तदध्यक्ष-परोक्षयोः । ( )
तिमिराद्युपप्लुतं ज्ञानं चन्द्रादावविसंवादकत्वात् प्रमाणम्, तत्संख्यादौ तदेव विसंवादकत्वादप्रमाणम् प्रमाणेतरव्यवस्थायाः तल्लक्षणत्वात् । यतो ज्ञानं यदप्यनुकरोति तत्र न ( ? ) प्रमाणमेव समारोपव्यवच्छेदापेक्षत्वात् । 5 अन्यथा दृष्टे प्रमाणान्तरवृत्तिर्न स्यात्, कृतस्य करणाऽयोगात्, तदेकान्तहानेः कथंचित् करणाऽनिष्टे :, तदस्य विसंवादोऽप्यवस्तुनिर्भासाद् अविसंवादोऽपीत्येकस्यैव ज्ञानस्य यत्राऽविसंवादस्तत्र प्रमाणता इतरत्र तदाभासतेति प्राक् प्रतिपादितत्वाद् न पुनरुच्यते । स्थितमेतत् प्रत्यक्षं परोक्षं च द्वे एव प्रमाणे ।
अत्र च मति श्रुताऽवधि - मनःपर्याय - केवलज्ञानानां मध्ये मति श्रुते मुख्यतः परोक्षं प्रमाणम् । अवधि - मनःपर्याय- केवलानि तु प्रत्यक्षं प्रमाणम्। तदुक्तं वाचकमुख्येन (तत्त्वार्थ०१-९,१०,११,१२)
'मति श्रुत-अवधि- मनःपर्याय - केवलानि ज्ञानम् । तत् प्रमाणे । आद्ये परोक्षम् । प्रत्यक्षमन्यत् । ' परोक्ष प्रमाण है । संग्रह श्लोक में कहा है
'मुख्य और सांव्यावहारिक दो भेद से
स्पष्ट एवं संवादी ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष माना गया है। अन्य यह संग्रह है ।।' 'जो ज्ञान जिस अंश में अविसंवादी हो
( संवादी किन्तु अस्पष्ट ज्ञान ) परोक्ष है वह उस अंश में प्रमाण माना गया है। प्रत्यक्ष या परोक्ष में जो विसंवादी है वह अप्रमाण है ।।'
15
इस का भावार्थ यह है कि तिमिरादिदोषग्रस्त चक्षुजन्य द्विचन्द्रदर्शी ज्ञान चन्द्रादि के विषय में तो प्रमाण है किन्तु उस की संख्या द्वित्व के विषय में प्रमाण नहीं है । प्रमाण और अप्रमाण की इसी लिये उपरोक्त रूप से ( संग्रह श्लोक में) व्याख्या की गयी । ऐसी व्याख्या का कारण यह है कि ज्ञान जिस अंश या विषय का अनुकरण (विषयीकरण) करता है उसी अंश या विषय प्रमाण होता ही है क्योंकि प्रमाण का कार्य है समारोपव्यवच्छेद, उस की अपेक्षया ही ज्ञान प्रमाण होता है । 20 अन्यथा ऐसा होगा कि दृष्ट वस्तु के ( अदृष्टांश के) बारे में अन्य प्रमाण की प्रवृत्ति ही रुक जायेगी, क्योंकि कृत का करण एवं गृहीत का ग्रहण व्यर्थ होता है। हाँ, जिस अंश में अकृतत्व या अगृहीतत्व है उस अंश का कथंचित् करण ( या ग्रहण) यदि अनिष्ट होगा तो उपरोक्त दोष होगा, यदि इष्ट होगा तो एकान्तवाद की हानि प्रसक्त होगी । इस लिये द्विचन्द्रज्ञान के लिये कहा गया कि वह अवस्तु (द्वित्व संख्या) का निर्भासक होने से विसंवादी है तो चन्द्रादिवस्तुनिर्भासी होने से अविसंवादी भी 25 है। इस प्रकार, एक ही ज्ञान का जिस अंश में अविसंवाद है उस अंश में प्रामाण्य है और विसंवादवाले अंश में अप्रामाण्य भी है। पहले भी यह कहा जा चुका है अतः यहाँ पुनरुक्ति नहीं करेंगे ।
निष्कर्ष यह है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो ही प्रमाण है। जैन दर्शन में, मतिज्ञान- श्रुतज्ञानअवधिज्ञान-मनःपर्यायज्ञान और केवलज्ञान ऐसे ज्ञान के पाँच प्रकार कहे गये हैं । उन में से मति और श्रुत मुख्यरूप से परोक्ष प्रमाण है। जब कि अवधि, मनःपर्याय और केवलज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है । 30 वाचकमुख्य उमास्वाति आचार्यने 'तत्त्वार्थाधिगम' नाम से एक सूत्र बनाया । उस में उन्होंने कहा है मति श्रुत-अवधि - मनःपर्याय - केवल ये ज्ञान है । पाँचो ज्ञान दो प्रमाणरूप है। पहले दो परोक्ष है । बाकी तीन प्रत्यक्ष है। इस सूत्रसमूह की व्याख्या आचार्य गन्धहस्ति आदिने विस्तार से कर दी है।
10
४४२
-
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org