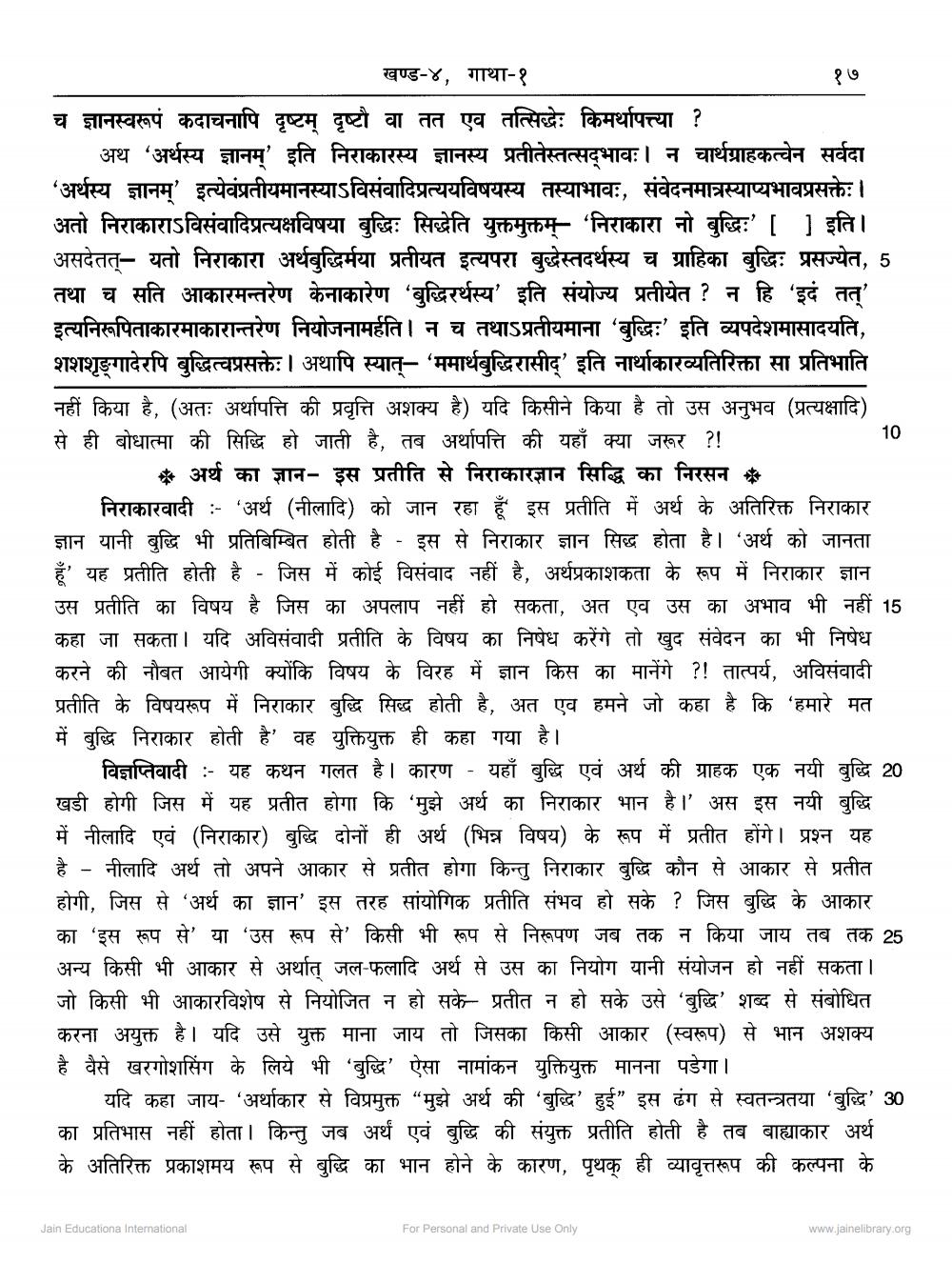________________
खण्ड-४, गाथा-१ च ज्ञानस्वरूपं कदाचनापि दृष्टम् दृष्टौ वा तत एव तत्सिद्धेः किमर्थापत्त्या ?
___ अथ ‘अर्थस्य ज्ञानम्' इति निराकारस्य ज्ञानस्य प्रतीतेस्तत्सद्भावः। न चार्थग्राहकत्वेन सर्वदा 'अर्थस्य ज्ञानम्' इत्येवंप्रतीयमानस्याऽविसंवादिप्रत्ययविषयस्य तस्याभावः, संवेदनमात्रस्याप्यभावप्रसक्तेः । अतो निराकाराऽविसंवादिप्रत्यक्षविषया बुद्धिः सिद्धेति युक्तमुक्तम्- 'निराकारा नो बुद्धिः' [ ] इति। असदेतत्- यतो निराकारा अर्थबुद्धिर्मया प्रतीयत इत्यपरा बुद्धेस्तदर्थस्य च ग्राहिका बुद्धिः प्रसज्येत, 5 तथा च सति आकारमन्तरेण केनाकारेण 'बुद्धिरर्थस्य' इति संयोज्य प्रतीयेत ? न हि 'इदं तत्' इत्यनिरूपिताकारमाकारान्तरेण नियोजनामर्हति । न च तथाऽप्रतीयमाना 'बुद्धिः' इति व्यपदेशमासादयति, शशशृङ्गादेरपि बुद्धित्वप्रसक्तेः । अथापि स्यात्- ‘ममार्थबुद्धिरासीद्' इति नार्थाकारव्यतिरिक्ता सा प्रतिभाति नहीं किया है, (अतः अर्थापत्ति की प्रवृत्ति अशक्य है) यदि किसीने किया है तो उस अनुभव (प्रत्यक्षादि) से ही बोधात्मा की सिद्धि हो जाती है, तब अर्थापत्ति की यहाँ क्या जरूर ?!
* अर्थ का ज्ञान- इस प्रतीति से निराकारज्ञान सिद्धि का निरसन * निराकारवादी :- ‘अर्थ (नीलादि) को जान रहा हूँ इस प्रतीति में अर्थ के अतिरिक्त निराकार ज्ञान यानी बुद्धि भी प्रतिबिम्बित होती है - इस से निराकार ज्ञान सिद्ध होता है। ‘अर्थ को जानता हूँ' यह प्रतीति होती है - जिस में कोई विसंवाद नहीं है, अर्थप्रकाशकता के रूप में निराकार ज्ञान उस प्रतीति का विषय है जिस का अपलाप नहीं हो सकता, अत एव उस का अभाव भी नहीं 15 कहा जा सकता। यदि अविसंवादी प्रतीति के विषय का निषेध करेंगे तो खुद संवेदन का भी निषेध करने की नौबत आयेगी क्योंकि विषय के विरह में ज्ञान किस का मानेंगे ?! तात्पर्य, अविसंवादी प्रतीति के विषयरूप में निराकार बुद्धि सिद्ध होती है, अत एव हमने जो कहा है कि 'हमारे मत में बुद्धि निराकार होती है' वह युक्तियुक्त ही कहा गया है।
विज्ञप्तिवादी :- यह कथन गलत है। कारण - यहाँ बद्धि एवं अर्थ की ग्राहक एक खड़ी होगी जिस में यह प्रतीत होगा कि 'मुझे अर्थ का निराकार भान है।' अस इस नयी बुद्धि में नीलादि एवं (निराकार) बुद्धि दोनों ही अर्थ (भिन्न विषय) के रूप में प्रतीत होंगे। प्रश्न यह है - नीलादि अर्थ तो अपने आकार से प्रतीत होगा किन्तु निराकार बुद्धि कौन से आकार से प्रतीत होगी, जिस से ‘अर्थ का ज्ञान' इस तरह सांयोगिक प्रतीति संभव हो सके ? जिस बुद्धि के आकार का 'इस रूप से' या 'उस रूप से किसी भी रूप से निरूपण जब तक न किया जाय तब तक 25 अन्य किसी भी आकार से अर्थात जल-फलादि अर्थ से उस का नियोग यानी संयोजन हो नहीं सकता। जो किसी भी आकारविशेष से नियोजित न हो सके- प्रतीत न हो सके उसे 'बुद्धि' शब्द से संबोधित करना अयुक्त है। यदि उसे युक्त माना जाय तो जिसका किसी आकार (स्वरूप) से भान अशक्य है वैसे खरगोशसिंग के लिये भी 'बुद्धि' ऐसा नामांकन युक्तियुक्त मानना पडेगा।
यदि कहा जाय- ‘अर्थाकार से विप्रमुक्त “मुझे अर्थ की 'बुद्धि' हुई" इस ढंग से स्वतन्त्रतया 'बुद्धि' 30 का प्रतिभास नहीं होता। किन्तु जब अर्थं एवं बुद्धि की संयुक्त प्रतीति होती है तब बाह्याकार अर्थ के अतिरिक्त प्रकाशमय रूप से बुद्धि का भान होने के कारण, पृथक् ही व्यावृत्तरूप की कल्पना के
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org