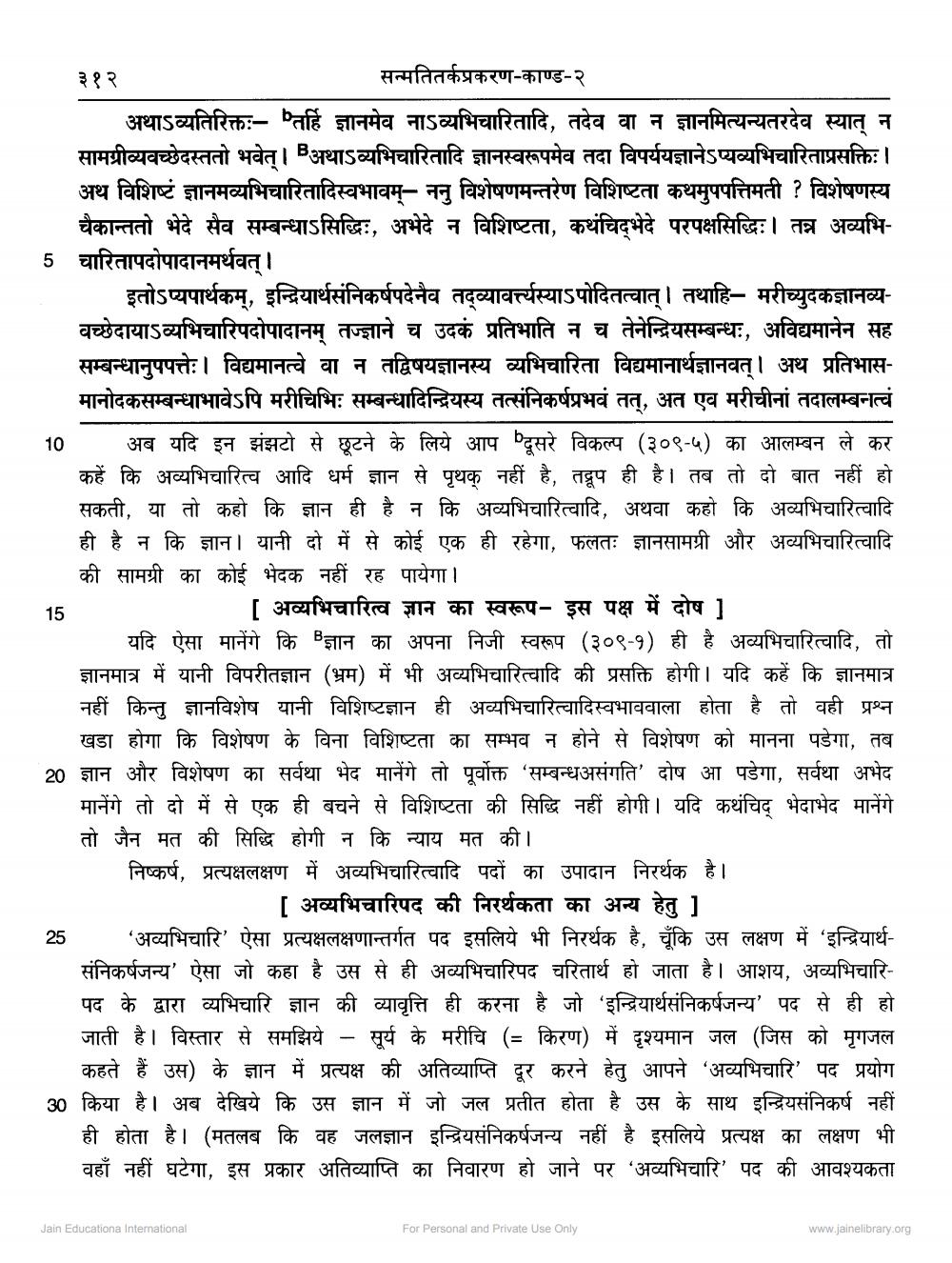________________
३१२
सन्मतितर्कप्रकरण-काण्ड-२ अथाऽव्यतिरिक्त:- तिर्हि ज्ञानमेव नाऽव्यभिचारितादि, तदेव वा न ज्ञानमित्यन्यतरदेव स्यात् न सामग्रीव्यवच्छेदस्ततो भवेत् । Bअथाऽव्यभिचारितादि ज्ञानस्वरूपमेव तदा विपर्ययज्ञानेऽप्यव्यभिचारिताप्रसक्तिः । अथ विशिष्टं ज्ञानमव्यभिचारितादिस्वभावम्- ननु विशेषणमन्तरेण विशिष्टता कथमुपपत्तिमती ? विशेषणस्य
चैकान्ततो भेदे सैव सम्बन्धाऽसिद्धिः, अभेदे न विशिष्टता, कथंचिद्भेदे परपक्षसिद्धिः। तन्न अव्यभि5 चारितापदोपादानमर्थवत्।
इतोऽप्यपार्थकम्, इन्द्रियार्थसंनिकर्षपदेनैव तव्यावर्त्यस्याऽपोदितत्वात् । तथाहि- मरीच्युदकज्ञानव्यवच्छेदायाऽव्यभिचारिपदोपादानम् तज्ज्ञाने च उदकं प्रतिभाति न च तेनेन्द्रियसम्बन्धः, अविद्यमानेन सह सम्बन्धानुपपत्तेः। विद्यमानत्वे वा न तद्विषयज्ञानस्य व्यभिचारिता विद्यमानार्थज्ञानवत् । अथ प्रतिभास
मानोदकसम्बन्धाभावेऽपि मरीचिभिः सम्बन्धादिन्द्रियस्य तत्संनिकर्षप्रभवं तत्, अत एव मरीचीनां तदालम्बनत्वं 10 अब यदि इन झंझटो से छूटने के लिये आप दूसरे विकल्प (३०९-५) का आलम्बन ले कर
कहें कि अव्यभिचारित्व आदि धर्म ज्ञान से पृथक् नहीं है, तद्रूप ही है। तब तो दो बात नहीं हो सकती, या तो कहो कि ज्ञान ही है न कि अव्यभिचारित्वादि, अथवा कहो कि अव्यभिचारित्वादि ही है न कि ज्ञान। यानी दो में से कोई एक ही रहेगा, फलतः ज्ञानसामग्री और अव्यभिचारित्वादि की सामग्री का कोई भेदक नहीं रह पायेगा।
[ अव्यभिचारित्व ज्ञान का स्वरूप- इस पक्ष में दोष ] यदि ऐसा मानेंगे कि Bज्ञान का अपना निजी स्वरूप (३०९-१) ही है अव्यभिचारित्वादि, तो ज्ञानमात्र में यानी विपरीतज्ञान (भ्रम) में भी अव्यभिचारित्वादि की प्रसक्ति होगी। यदि कहें कि ज्ञानमात्र नहीं किन्तु ज्ञानविशेष यानी विशिष्टज्ञान ही अव्यभिचारित्वादिस्वभाववाला होता है तो वही प्रश्न
खडा होगा कि विशेषण के विना विशिष्टता का सम्भव न होने से विशेषण को मानना पडेगा, तब 20 ज्ञान और विशेषण का सर्वथा भेद मानेंगे तो पूर्वोक्त ‘सम्बन्धअसंगति' दोष आ पडेगा, सर्वथा अभेद
मानेंगे तो दो में से एक ही बचने से विशिष्टता की सिद्धि नहीं होगी। यदि कथंचिद् भेदाभेद मानेंगे तो जैन मत की सिद्धि होगी न कि न्याय मत की। निष्कर्ष, प्रत्यक्षलक्षण में अव्यभिचारित्वादि पदों का उपादान निरर्थक है।
[अव्यभिचारिपद की निरर्थकता का अन्य हेतु ] 'अव्यभिचारि' ऐसा प्रत्यक्षलक्षणान्तर्गत पद इसलिये भी निरर्थक है. चूँकि उस लक्षण में 'इन्द्रियार्थसंनिकर्षजन्य' ऐसा जो कहा है उस से ही अव्यभिचारिपद चरितार्थ हो जाता है। आशय, अव्यभिचारिपद के द्वारा व्यभिचारि ज्ञान की व्यावृत्ति ही करना है जो 'इन्द्रियार्थसंनिकर्षजन्य' पद से ही हो जाती है। विस्तार से समझिये - सूर्य के मरीचि (= किरण) में दृश्यमान जल (जिस को मृगजल
कहते हैं उस) के ज्ञान में प्रत्यक्ष की अतिव्याप्ति दूर करने हेतु आपने 'अव्यभिचारि' पद प्रयोग 30 किया है। अब देखिये कि उस ज्ञान में जो जल प्रतीत होता है उस के साथ इन्द्रियसंनिकर्ष नहीं
ही होता है। (मतलब कि वह जलज्ञान इन्द्रियसंनिकर्षजन्य नहीं है इसलिये प्रत्यक्ष का लक्षण भी वहाँ नहीं घटेगा, इस प्रकार अतिव्याप्ति का निवारण हो जाने पर 'अव्यभिचारि' पद की आवश्यकता
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org