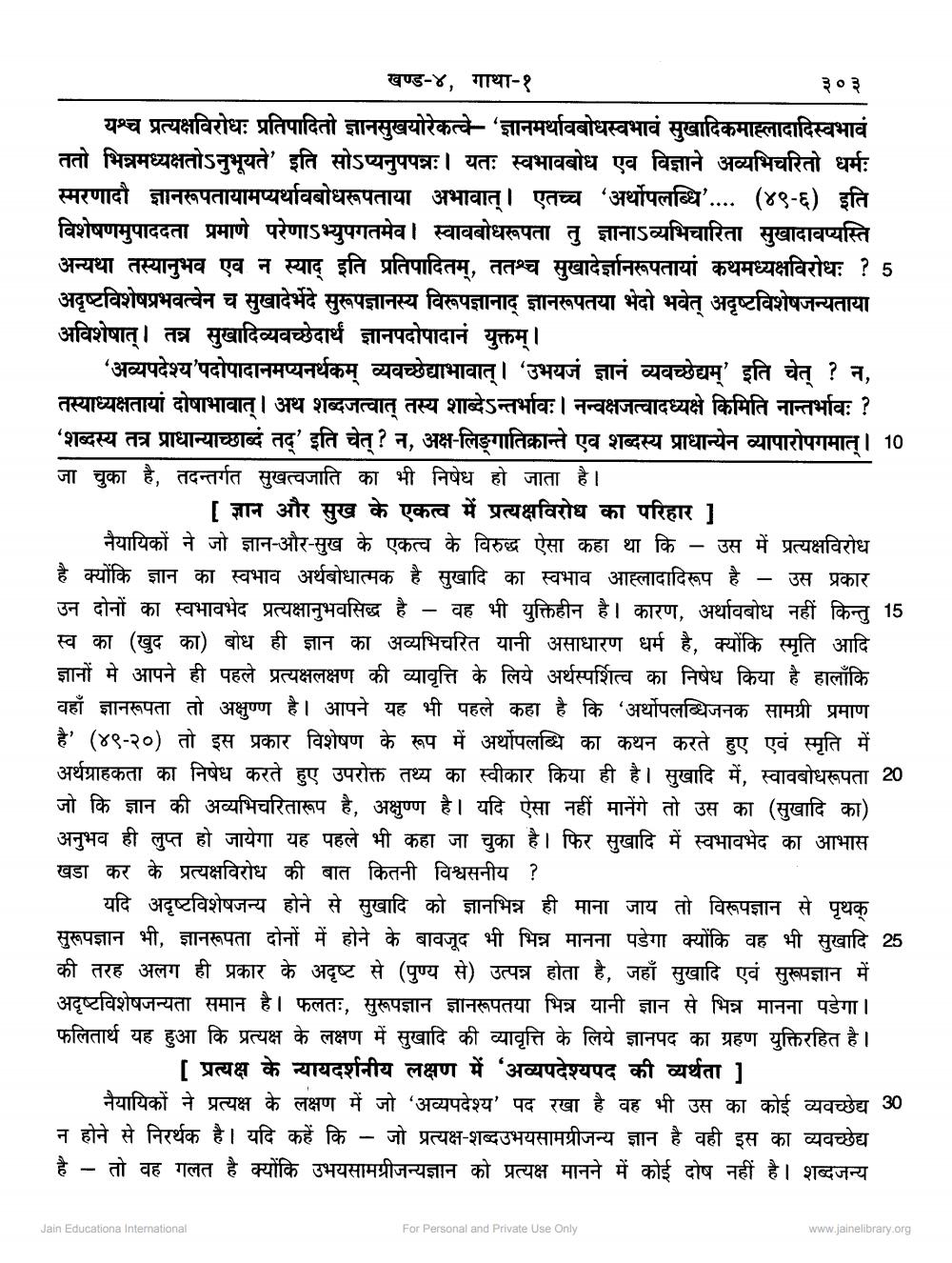________________
खण्ड-४, गाथा-१
३०३
यश्च प्रत्यक्षविरोधः प्रतिपादितो ज्ञानसुखयोरेकत्वे 'ज्ञानमर्थावबोधस्वभावं सुखादिकमालादादिस्वभावं ततो भिन्नमध्यक्षतोऽनुभूयते' इति सोऽप्यनुपपन्नः। यतः स्वभावबोध एव विज्ञाने अव्यभिचरितो धर्मः स्मरणादौ ज्ञानरूपतायामप्यर्थावबोधरूपताया अभावात्। एतच्च ‘अर्थोपलब्धि'.... (४९-६) इति विशेषणमुपाददता प्रमाणे परेणाऽभ्युपगतमेव । स्वावबोधरूपता तु ज्ञानाऽव्यभिचारिता सुखादावप्यस्ति अन्यथा तस्यानुभव एव न स्याद् इति प्रतिपादितम्, ततश्च सुखादेर्ज्ञानरूपतायां कथमध्यक्षविरोधः ? 5 अदृष्टविशेषप्रभवत्वेन च सुखादेर्भदे सुरूपज्ञानस्य विरूपज्ञानाद् ज्ञानरूपतया भेदो भवेत् अदृष्टविशेषजन्यताया अविशेषात्। तन्न सुखादिव्यवच्छेदार्थं ज्ञानपदोपादानं युक्तम् ।
'अव्यपदेश्य'पदोपादानमप्यनर्थकम् व्यवच्छेद्याभावात्। 'उभयजं ज्ञानं व्यवच्छेद्यम्' इति चेत् ? न, तस्याध्यक्षतायां दोषाभावात् । अथ शब्दजत्वात् तस्य शाब्देऽन्तर्भावः । नन्वक्षजत्वादध्यक्षे किमिति नान्तर्भावः ? 'शब्दस्य तत्र प्राधान्याच्छाब्दं तद्' इति चेत् ? न, अक्ष-लिङ्गातिक्रान्ते एव शब्दस्य प्राधान्येन व्यापारोपगमात्। 10 जा चुका है, तदन्तर्गत सुखत्वजाति का भी निषेध हो जाता है।
[ ज्ञान और सुख के एकत्व में प्रत्यक्षविरोध का परिहार ] नैयायिकों ने जो ज्ञान-और-सुख के एकत्व के विरुद्ध ऐसा कहा था कि - उस में प्रत्यक्षविरोध है क्योंकि ज्ञान का स्वभाव अर्थबोधात्मक है सुखादि का स्वभाव आह्लादादिरूप है - उस प्रकार उन दोनों का स्वभावभेद प्रत्यक्षानुभवसिद्ध है - वह भी युक्तिहीन है। कारण, अर्थावबोध नहीं किन्तु 15 स्व का (खुद का) बोध ही ज्ञान का अव्यभिचरित यानी असाधारण धर्म है, क्योंकि स्मृति आदि ज्ञानों मे आपने ही पहले प्रत्यक्षलक्षण की व्यावृत्ति के लिये अर्थस्पर्शित्व का निषेध किया है हालाँकि वहाँ ज्ञानरूपता तो अक्षुण्ण है। आपने यह भी पहले कहा है कि 'अर्थोपलब्धिजनक सामग्री प्रमाण है' (४९-२०) तो इस प्रकार विशेषण के रूप में अर्थोपलब्धि का कथन करते हुए एवं स्मृति में अर्थग्राहकता का निषेध करते हुए उपरोक्त तथ्य का स्वीकार किया ही है। सुखादि में, स्वावबोधरूपता 20 जो कि ज्ञान की अव्यभिचरितारूप है, अक्षुण्ण है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो उस का (सुखादि का) अनुभव ही लुप्त हो जायेगा यह पहले भी कहा जा चुका है। फिर सुखादि में स्वभावभेद का आभास खडा कर के प्रत्यक्षविरोध की बात कितनी विश्वसनीय ?
यदि अदृष्टविशेषजन्य होने से सुखादि को ज्ञानभिन्न ही माना जाय तो विरूपज्ञान से पृथक् सुरूपज्ञान भी, ज्ञानरूपता दोनों में होने के बावजूद भी भिन्न मानना पडेगा क्योंकि वह भी सुखादि 25 की तरह अलग ही प्रकार के अदृष्ट से (पुण्य से) उत्पन्न होता है, जहाँ सुखादि एवं सुरूपज्ञान में अदृष्टविशेषजन्यता समान है। फलतः, सुरूपज्ञान ज्ञानरूपतया भिन्न यानी ज्ञान से भिन्न मानना पडेगा। फलितार्थ यह हुआ कि प्रत्यक्ष के लक्षण में सुखादि की व्यावृत्ति के लिये ज्ञानपद का ग्रहण युक्तिरहित है।
[ प्रत्यक्ष के न्यायदर्शनीय लक्षण में 'अव्यपदेश्यपद की व्यर्थता ] नैयायिकों ने प्रत्यक्ष के लक्षण में जो ‘अव्यपदेश्य' पद रखा है वह भी उस का कोई व्यवच्छेद्य 30 न होने से निरर्थक है। यदि कहें कि - जो प्रत्यक्ष-शब्दउभयसामग्रीजन्य ज्ञान है वही इस का व्यवच्छेद्य है - तो वह गलत है क्योंकि उभयसामग्रीजन्यज्ञान को प्रत्यक्ष मानने में कोई दोष नहीं है। शब्दजन्य
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org